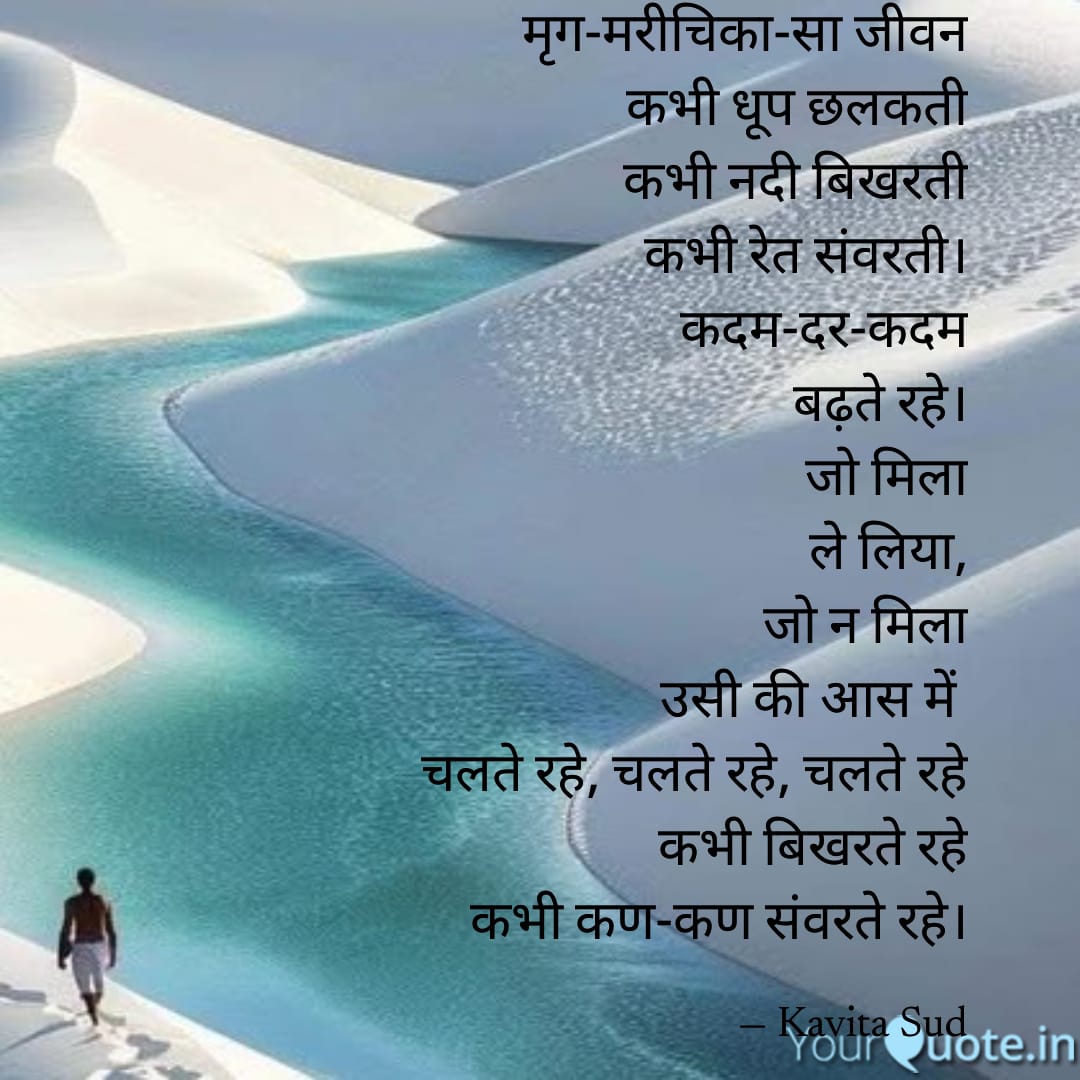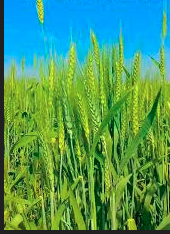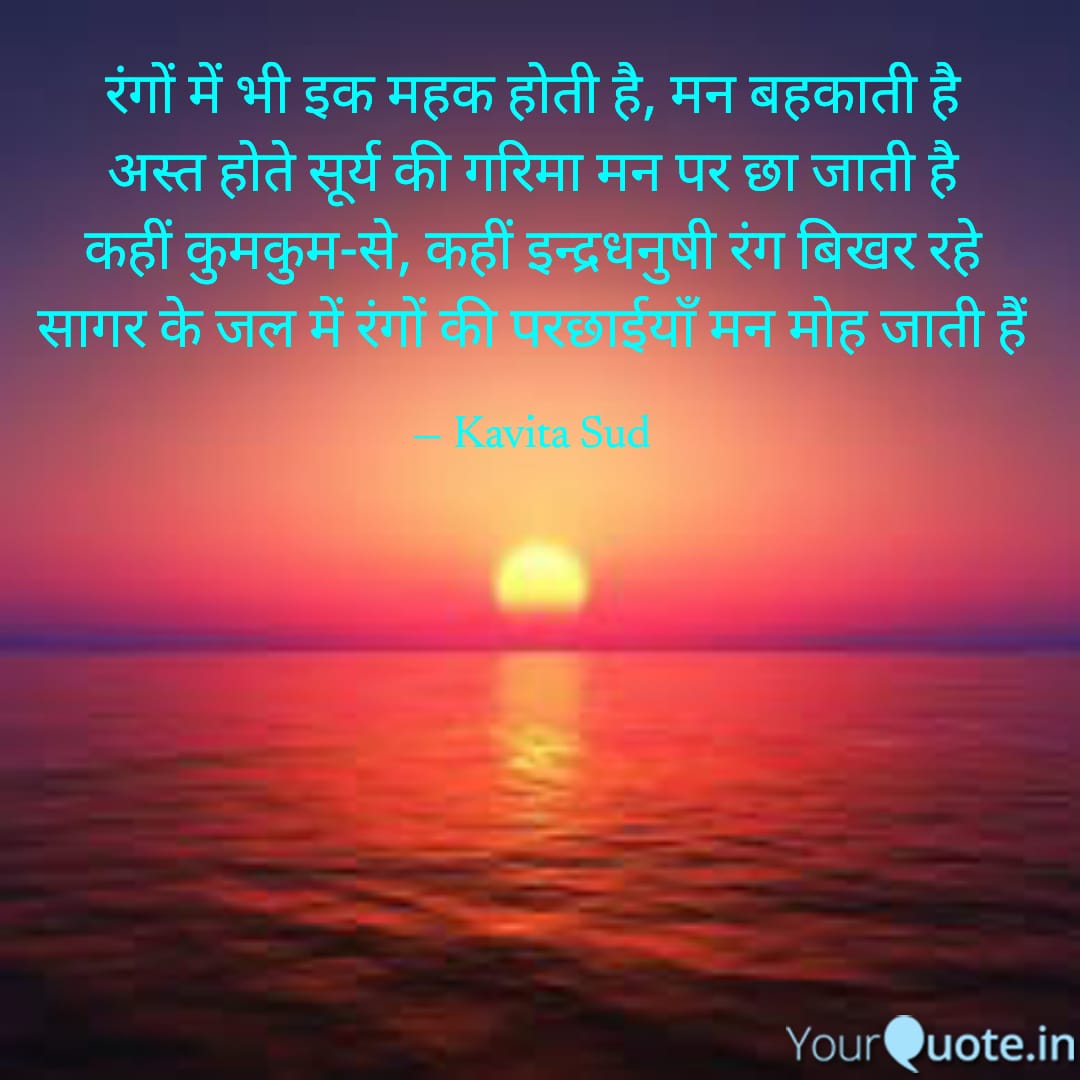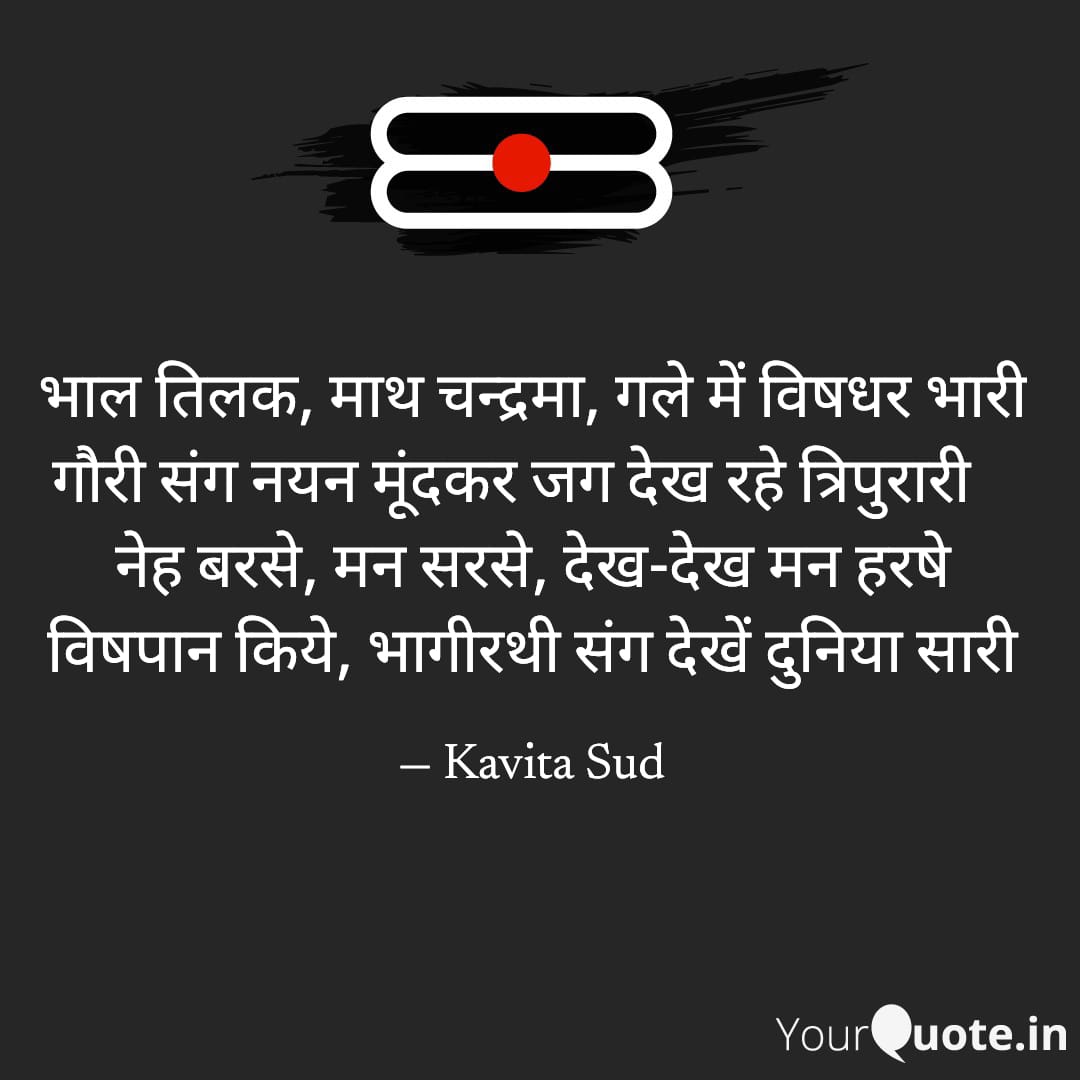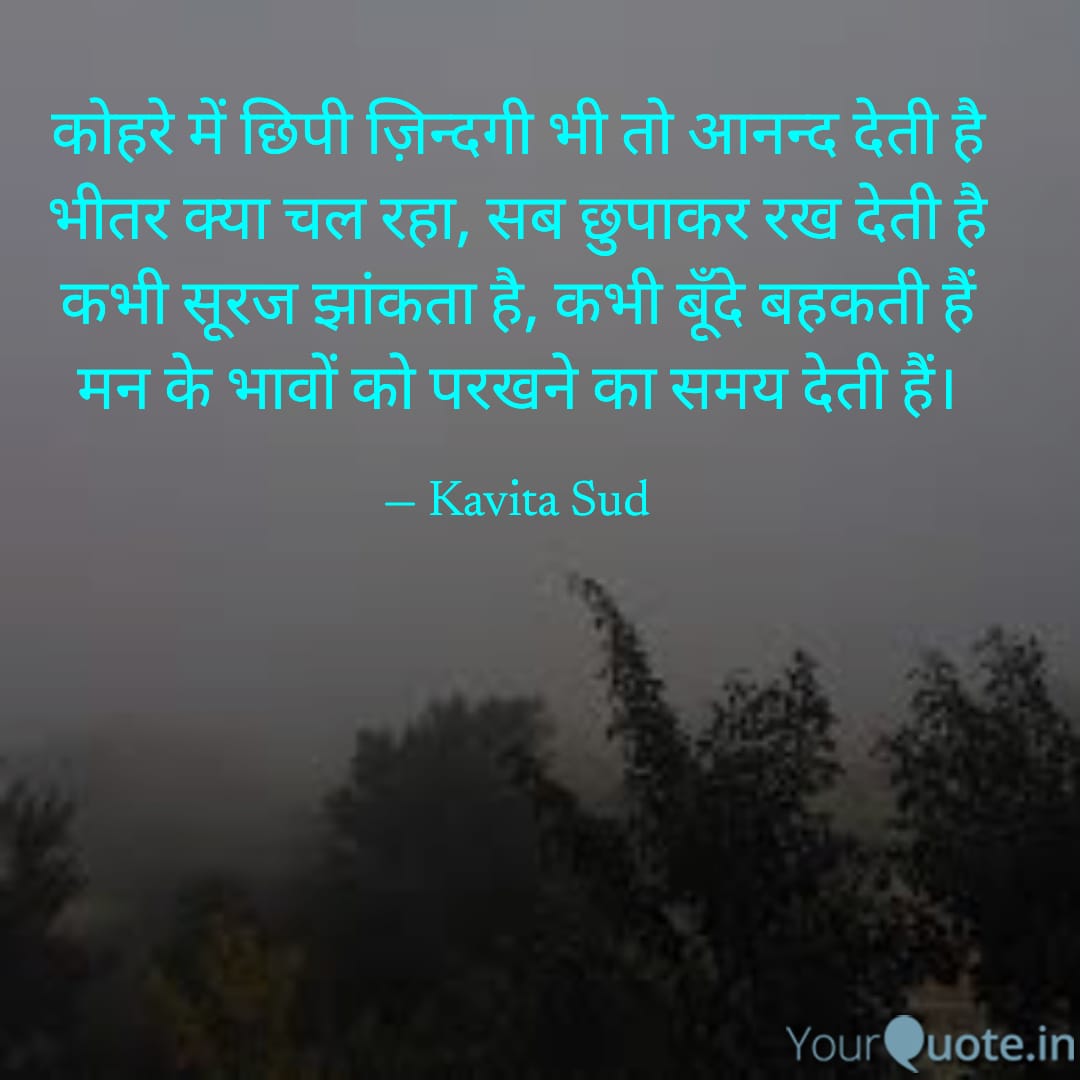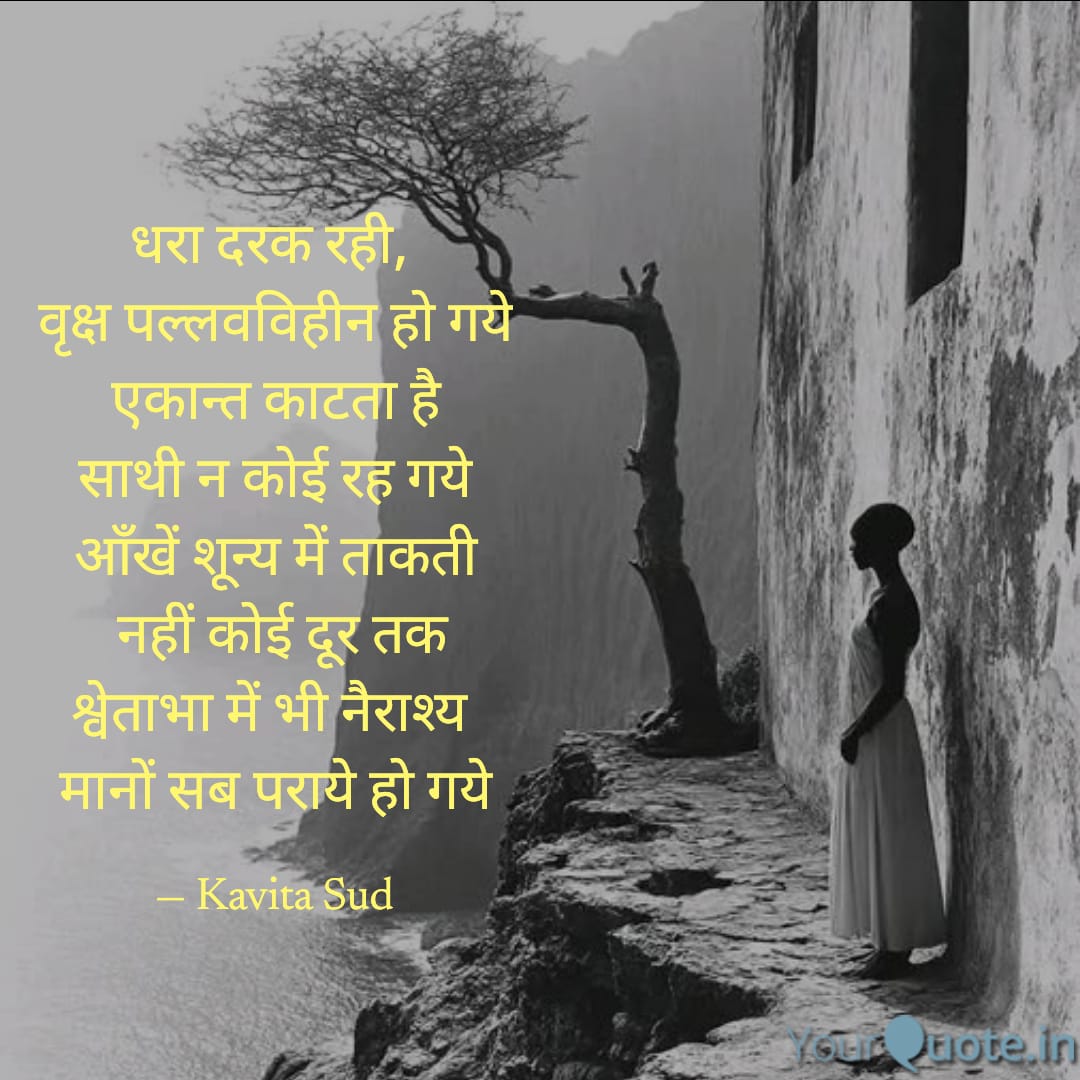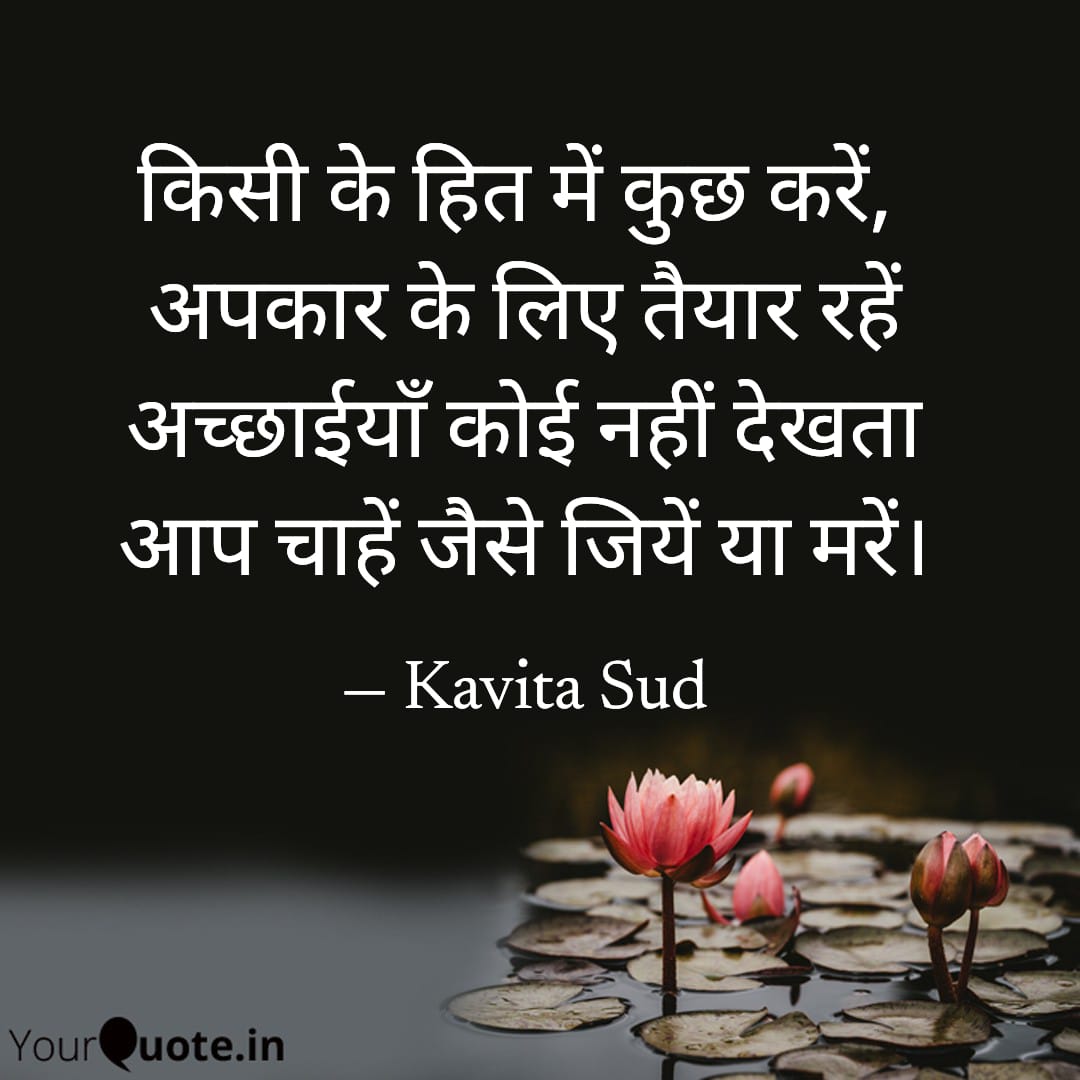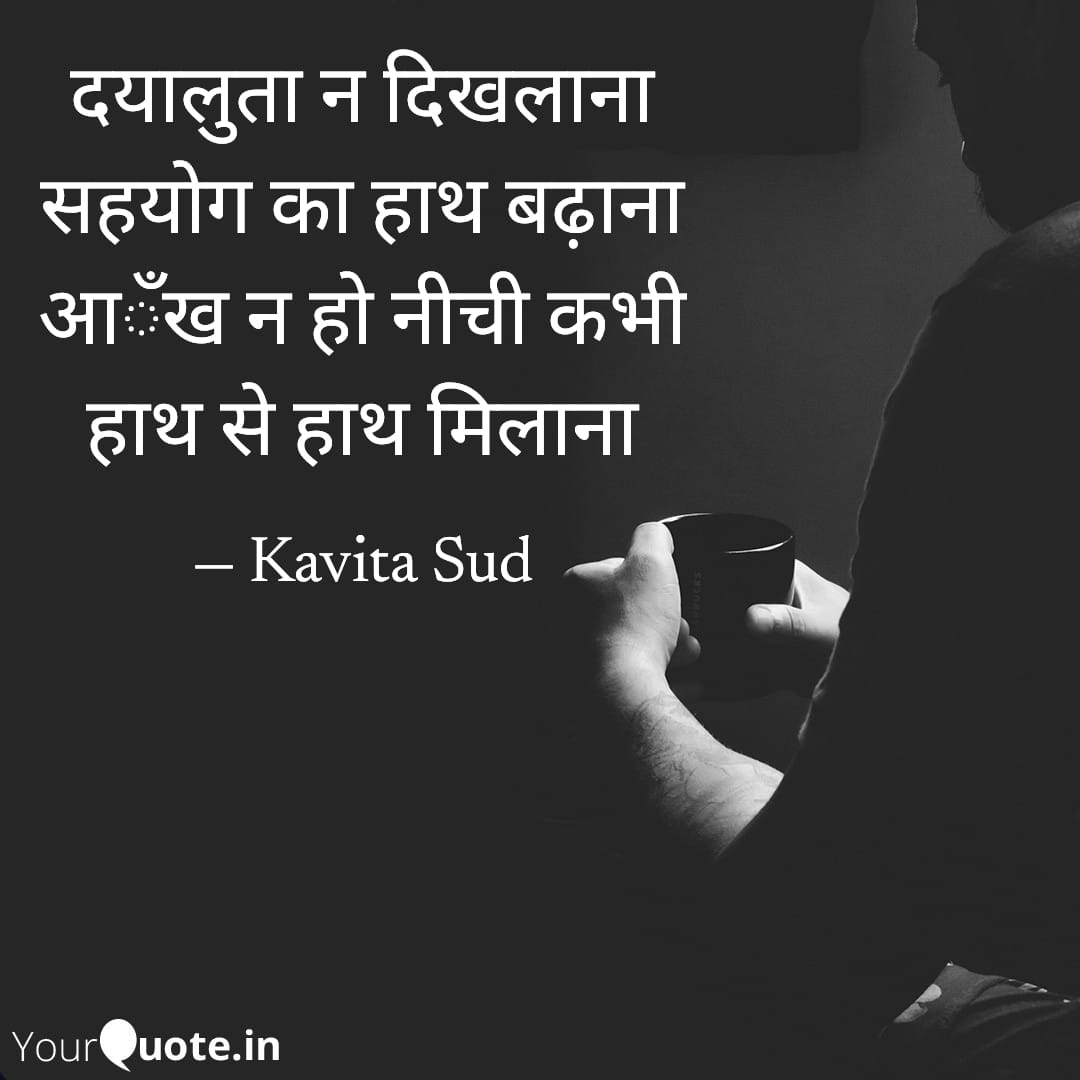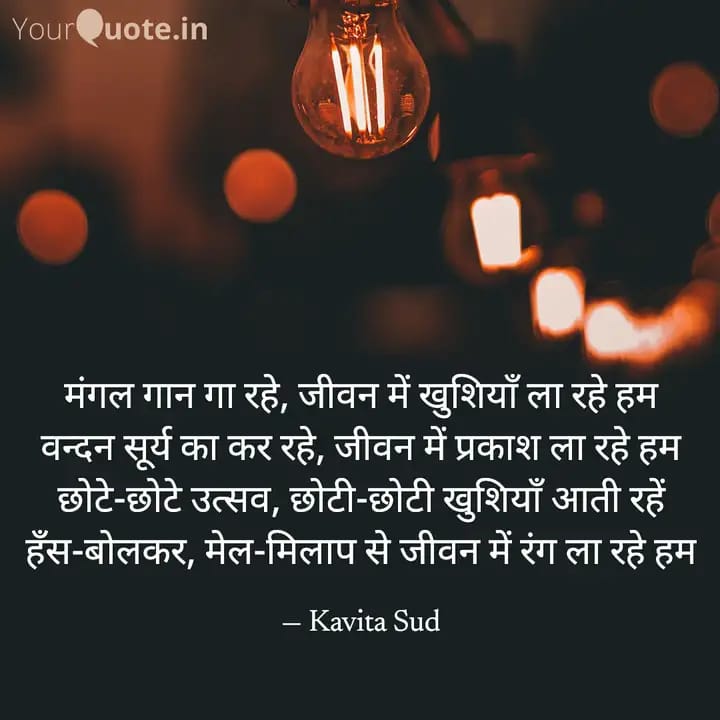ज़िन्दगी जीना भूल जाते हैं
ज़िन्दगी में
तप, उपासना, साधना
ज्ञान, ध्यान, स्नान
किसी काम नहीं आतीं।
जीवन भर करते रहिए
मरते रहिए
कब उपलब्धियाँ
कैसे हाथ से
सरक जायेंगी
पता ही नहीं लगता।
ज़िन्दगी जीने से ज़्यादा
हम न जाने क्यों
लगे रहते हैं
तप, उपासना, साधना में
और ज़िन्दगी जीना भूल जाते हैं
वह सब पाने के पीछे भागने लगते हैं
जिसका अस्तित्व ही नहीं।
आभासी दुनिया में जीने लगते हैं,
पारलौकिकता को ढूँढने में
लगे रहते हैं
और लौकिक संसार के
असीम सुखों से
मुँह मोड़ बैठते हैं
न जीवन जीते हैं
और न जीने देते हैं।
और अपने जीवन के
अमूल्य दिन खो देते हैं
वह सब पाने के लिए
जिसका अस्तित्व ही नहीं।
तेरा विश्वास
तेरा विश्वास
जब-जब किया
तब-तब ज़िन्दगी ने
पाठ पढ़ाया।
उस ईश्वर ने कहा
तुझे भी तो दिया था
एक दिमाग़
उसमें कचरा नहीं था,
बहुत कुछ था।
किन्तु
जब प्रयोग नहीं किया
तो वह
कचरा ही बन गया
अब दोष मुझे देते हो
कि
ऐसा साथ क्यों दिया।
समय यूँ ही बीत जाता है
एकान्त
कभी-कभी अच्छा लगता है।
सूनापन
मन में रमता है।
जल, धरा, गगन
मानों परस्पर बातें करते हैं,
जीवन छलकता है।
नाव रुकी, ठहरी-ठहरी-सी
परख रही हवाएँ
जीवन यूँ ही चलता है।
न अंधेरा, न रोशनी,
जीवन में धुंधलापन
बहकता है।
हाथों में डोरी
कुछ सवाल बुनती है
कभी उधेड़ती है
कभी समेटती है
समय यूँ ही बीत जाता है।
अंधेरे के बाद सवेरा
अंधेरे के बाद सवेरा !
ज़रूरी तो नहीं
रोशनी भी लेकर आये।
कभी-कभी
सवेरे भी अंधकारमय होते हैं।
सूरज बहका-बहका-सा
घूमता है।
किरणें कहीं खो जाती हैं।
भीतर ही भीतर
बौखला जाती हैं।
आंखें धुंधली हो जाती हैं,
दिखाई कुछ नहीं देता
किन्तु
हाथ बढ़ाने पर
अनदेखी रोशनियों से
हाथ जलने जाते हैं
अंधेरे और रोशनियों के बीच
ज़िन्दगी कहीं खो जाती है।
इच्छाओं का कोई अन्त नहीं
हमारी इच्छाओं का
कोई अन्त नहीं।
बालपन में
चिन्ताओं से दूर
मस्ती में जीते थे
किन्तु बड़ों को देखकर
आहें भरते थे।
कब बड़े होंगे हम।
बड़ों के स्वांग भर
खूब आनन्द लेते थे हम।
बड़े हुए
तो बालपन में
मन भटकने लगा
अक्सर कहते फ़िरते
आह! काश!
हम फिर बच्चे बन जायें।
और वृ़द्धावस्था क्या आई
सब कहने लगे
वृद्ध और बाल
तो समान ही होते हैं।
ऐसा नहीं होता रे
कोई मेरे मन से पूछे
इच्छाएँ कभी नहीं मरतीं
बालपन हो
युवावस्था अथवा वृद्धावस्था
चक्रव्यूह की भांति
जीवन भर उलझाये रखती हैं
जो मिला है,
वह भाता नहीं
जो नहीं मिला
वह जीवन-भर आता नहीं।
मन करता करूँ बात चाँद तारों से
मन करता करूँ बात चाँद तारों से।
न जाने कितने भाव
कितनी बातें
अनकही, सुलझी-अनसुलझी
भीतर-ही-भीतर
कचोटती हैं
बिलखती हैं
बहुत कुछ बोलती हैं।
किसी से कहते हुए
मन डरता है
कहीं कोई पूछ न ले
कोई बात की बात न हो जाये
कहीं पुराने ज़ख्म न खुल जायें
कहीं कोई अपनापन दिखाए
और हम शत्रुता का भाव पायें
न जाने किस बात का
कौन-सा अर्थ निकल आये
खुले गगन के नीचे
चाँद -तारों से बतियाती हूँ
मन की हर बात बताती हूँ ।
और गहरी नींद सो जाती हूँ ।
मृग-मरीचिका-सा जीवन
मृग-मरीचिका-सा जीवन
कभी धूप छलकती
कभी नदी बिखरती
कभी रेत संवरती।
कदम-दर-कदम
बढ़ते रहे।
जो मिला
ले लिया,
जो न मिला
उसी की आस में
चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे
कभी बिखरते रहे
कभी कण-कण संवरते रहे।
नई आस नया विश्वास
एक चक्र घूमता है जीवन का।
उर्वरा धरा
जीवन विकसित करती है।
बीज से अंकुरण होता है
अंकुरण से
पौधे रूप लेने लगते हैं
जीवन की आहट मिलती है।
डालियाँ झूमती हैं
रंगीनियाँ बोलती हैं
गगन देखता है
मन इस आस में जीता है,
कुछ नया मिलेगा
जीवन आगे बढ़ेगा।
मानों धन-धान्य
बिखरता है इन डालियों में,
पुनः धरा में
और अंकुरित होती है नई आस
नया विश्वास।
जीवन का सच
महाभारत का यु़द्ध
झेलने के लिए
किसी से लड़ना नहीं पड़ता
बस अपने-आपको
अपने-आपसे
भीतर-ही-भीतर
मारना पड़ता है।
शायद
यही नियति है
हर औरत की।
कृष्ण क्या संदेश दे गये
सुनी-सुनाई बातें हैं सब।
कर्म किये जा
फल की चिन्ता मत कर।
कौन पढ़ता है आज गीता
कौन करता है वाचन
कृष्ण के वचनों का।
जीवन का सच
अपने-आपसे ही
झेलना पड़ता है
अपने-आपसे ही
जीना
और अपने-आपको ही
मारना पड़ता है।
अकेला ही चला जा रहा है आदमी
अपने भीतर
अपने-आपसे ही कट रहा है आदमी।
कहाँ जायें, कैसे जायें
कहाँ समझ पर रहा है आदमी।
टुकड़ों में है जीवन बीत रहा
बस
ऐसे ही तो चला जा रहा है आदमी।
कुछ काम का बोझ,
कुछ जीवन की नासमझी
कहाँ कोई साथ देता है
बस अकेला ही चला जा रहा है आदमी।
पानी की गहराई
नहीं जानता है
इसलिए पत्थरों पर ही
कदम-दर-कदम बढ़ रहा है आदमी।
देह कब तक साथ देगी
नहीं जानता
इसलिए देह को भी मन से नकार रहा है आदमी।
याद आते हैं वे दिन
याद आते हैं वे दिन जब सखियों संग स्कूल से आया करते थे
छीन-छीनकर एक-दूजे की रोटी आनन्द से खाया करते थे
राह चलते कभी खटमिट खाई, कभी खुरमानी तोड़ा करते थे
राहों में छुपन-छुपाई, गुल्ली-डंडा, लम्बी दौड़ लगाया करते थे
रस्सी-टप्पा, गिट्टे, उंच-नीच, स्टापू, जाने कितने खेल जमाया करते थे
पुरानी कापियाँ दे-देकर गोलगप्पे, चूरन, पापड़ी खाया करते थे
बारिश में भीग-भीगकर, छप्पक-छप्पक पानी उड़ाया करते थे
चलते-चलते जब थक जाते थे, बैग रख सो जाया करते थे
एक-दूसरे की कापियों की नकल कर होमवर्क कर लिया करते थे
याद आये वे दिन जब सखियों संग धमा-चैकड़ी मचाया करते थे
न जाने कौन कहाँ है आज याद नहीं, कुछ यादें रह गई हैं बस
कभी मिलेंगीं भी तो कहाँ पहचान होगी, क्यों सोच रही मैं आज
वे सड़कें, वे स्कूल, वो मस्तियाँ, लड़ना-झगड़ना, कुट्टी-मिट्टी
कभी-कभी बचपन के वे बीते दिन यूँ ही याद आ जाया करते थे
रंगों में भी इक महक होती है
रंगों में भी इक महक होती है, मन बहकाती है
अस्त होते सूर्य की गरिमा मन पर छा जाती है
कहीं कुमकुम-से, कहीं इन्द्रधनुषी रंग बिखर रहे
सागर के जल में रंगों की परछाईयाँ मन मोह जाती हैं
देख रहे त्रिपुरारी
भाल तिलक, माथ चन्द्रमा, गले में विषधर भारी
गौरी संग नयन मूंदकर जग देख रहे त्रिपुरारी
नेह बरसे, मन सरसे, देख-देख मन हरषे
विषपान किये, भागीरथी संग देखें दुनिया सारी
रोशनियाँ खिलती रहें
कदम बढ़ते रहें, जीवन चलता रहे, रोशनियाँ खिलती रहें
शाम हो या सवेरा, आस और विश्वास से बात बनती रहे
कहीं धूप खिली, कहीं छाया, कहीं बदरी छाये मन भाये
विश्राम क्या करना, जब साथ हों सब, खुशियाँ मिलती रहें
संगम का भाव
संगम का भाव मन में हो तो गंगा-घाट घर में ही बसता है
रिश्तों में खटास हो तो मन ही भीड़-तन्त्र का भाव रचना है
वर्षों-वर्षों बाद आता है कुम्भ जहाँ मिलते-बिछड़ते हैं अपने
ज्ञान-ध्यान, कहीं आस-विश्वास, इनसे ही जीवन चलता है
कोहरे में छिपी ज़िन्दगी
कोहरे में छिपी ज़िन्दगी भी तो आनन्द देती है
भीतर क्या चल रहा, सब छुपाकर रख देती है
कभी सूरज झांकता है, कभी बूँदे बहकती हैं
मन के भावों को परखने का समय देती हैं।
रोशनियाँ अंधेरों में भटक रही हैं
देखना ज़रा, आज रोशनियाँ अंधेरों में भटक रही हैं
पग-पग पर कंकड़-पत्थर हैं, पैरों में अटक रही हैं
न अंधेरे मिले सही से, न रोशनियों ने राह दिखाई
जीवन की गति इनकी ही पहचान में सटक रही है
मन में अब धीरज कहाँ रह गया
मन में अब धीरज कहाँ रह गया
पल-पल उलझनों में बह गया
मन का मौसम भी तो बदल रहा
पता नहीं कौन क्या-क्या कह गया
स्वार्थ का मुखौटा
किसी को कौन कब यहाँ पहचानता है
स्वार्थ का मुखौटा हर कोई पहनता है
मुँह फ़ेर कर निकल जाते हैं देखते ही
बस अगले-पिछले बदले निकालता है।
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचनाकार
यह विधाता,
जगत-नियन्ता
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचनाकार।
इसकी कुछ बातें मुझे
समझ ही नहीं आतीं।
इतने बड़े ब्रह्माण्ड का निर्माण किया
करोड़ों जीव-जन्तु बनाये
कितना श्रम किया होगा
कितना तो समय लगा होगा
शायद अरबों-खरबों वर्ष।
फिर उनकी देख-भाल
नवीनीकरण, और पता नहीं क्या-क्या।
किन्तु इतनी बड़़ी भूल
कैसे हो सकती है।
विज्ञान कहता है
जब बच्चा जन्म लेता है
तो उसके शरीर में
300 हड्डियाँ होती हैं
जो कालान्तर में 206 में
बदल जाती हैं।
और 300 हड्डियों को
लगाते-लगाते
जिह्वा में हड्डी लगाना ही भूल गये।
.
शायद, इसीलिए
अकेली जिह्वा ही
ज़रा-सा हिलकर
206 हड्डियों वाले
किसी भी ढांचे की
चूर-चूर, चकनाचूर
करने की क्षमता रखती है।
एकान्त काटता है
धरा दरक रही, वृक्ष पल्लवविहीन हो गये
एकान्त काटता है, साथी न कोई रह गये
आँखें शून्य में ताकती, नहीं कोई दूर तक
श्वेताभा में भी नैराश्य मानों सब पराये हो गये
दर्द का अब घूँट पिये
पुण्य करने गये थे, अपनों को साथ आस लिए
हाथ छूटे, साथ छूटे, कितने रहे, कितने जिये
नाम नहीं, पहचान नहीं, लाखों की भीड़ रही
अपनों को कहाँ खोजें, दर्द का अब घूँट पिये
जियें या मरें
किसी के हित में कुछ करें,
अपकार के लिए तैयार रहें
अच्छाईयाँ कोई नहीं देखता
आप चाहें जैसे जियें या मरें।
दयालुता न दिखलाना
दयालुता न दिखलाना
सहयोग का हाथ बढ़ाना
आँख न हो नीची कभी
हाथ से हाथ मिलाना
ऐसा नहीं होता
पता नहीं कौन कह गया
बूंद-बूंद से सागर भरता है।
सुनी-सुनाई पर
सभी कह देते हैं।
कभी देखा भी है सागर
उसकी गहराई
उसकी तलछट
उसके ज्वार-भाटे।
यहाँ तो बूंद-बूंद से
घट नहीं भरता
सागर क्या भरेगा।
कहने वालो
कभी आकर मिलो न
सागर क्या
मेरा घट ही भरकर दिखला दो न।
मंगल गान गा रहे
मंगल गान गा रहे, जीवन में खुशियाँ ला रहे हम
वन्दन सूर्य का कर रहे, जीवन में प्रकाश ला रहे हम
छोटे-छोटे उत्सव, छोटी-छोटी खुशियाँ आती रहें
हॅंस-बोलकर, मेल-मिलाप से जीवन में रंग ला रहे हम
कोहरे में दूरियाँ
कोहरे में दूरियाँ दिखती नहीं हैं, नज़दीकियाँ भी तो मिटती नहीं हैं
कब, कहाँ, कौन, कैसे टकरा जाये, दृष्टि भी स्पष्ट टिकती नहीं है
वेग पर नियन्त्रण, भावनाओं पर नज़र रहे, रुक-रुककर चलना ज़रा
यही अवसर मिलता है समझने का, अपनों की पहचान मिटती नहीं है
संस्मरण: धर्मशाला साहित्यिक आयोजन
26 नवम्बर। धर्मशाला। पर्वत की गूंज द्वारा प्रकाशित हिमतरु दशहरा-दीपावली विशेषांक के लोकार्पण का अवसर। इसमें मेरा भी एक आलेख है। रेडियो गुंजन सिद्धवाड़ी धर्मशाला। एक सुखद अनुभव।
पर्वत की गूंज के संस्थापक, संचालक राजेन्द्र पालमपुरी जी का एक संदेश मिला कि धर्मशाला में इस हेतु एक छोटा-सा आयोजन है । यदि मैं आना चाहूं। मेरा विचार था कि आयोजन छोटा या बड़ा नहीं होता, अच्छा होता है और अच्छे लोगों से, अच्छे साहित्यकारों से मिलने के लिए होता है।
इसलिए कार्यक्रम बना लिया। ठहरने की व्यवस्था के लिए पालमपुरी जी से ही अनुरोध किया। कैलाश मनहास जी ने Dadhwal Bnb homestay में रहने की व्यवस्था करवाई। बहुत ही अच्छी।
बहुत सुन्दर, सादगीपूर्ण एवं गरिमामयी आयोजन का हिस्सा बनकर मन को बहुत अच्छा लगा। एक अपनत्व भरा कार्यक्रम। कुछ पहाड़ी कविताएं भी सुनने को मिलीं। पहाड़ी कविताओं को सुनने का अपनी ही आनन्द है। अनेक बाल कवि हिमाचल के विभिन्न भागों से उपस्थित थे और उन्हें भी सम्मानित किया गया। शायद 1990 के बाद हिमाचल में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिमला मेरे भीतर बसता है और हिमाचल मुझे आकर्षित करता है। इसलिए इस अवसर को तो मैं जाने ही नहीं देना चाहती थी। इस सुन्दर आयोजन के लिए सभी मनीषियों का धन्यवाद एवं आभार।
छन्दमुक्त कविताएॅं
मैं किसी विवादास्पद विषय पर लिखने अथवा प्रतिक्रिया से बचकर चलती हूं। किन्तु कभी-कभी कुछ चुभ भी जाता है। फ़ेसबुक पर हम सब लिखने के लिए स्वतन्त्र हैं। किन्तु इतना भी न लिखें कि सीधे-सीधे अनर्गल आक्षेप हों। कुछ अति के महान लेखक यहां विराजमान हैं। सैंकड़ों मंचों के सदस्य हैं, सैंकड़ों सम्मान प्राप्त हैं। सुना है और उनकी बातों से लगता है कि वे महान छन्द विधाओं में लिखते हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं। इस कारण वे सामूहिक रूप से किसी का भी, विशेषकर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं। आपकी मित्र-सूची में भी होंगे, पढ़िए उनका लेख और अपने विचार दीजिए। मुझे लगता है इन महोदय को बड़े दिन से कोई सम्मान नहीं मिला अथवा किसी काव्य समारोह का निमन्त्रण तो भड़ास तो कहीं निकालनी ही थी। और ऐसे महान छन्दलेखक की भाषा! वाह!!! वे इतने महान हैं कि वे तय करेंगे कि कौन कवि है और कौन कवि नहीं।
वैसे वाह-वाही पाने और हज़ारों लाईक्स पाने का भी यह एक तरीका आजकल फ़ेसबुक पर चल रहा है कि आप जितना ही अनर्गल लिखेंगे उतने ही लाईक्स मिलेंगे।
वे लिखते हैं
“आज अगर यह मुक्त छंद वाली कविता या उल जुलूल बेसिर पैर के गद्य को कविता की श्रेणी से निकाल दिया जाय तो 90 प्रतिशत कवि इस सोशल मीडिया से गायब हो जायेंगे जिनमें 80 प्रतिशत महिला कवियत्री औऱ बाकी के पुरुष कवि कहलाने वाले लोग हैं ।”
छंद मुक्त लेखकों या अगड़म बगड़म गद्य को इधर इधर करके कविता नाम देने वाले स्त्री पुरुषों को तो मैं कवियों की श्रेणी में रखता ही नहीं ।
आप ऐसे समझिये कि जिसको कुछ नहीं आता, वह छंदमुक्त के नाम से लेखन कर कवि बन जाता है ।
जैसे जिसको कुछ नहीं आता या जिसमें कोई गुण नहीं, तो उससे कहा दिया जाता है कि चलो तुम laterine ही साफ कर दो ।“”
मैं मान लेती हूं कि छन्दमुक्त लिखने वाले कवि नहीं हैं तो सबसे पहले तो निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह, केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विमल, गिरिजाकुमार माथुर आदि अनेक कवियों को हिन्दी साहित्य से बाहर कर देना चाहिए।
महिलाओं के परिधान
हमारे समाज में महिलाओं के परिधान की अनेक तरह से बहुत चर्चा होती है। वय-अनुसार, पारिवारिक पोस्ट के अनुसार, अर्थात अविवाहित युवती, भाभी, ननद, बहन, माँ, दादी आदि के लिए। इसके अतिरिक्त भारत में रीति-परम्पराओं, राज्यानुसार प्रचलित, एवं धार्मिक आख्यानों में भी इतनी विविधता है कि उसके अनुसार भी महिलाओं के वस्त्रों पर दृष्टि रहती है।
और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे आधुनिक समाज में महिलाओं के परिधानों के अनुसार ही उनका चरित्र-चित्रण किया जाता है। आधुनिक वस्त्र धारण करने वाली युवती के लिए मान लिया जाता है कि यह बहुत तेज़ होगी, घर-गृहस्थी के योग्य नहीं होगी, पति, सास-ससुर की सेवा करने वाली नहीं होगी। ( किन्तु जब महिलाओं की बात होती है तब सेवा-भाव वाली बात आती ही क्यों है, उसके अपने अस्तित्व की बात क्यों नहीं की जाती। परिवार के सदस्य की बात क्यों नहीं आती?, पुरुषों के सन्दर्भ में तो इस तरह की बात कभी नहीं आती। इस विषय पर चर्चा को विराम देती हूँ, यह भिन्न चर्चा का विषय है।)
किन्तु पुरुषों के परिधान, वस्त्रों पर कभी कोई बात नहीं करता।
क्योंकि महिलाएं खुलेआम टिप्पणी नहीं कर पातीं इस कारण कहती नहीं।
सबसे बुरा लगता है जब पुरुष केवल अन्तर्वस्त्रों में अथवा तौलिए में प्रातःकाल बरामदे में घूमते दिखते हैं। गर्मियों में तो जैसे उनका अधिकार होता है अर्द्धनग्न रहना। मुझे नहीं पता कि उनके घर की महिलाएं उन्हें टोकती हैं अथवा नहीं।
मैं शिमला से हूँ। वहां हमने सदैव ही यही देखा है कि पुरुष भी महिलाओं की भांति स्नानागार से पूरे वस्त्रों में ही तैयार होकर निकलते हैं। किन्तु जब मैं यहां आई तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि घर के बच्चे क्या, युवा, अधेड़, बुजुर्ग सब आधे-अधूरे कपड़ों में घूमते हैं। हमें यह अश्लील लगता है। अभिनेत्रियों के वस्त्रों पर भी बहुत कुछ लिखा जाता है किन्तु जब बड़े.बड़े मंचों पर बड़े नामी कलाकार नग्न प्रदर्शन करते हैं तब वह भव्यता होती है। इन नग्नता की तुलना हम किसी कार्य या खेल में पहने जाने वस्त्रों से नहीं कर सकते।
पुरुष की वस्त्रहीनता उसका सौन्दर्य है और स्त्री के देह-प्रदर्शनीय वस्त्र अश्लीलता।
सबसे बड़ी बात जो मुझे अचम्भित भी करती है और हमारे समाज की मानसिकता को भी प्रदर्शित करती है वह यह कि हमारे प्रायः सभी प्राचीन पात्रों के चित्रों में उपरि वस्त्र धारण नहीं दिखाये जाते। फिर वह चित्रकारी हो अथवा अभिनय। किसने देखा है वह काल कि ये लोग उपरि वस्त्र पहनते थे अथवा नहीं। क्यों यह अश्लीलता नहीं दिखती और कभी भी क्यों इस पर आपत्ति नहीं होती। निश्चित रूप से उस युग को तो किसी ने नहीं देखा, यह हमारी ही मानसिकता का प्रतिफल है। किसने देखा है कि पौराणिक, अथवा अनदेखे काल के लोग कैसे वस़्त्र पहनते थे, क्या पहनते थे। यह उस कलाकार की अथवा भक्त की मानसिकता है जो अपने आराध्य की सुन्दर, सुघड़ देहयष्टि दिखाना चाहता है।
महिलाएं पुरुषों के पहनावे से आहत होती हैं। प्रकृति ने पुरुष को छूट दी है, यह हमारी सोच है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब हम महिलाएं भी उसी बनी.बनाई लीक पर चलती हैं।
एक अन्य तथ्य यह कि जब भी भारतीय संस्कृति, परम्पराओं, रीति-रिवाज़ों के अनुसार पहनावे की बात उठती है तब केवल महिलाओं के सन्दर्भ में ही चर्चा होती है, पुरुषों के पहरावे पर कोई बात नहीं की जाती।
इतना और कहना चाहूंगी कि कमी पुरुषों की मानसिकता में नहीं महिलाओं की मानसिकता में है जो पुरुष नग्नता का विरोध नहीं करतीं।