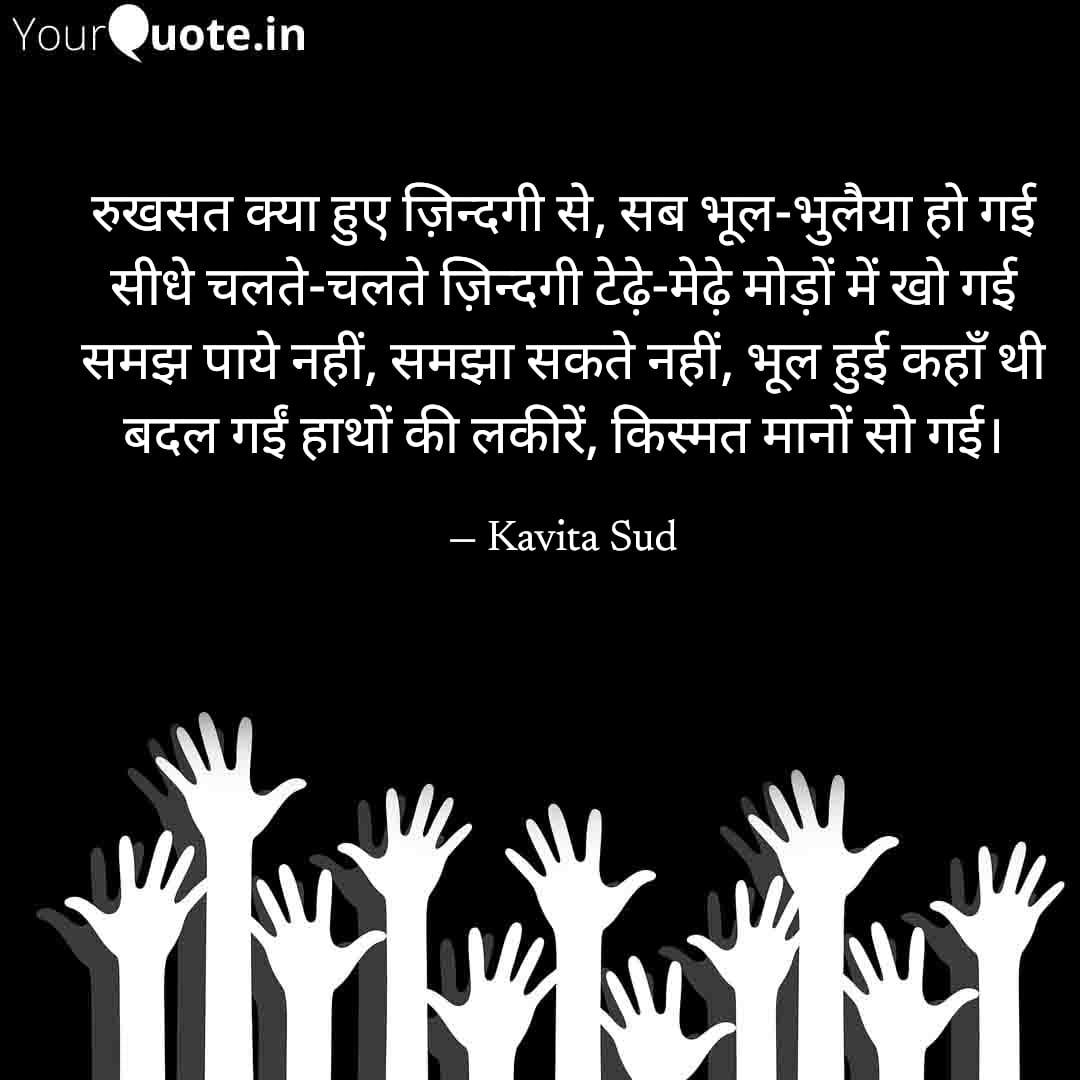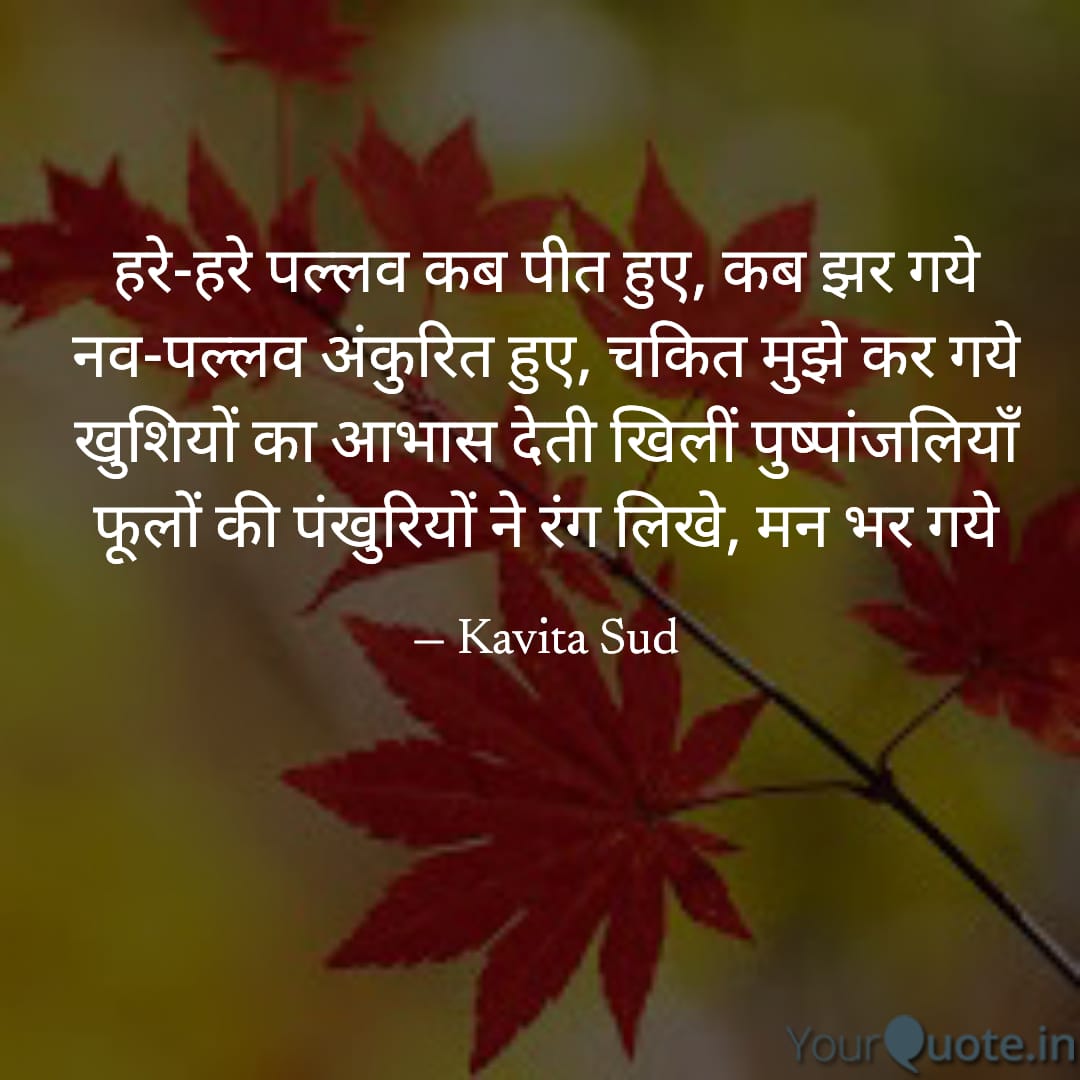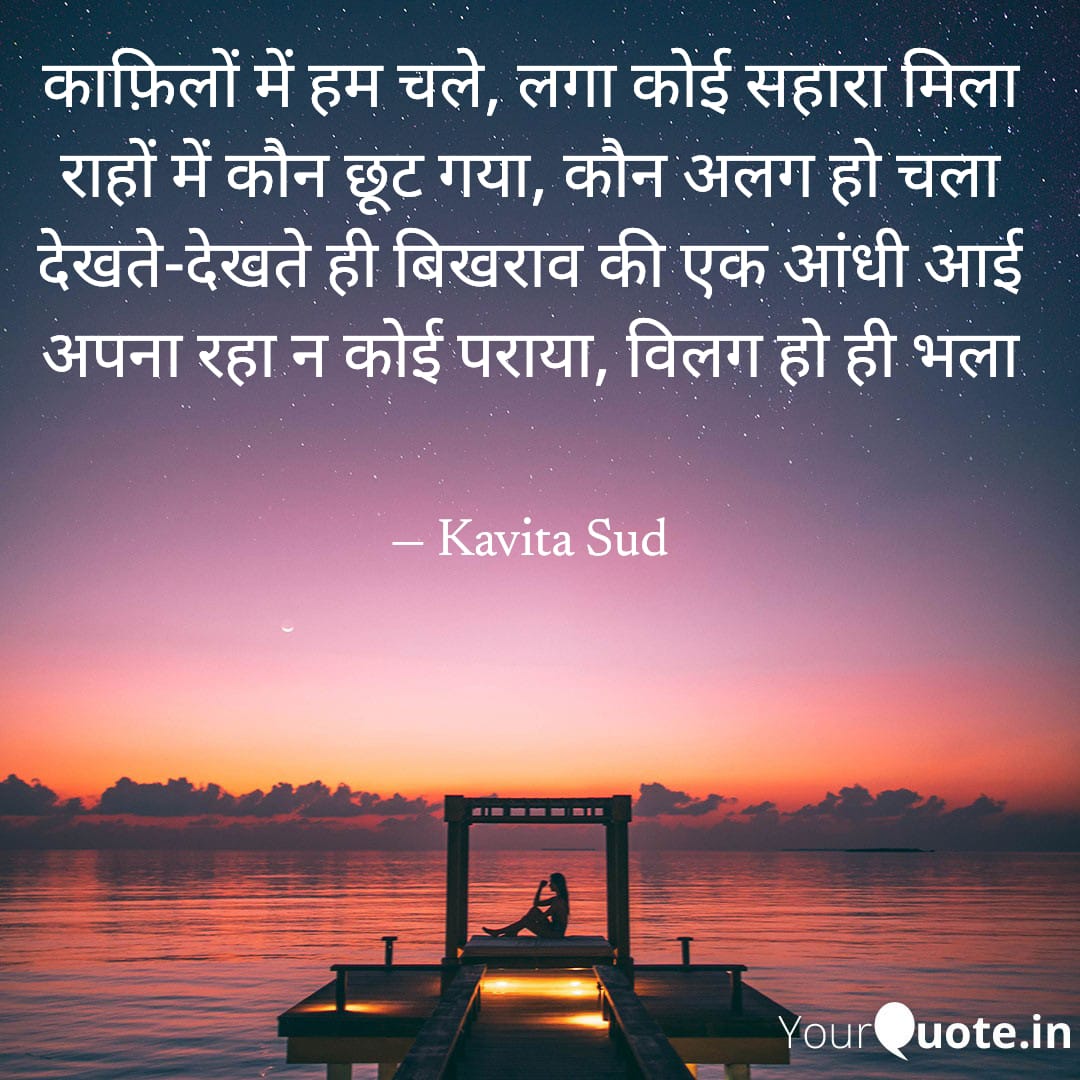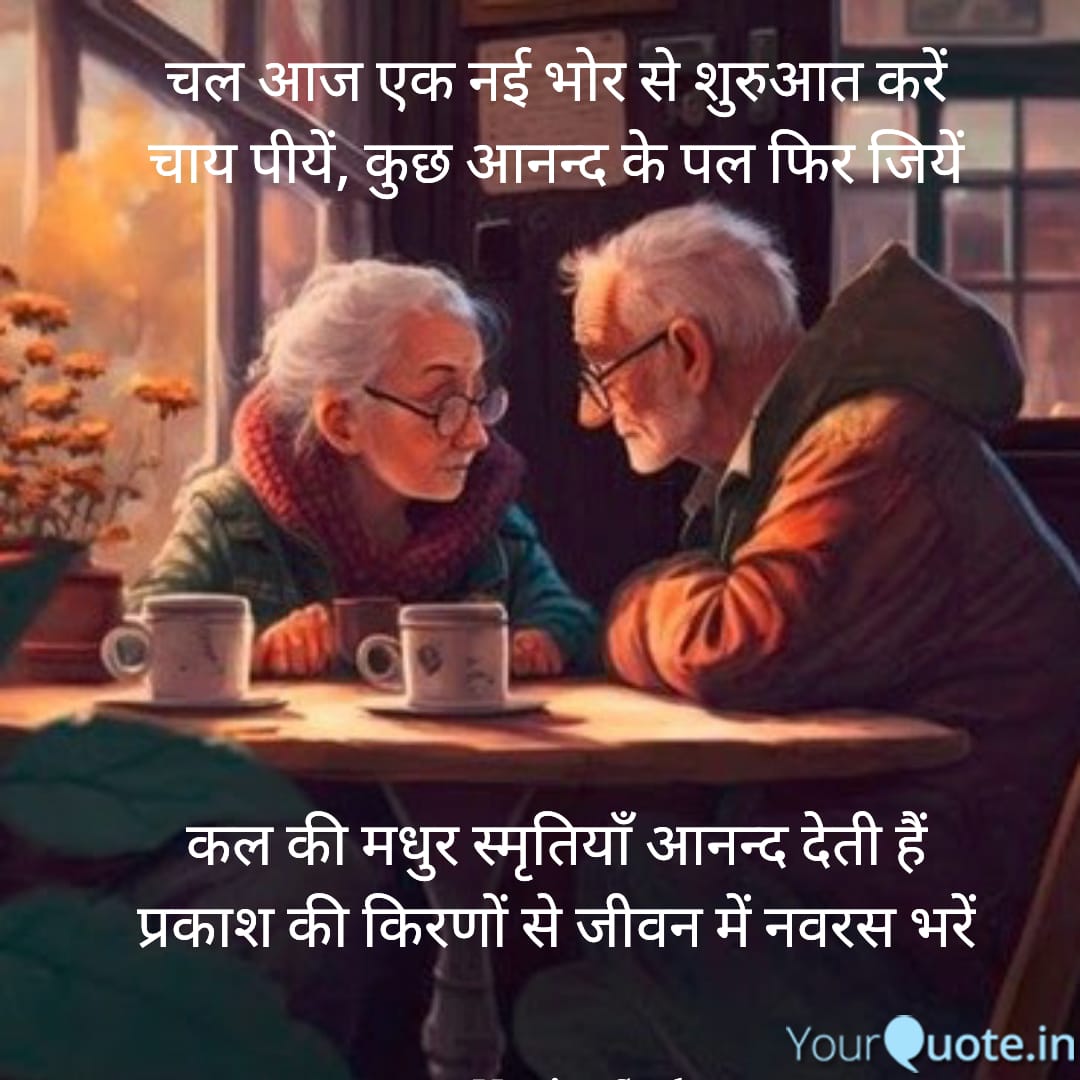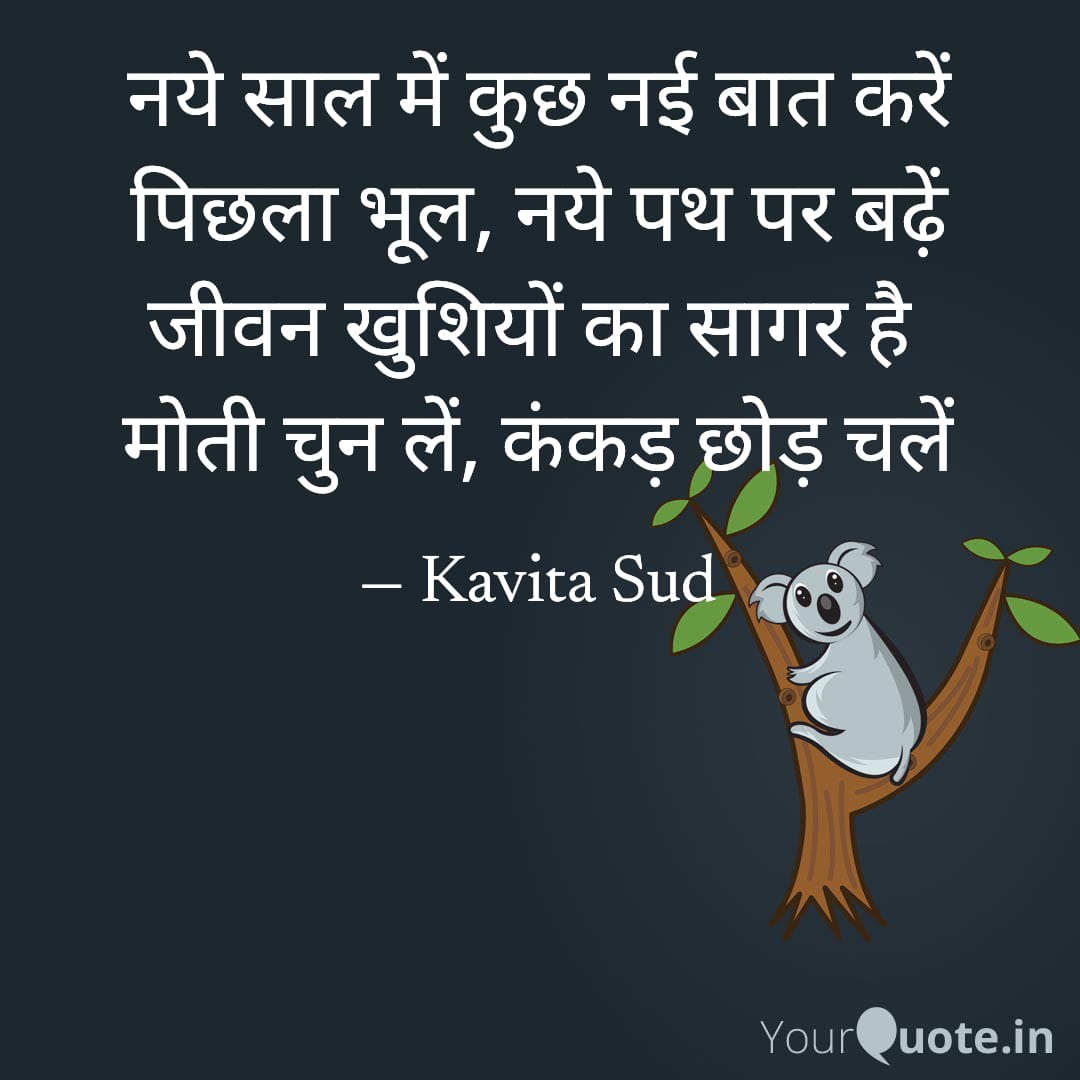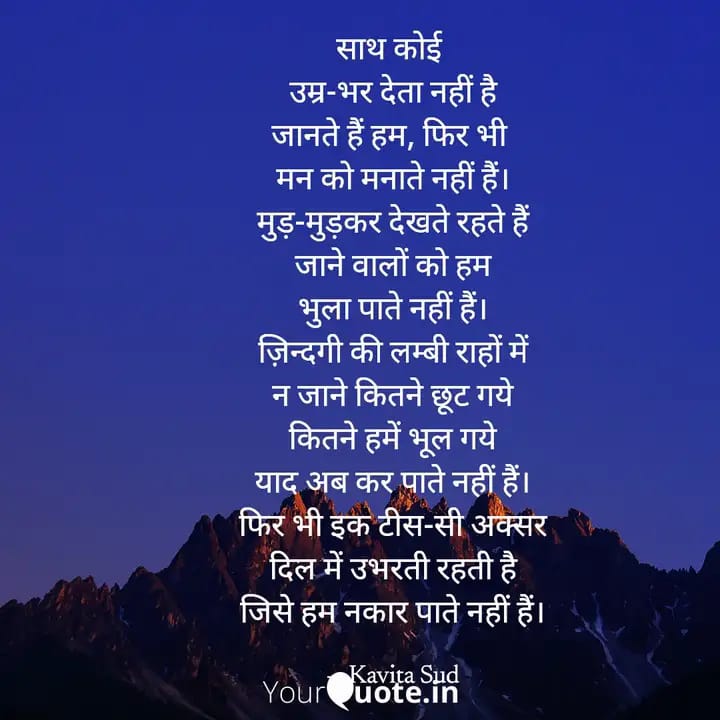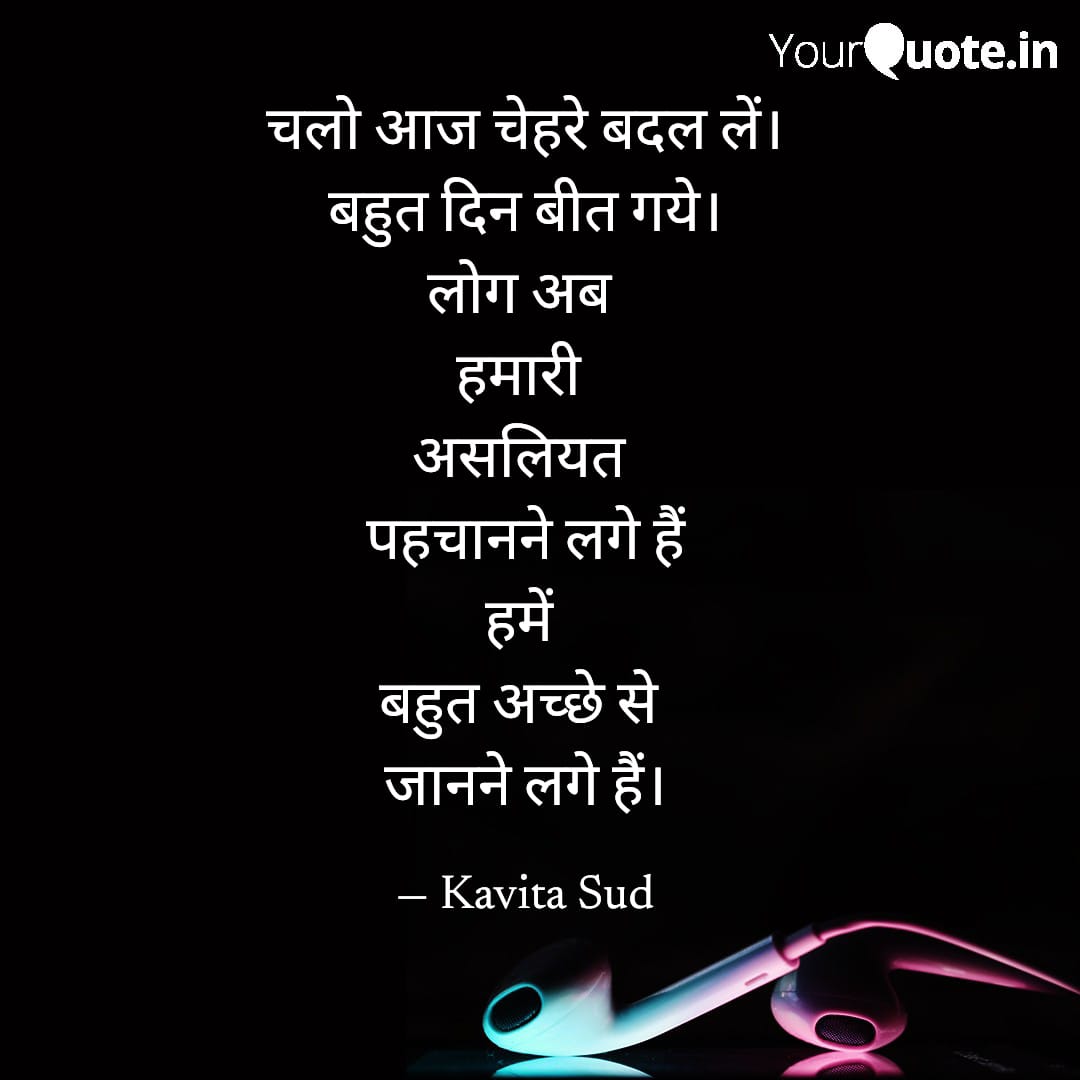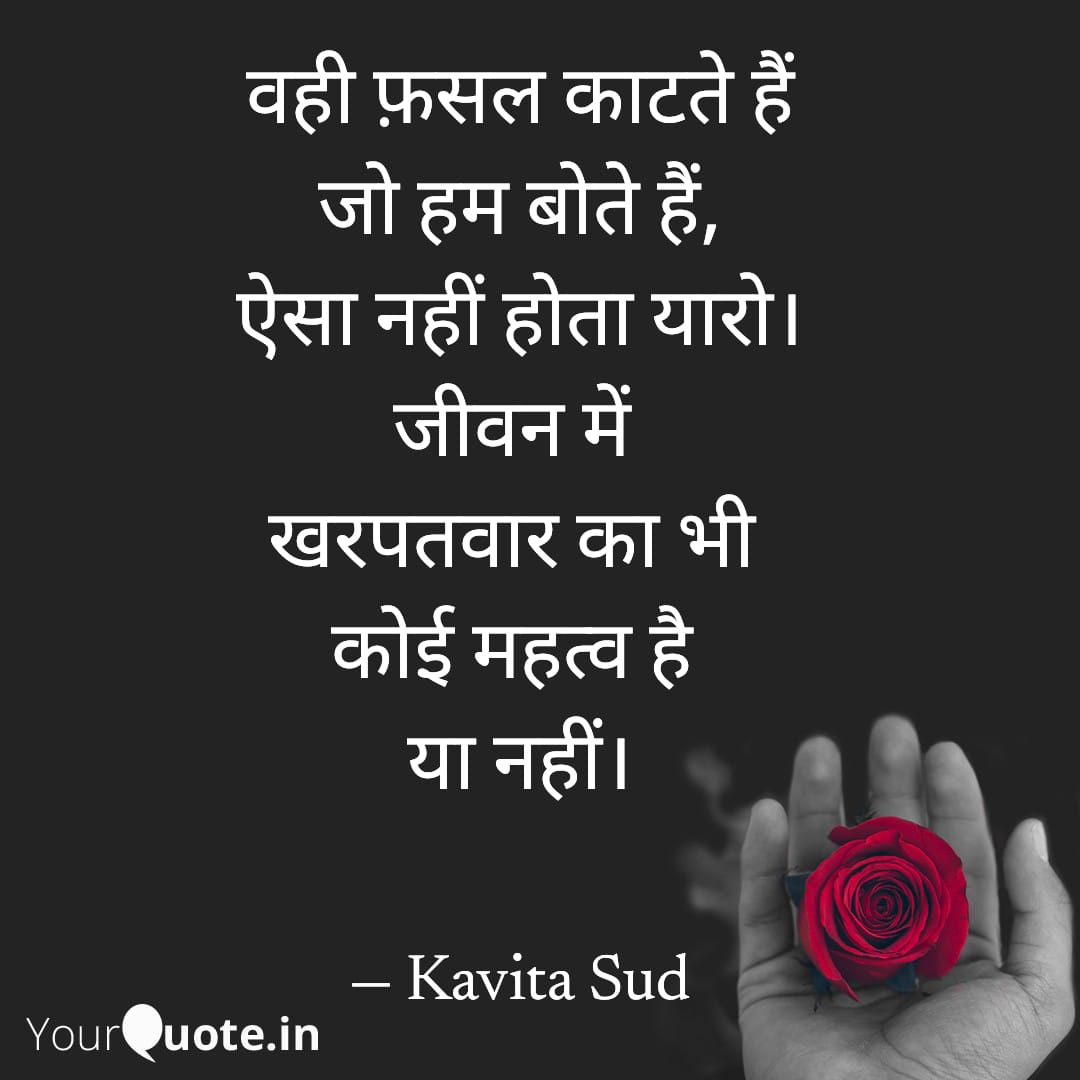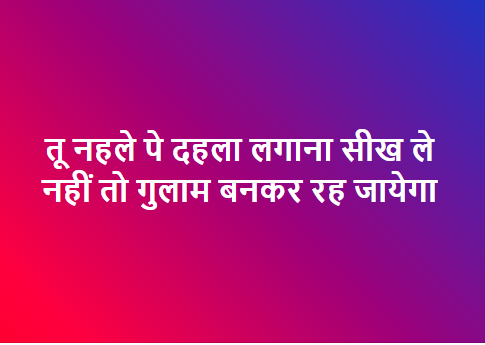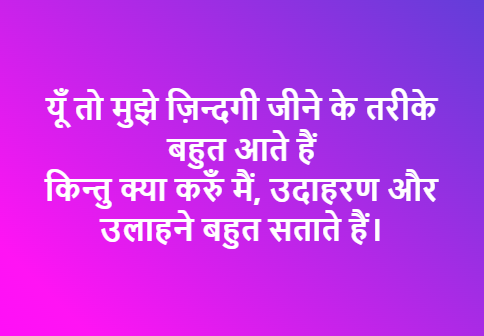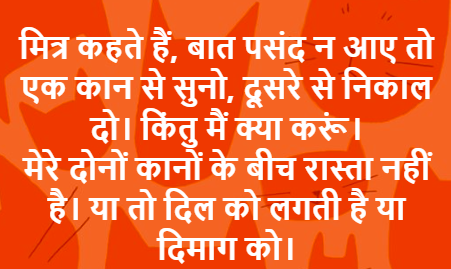भूल हुई कहाॅं थी
रुखसत क्या हुए ज़िन्दगी से, सब भूल-भुलैया हो गई
सीधे चलते-चलते ज़िन्दगी टेढ़े-मेढ़े मोड़ों में खो गई
समझ पाये नहीं, समझा सकते नहीं, भूल हुई कहाॅं थी
बदल गईं हाथों की लकीरें, किस्मत मानों सो गई।
नयानाभिराम रूप रघुराई
राम-लखन संग-संग चले, अयोध्या नगरी मुस्काई
दीपों की आभा से आलोकित सब जन-मन हरषाई
हर मन में उल्लास है, मधुर गान से नभ गूंज रहा
गगन-धरा सब निरख रहे, नयानाभिराम रूप रघुराई
प्रदर्शन का दर्शनn
पर्व अब प्रदर्शन बनकर रह गये हैं
प्रदर्शन का दर्शन बनकर रह गये हैं
उपहारों का लेन-देन प्रथा बन गई
बाज़ारीकरण में रिश्ते कहाॅं रह गये हैं
फ़ागुन की आहट
फ़ागुन की आहट
मानों जीवन में
मधुर सी गुनगुनाहट
हवाओं में फूलों की महक
नव-पल्लव अंकुरित
वृक्षों की शाखाओं से
पंछियों की
मधुर कलरव
पत्तों की मरमर
तृण मानों
ओस की बूंदों से
कर रहे शरारत।
भीगा-भीगा-सा मौसम
कभी धूप कभी छांव
कहता है
ले ले आनन्द
पता नहीं
फिर कब मिलेगा यह जीवन।
खुशियों का आभास देती
हरे-हरे पल्लव कब पीत हुए, कब झर गये
नव-पल्लव अंकुरित हुए, चकित मुझे कर गये
खुशियों का आभास देती खिलीं पुष्पांजलियाॅं
फूलों की पंखुरियों ने रंग लिखे, मन भर गये
शक्ति-स्वरूपा
दिव्य आलोकित रूप तुम्हारा मन हर्षित करता है
हाथों में त्रिशूल देखकर मन में साहस भरता है
भोली-सी मुस्कान तुम्हारी आशीष की भांति लगती है
शक्ति-स्वरूपा हो तुम, अरि भी तुमसे डरता है।
सुहाना दिन
भोर की रंगीनीयाॅं मदमाती हैं
सूर्य रश्मियाॅं मन भरमाती हैं
सुहाना दिन आया जीवन में
भावों की कलियाॅं शरमाती हैं
कोई नहीं अपना
काफ़िलों में हम चले, लगा कोई सहारा मिला
राहों में कौन छूट गया, कौन अलग हो चला
देखते-देखते ही बिखराव की एक आंधी आई
अपना रहा न कोई पराया, विलग हो ही भला
नई शुरुआत
चल आज एक नई भोर से शुरुआत करें
चाय पीयें, कुछ आनन्द के पल फिर जियें
कल की मधुर स्मृतियाॅं आनन्द देती हैं
प्रकाश की किरणों से जीवन में नवरस भरें
चित्राधारित कथा
आज सबके पास घड़े और बाल्टियां तो थीं किन्तु खाली थीं। धूप और सूखी धरती पर चलते-चलते उनके पांव थक गये थे। गांव में एक ही कुंआ था आम लोगों के लिए और गर्मी आते ही पानी की कमी होने लगती थी और दूसरे कुंए और नहर के पानी पर उनका अधिकार नहीं था। आज कुंए से पानी खिंचा ही नहीं। सभी महिलाएं उदास थीं। कैसे खाना बनायेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे।
उन्होंने मिलकर तय किया कि वे सरपंच से जाकर मिलेंगी और जब तक उन्हें नहर के पानी और दूसरे कुंए से पानी नहीं लेने दिया जाता वे घर ही नही जायेंगी।
गांव की सभी महिलाएं बच्चों के साथ जाकर सरपंच के घर के सामने बैठ गईं। पंचों ने और गांव के लोगों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया किन्तु वे न मानीं। वे सब बोलीं कि जब उनके पास कुछ खाने-पीने के लिए ही नहीं है तो वे घर जाकर क्या करेंगीं। जब तक उनको नहर से या दूसरे कुंएं से पानी नहीं लेने दिया जायेगा, वे घर नहीं जायेंगी।
यह समाचार धीरे-धीरे सारे गांव में फैल गया और अन्य घरों की महिलाएं और बच्चे भी वहां आने लगे। भीड़ बढ़ती देख सरपंच ने पुलिस बुलाने का निर्णय लिया। किन्तु इससे पहले कि वे पुलिस बुलाते, सरपंच की पत्नी और बच्चे उनके सामने आ खड़े हुए। पत्नी ने कहा कि आप सोचिए कि अगर हमें एक दिन भी पानी न मिले तो हम क्या करेंगे। और ये लोग तो हर रोज़ कितनी दूर से पानी लाते हैं। मैंने इन महिलाओं और बच्चों को दिन में इतनी धूप और कड़ी गर्मी में दो-दो, तीन-तीन चक्कर लगाते देखा है। कैसे कर लेती हैं ये इतनी मेहनत। फिर घर जाकर घर के सारे काम करती हैं। आप कुछ तो इन पर दया कीजिए और अपना कुंआ इनके लिए खोल दीजिए।
सरपंच की मानों आंखें खुल गईं , इस तरह तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने तत्काल अपने कुंए से सारे गांव को पानी भरने की अनुमति दे दी और साथ ही पंचों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने गांव की पानी की समस्या को सदा के लिए हल करने के लिए नीतियां बनायेंगें।
नये साल में
नये साल में कुछ नई बात करें
पिछला भूल, नये पथ पर बढ़ें
जीवन खुशियों का सागर है
मोती चुन लें, कंकड़ छोड़ चलें
ज़िन्दगी की लम्बी राहों में
साथ कोई
उम्र-भर देता नहीं है
जानते हैं हम, फिर भी
मन को मनाते नहीं हैं।
मुड़-मुड़कर देखते रहते हैं
जाने वालों को हम
भुला पाते नहीं हैं।
ज़िन्दगी की लम्बी राहों में
न जाने कितने छूट गये
कितने हमें भूल गये
याद अब कर पाते नहीं हैं।
फिर भी इक टीस-सी अक्सर
दिल में उभरती रहती है
जिसे हम नकार पाते नहीं हैं।
जीवन के राज़
जिन्हें हम जीवन में
राज़ बनाये रखना चाहते हैं
वे ही सबसे ज़्यादा
चर्चित विषय रहते हैं।
मेरा सुख-दुख
मेरी पसन्द-नापसन्द
मेरी चिन्ताएॅं, मेरी अर्हताएॅं,
मेरी विवशताएॅं,
कहाॅं रह पाती हैं मेरी।
न जाने कैसे
मेरे अन्तर्मन से निकलकर
सारे जहाॅं में
चर्चा का विषय बन जाते हैं।
डरती नहीं
पर विश्वस्त भी नहीं रह पाती,
इस कारण
अपनी बात
अपने-आप से ही
नहीं कर पाती।
आसमान में छेद
पता नहीं कौन शायर कह गया
आसमां में छेद क्यों नहीं हो सकता
एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता यारो ।
पता नहीं किस युग का था वह शायर।
उछालकर देखा था क्या उसने कभी पत्थर।
बड़ा काम तो हम ज़िन्दगी में
कभी कर नहीं पाये
सोचा, चलो आज कुछ नया करते हैं
उस शायर की इच्छा पूरी करते हैं।
एक क्यों,
तबीयत से कई पत्थर उछालते हैं,
आसमान में एक नहीं
अनेक छेद करते हैं।
पर शायद
युग बदल गया था
या हमें
पत्थर उछालने का
तरीका पता नहीं था
हमने तो अभी बस
एक ही पत्थर उठाया था
उछालने की नौबत भी नहीं आई थी
सैंकड़ों पत्थर लौट आये हमारे पास।
लगता है
उस शायर का शेर
सबने पसन्द कर लिया है
और हमारी तरह
सभी पत्थर उछालने में लगे हैं
और हम तो
अपना ही सिर फोड़ने में लगे हैं।
चेहरे बदल लें
चलो आज चेहरे बदल लें।
बहुत दिन बीत गये।
लोग अब
हमारी
असलियत
पहचानने लगे हैं
हमें
बहुत अच्छे से
जानने लगे हैं।
खरपतवार
वही फ़सल काटते हैं
जो हम बोते हैं,
ऐसा नहीं होता यारो।
जीवन में
खरपतवार का भी
कोई महत्व है
या नहीं।
अपनी-अपनी कयामत
किसी दिन।
आसमान टूट पड़े
धरती हिल जाये
सागर उफ़न पड़े
दुनिया डूबने लगे
शायद
इसे ही कहते हैं न कयामत।
नहीं रे !!
सबकी ज़िन्दगी की
अपनी-अपनी कयामत भी होती है।
न आसमान गिरता है
न धरा फ़टती है
न सागर सूखता है
फिर भी
आ जाती है कयामत।
कोई एक बात,
कोई एक शब्द, एक चुटकी,
एक कसक,
कोई नाराज़गी,
कुछ दूरियाॅं
कोई मन-मुटाव,
आॅंख-भर का इशारा
और हो जाती है कयामत।
नहले पे दहला
तू
नहले पे दहला
लगाना सीख ले
नहीं तो
गुलाम
बनकर
रह जायेगा
ज़िन्दगी जीने के तरीके
ज़िन्दगी जीने के
तरीके
यूॅं तो मुझे
ज़िन्दगी जीने के
तरीके बहुत आते हैं
किन्तु क्या करुॅं मैं
उदाहरण और उलाहने
बहुत सताते हैं।
दिल या दिमाग
मित्र कहते हैं,
बात पसन्द न आये
तो एक कान से सुनो,
दूसरे से निकाल दो।
किन्तु मैं क्या करूॅं।
मेरे दोनों कानों के बीच
रास्ता नहीं है।
या तो
दिल को जाकर लगती है
या दिमाग भन्नाती है।
झूठ-सच Lia
झूठ-सच के अर्थ बदल गये
फूलों से ज़्यादा कांटे बसर गये
जीवन पथ
जीवन पथ की क्या बात करें
कुछ कंकड़, कुछ पत्थर,
कुछ फूल बिछे, कुछ कांटे उलझे।
पग-पग पर थी बाधाएॅं
पग-पग पर द्वार उन्मुक्त मिले।
वादों की, बातों की धूम रही,
कुछ निभ गये, कुछ छूट गये।
अपनों की अपनों से बात हुई
कभी मन मिला, कभी बिखर गये।
जीवन तो चलता ही रहता है
कभी रुकते-रुकते, कभी भाग लिये।
कब कौन मिला, कितने छूट गये
याद नहीं अब, कितना तो भूल गये।
कितने कागज़ रंगीन हुए
कितनों पर स्याही बिखर गई,
कभी कुछ भी न लिख पाने की पीर हुई।
उलझी, बिखरी, खट्टी-मीठी
जैसी भी हैं
सब अपनी हैं,
टुकड़ों-टुकड़ों में बिखर गईं।
कहते हैं
हाथों की रेखाओं में
भाग्य लिखा रहता है
मुट्ठियां खोलीं
तो उलझी-उलझी सी महसूस हुईं।
कितने दिन बाकी हैं,
कितने बीत गये
सोच-सोचकर नहीं सोचती,
पर मन पर हावी हो गये।
निडर होकर उड़े हैं
बादलों के रंगों से मन में उमंग लेकर चले हैं
चंदा को पकड़कर उड़ान भरकर हम चले हैं
तम-प्रकाश में उंचाईयों से नहीं डरते हम
झिलमिलाती रोशनियों में निडर होकर उड़े हैं
भ्रष्टाचारी सांसद विधायक के चुने जाने पर पार्टी जिम्मेदार हैं या आम आदमी
चुनाव में जो भी लोग खड़े होते हैं, उनका चयन पार्टी ही करती है न कि आम आदमी। सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति को पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनती है, उसके बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं दी जाती, और आम आदमी भी केवल पार्टी का नाम देखकर ही वोट दे देता है न कि व्यक्ति-विशेष की जानकारी लेना चाहता है कि वह कैसा है। किन्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी तो अपने प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में जानती ही है। पार्टी एवं आम आदमी के अतिरिक्त चुनाव आयोग की भी भूमिका रहती है, जहाॅं दूध का दूध एवं पानी का पानी सम्भव है किन्तु होता नहीं।
वास्तव में पार्टियों के अपने स्वार्थ रहते हैं और आम आदमी दिशाहीन एवं असंलिप्त। अतः पार्टी का दायित्व प्रथम है। और आम आदमी का दोष यह कि वह अपने ही अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है कि जब उसके पास वोट मांगने के लिए प्रत्याशी आता है तो वे उससे उसकी आधिकारिक पूरा जानकारी लें। आम आदमी ऐसी किसी भी समस्या से बचकर निकलना चाहता है। उसे किसी झंझट में नहीं पड़ना। किन्तु सर्वाधिक दायित्व चुनाव आयोग का है जिसके पास प्रत्येक प्रत्याशी का पूरा विवरण जाता है और वहां से उसे चुनाव में खड़े होने के अधिकार मिलते हैं। वास्तविकता यह कि 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में जहाॅं आज भी धनबल पर वोट लिये जाते हैं, मतदान केन्द्र लूटे जाते हैं, अशिक्षा चरम पर है, वहाॅं आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। अतः मेरी समझ में दायित्व पार्टियों का एवं चुनाव आयोग का है कि भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को टिकट ही न मिले।
क्या समाज ने अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार कर लिया है
हमारा समाज बहुत विखण्डित है। हमारे समाज में लाखों-लाखों जातियाॅं हैं। लोगों की सोच में परिवर्तन शिक्षा, आर्थिक स्थिति, निवास-स्थान एवं कार्य-क्षेत्र पर बहुत निर्भर करता है। आज भी हम लोग जाति की सोच से बाहर नहीं निकल पाये। आज भी जब कोई हम लोगों से नाम पूछता है तो हम बिना जाति के नाम नहीं बताते। और यदि केवल नाम बताएॅं तो सामने वाले की आॅंखों में एक प्रश्नचिन्ह होता है कि अगले ने पता नहीं क्यों ‘‘जात’’ नहीं बताई। 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे आस-पास, परिचितों, सम्बन्धियों में अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं, और उन्हें मान्यता मिल जाती है अथवा विवशता में दे दी जाती है। किन्तु क्या यह स्थिति पूरे देश में है ? सभी जातियों, प्रान्तों, गांवों में है ? शायद , नहीं।
वास्तविकता यह है कि हम आज भी उन्हीं रूढ़ियों में जी रहे हैं। किन्तु अन्तर्जातीय विवाह का विरोध करने के और भी अनेक कारण हैं।
हमारे देश में जाति, स्थान, वर्ग, प्रदेश, गांव, आदि के अलग-अलक रीति-रिवाज़, परम्पराएॅं, लेन-देन, खान-पान, भाषा-भिन्नताएॅं हैं जिस कारण परिवारों में सामंजस्य बहुत कठिन होता है। इस कारण आज भी लोग अन्तर्जातीय विवाह करने में संकोच करते हैं।
अतः मेरे विचार में हमारे समाज ने अन्तर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया है।
श्मशान घाट
कौन कहता है कि श्मशान घाट से कोई लौटकर नहीं आता। जाता तो केवल एक है, शेष सब तो लौट ही आते हैं, डरे, सहमे, घबराये, अतीत की अमिट परछाईयों के साथ, जीवन के प्रति एक ऐसे नये चिन्तन एवं दृष्टिकोण के साथ जिसे हम न तो कभी सोच पाये थे और न ही समझ पाये थे। अपने-परायों, सम्बन्धों की उधेड़-बुन के साथ। जो गया, क्यों चला गया, कौन था, कितना अपना था, क्यों चला गया। सबसे कठिन होता है, जब हम जाने वाले के लिए तैयारी करने लगते हैं, सामान, सामग्री जुटाते हैं, समय निर्धारित करते हैं। सबको सूचित करने लगते हैं। आहत करती हैं ये स्थितियाँ, तोड़ती हैं, पूछती हैं, क्या कर लोगे तुम, कैसे करोगे। एक लम्बी कहानी रह जाती है, सम्बन्धों की, स्मृतियों की, अनुभवों की, और सबसे विशेष उन कथाओं की जो हमारे आस-पास बुनी जाने लगती हैं। जीवन के न जाने कितने नये पृष्ठ खुल जाते हैं। एक जीवन समाप्त होता है तो एक नया शुरु भी होता है। कुछ साथ देती हैं और कुछ उपेक्षा, कुछ मरहम लगाती हैं और कुछ कुरेदती हैं। यही जीवन के आने-जाने की वास्तविकता है।
एक पाती भाव भरी
अब हम सत्तर वर्ष के हो गये, एक क्या हज़ारों भाव भरी पाती स्मृति में उभर कर आ गईं। किस-किसकी बात करें आपसे। कभी तीन पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, पांच पैसे का अन्तर्देशीय और बन्द लिफ़ाफ़े पर दस पैसे का टिकट लगता था। जब घर में बन्द लिफ़ाफ़ा आता था तो पूरा घर चैकन्ना हो जाता था कि किसी का अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र आया है जो बन्द लिफ़ाफ़े में आया है।
मेरी पहली भावभरी पाती वह थी जो किसी पत्रिका में मेरी पहली कविता प्रकाशित होने पर एक पाठक ने प्रशंसा पत्र भेजा था। पोस्टकार्ड था । उस समय तक पोस्ट कार्ड का मूल्य बढ़ चुका थाः दस पैसे। मेरे जीवन का वह पहली भाव भरी पाती थी जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। दिनों-दिनों तक मैं उस पोस्ट कार्ड को छुपा-छुपाकर पढ़ती रहती थी। उसके बाद ऐसी कितनी ही भाव-भरी पाती आईं और मैं आह्लादित होती थी ऐसी पाती से। ऐसे पत्र पाठक के मन से लिखे होते थे, और उनका मैं उत्तर भी अवश्य देती थी। आज की तरह नहीं कि गूगल ने कुछ बने-बनाये शब्द दे दिये और हम उन्हें ही काॅपी-पेस्ट किये जा रहे हैं।
मेरे प्रिय हिन्दी साहित्यकार : हज़ारी प्रसाद द्विवेदी
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य से मैं बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हूं। अपने अध्ययन काल में अनेक कवि, लेखक, उपन्यासकार, इतिहासकार रहे जिनकी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया किन्तु हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन मुझे बहुत गहरे तक जोड़ता रहा है।
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी (19 अगस्त 1907 - 19 मई 1979) हिन्दी निबन्धकार, आलोचक, उपन्यासकार थे। कलाओं के प्रति इनके दृष्टिकोण ने प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के अध्ययन के नवीन द्वार उन्मुक्त किये। साहित्य की प्रत्येक विधा में वे पारंगत थे। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और बाङ्ला भाषाओं के विद्वान थे।
द्विवेदीजी ने शांति निकेतन में बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष, उपरान्त पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष, पुनः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। उनकी
विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्ति हुई। कुछ समय के लिए हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालान्तर में उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबन्ध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।1957 में पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किये गये। 1997 में इनके चित्र का डाक टिकट भी जारी हुआ।
हिन्दी साहित्य पर इनका लेखन पठनीय एवं अप्रतिम है। मुझे इनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा बहुत आकर्षित एवं प्रभावित करती रही है। हिन्दी साहित्य को इन्होंने एक नई पहचान दी। रामचन्द्र शुक्ल के बाद इनकी हिन्दी साहित्य एवं इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों ने हिन्दी साहित्य के पाठकों को एक नवीन, चिन्तनपूर्ण दृष्टि प्रदान की। मध्यकालीन हिन्दी साहित्य एवं प्राचीन एवं अर्चाचीन साहित्य पर इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें एक नवीन चिन्तन प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास गहन चिन्तन की ओर ले जाते हैं। विषय विविधता इनके लेखन की विशेषता रही है। अगस्त 1981 में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध सम्पूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली के नाम से प्रकाशित हुआ।
नई पीढ़ी और हिन्दी
नई पीढ़ी की हिन्दी आजकल स्टैंडअप कामेडियन बनकर रह गई है।
बात कटु किन्तु है सत्य कि नई पीढ़ी के पास हिन्दी नहीं है। वे केवल बोल-चाल में हीए उतनी ही हिन्दी जानते हैं जितनी आवश्यक है। और आज की पीढ़ी की हिन्दी, हिन्दी न होकर एक अद्भुत- मिश्रितए खिचड़ी भाषा है, अपशब्दों की भरमार रहती है।
इसके लिए हम नई पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते। उनको जो मिल रहा है वही वे परोस रहे हैं और खा-खिला रहे हैं।
इसके अनेक कारण हैं।
आज सारे देश में समान भाषा पद्धति नहीं है, है तो केवल अंग्रेज़ी के लिए। हिन्दी देश के कुछ ही राज्यों में अनिवार्य है वह भी केवल दसवीं तक। अनेक राज्यों में यहां भी अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए विकल्प दे दिया जाता है। प्रत्येक विषय का माध्यम अंग्रेज़ी ही रहता है। इसके अतिरिक्त CBSE, ICSE के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के अपने शिक्षा बोर्ड हैं जो अपने राज्य के अनुसार भाषा का चयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि दसवीं के बाद हिन्दी का विकल्प ही नहीं है। यदि आप विभिन्न शिक्षा बोर्ड के विषयों को देखें तब वहां आपको हिन्दी का विकल्प दिखाई तो देगा किन्तु अधिकांश विद्यालय इसके लिए अध्यापक ही नियुक्त नहीं करते और हिन्दी का विकल्प ही नहीं देते।
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, IT आदि सब अंग्रेज़ी आधारित ही हैं। यदि दसवीं तक अच्छी हिन्दी पढ़ाई भी जाये तो भी यहां तक आते-आते सब छूट जाती है।
कहने को हिन्दी समाचार-पत्र एवं टी वी समाचार पत्र हिन्दी में प्रसारित होते हैं किन्तु कैसी हिन्दी होती है यह तो हम जानते ही हैं। सरलता के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग एवं निरर्थक अंग्रेज़ी शब्दों का ही प्रयोग होता है ।
एक अन्य कारण यह कि हम आज वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अनेक देश आज भी अपनी भाषा से वैश्विक स्तर से जुड़े हुए हैं तो हम क्यों नहीं। इसका सीधा-सा कारण यह है कि जब हम 70 वर्षों में हिन्दी को उस स्तर पर स्थापित नहीं कर पाये तो अब यह असम्भव प्रायः ही प्रतीत होता है।
हमें स्वीकार करना ही होगा कि नई पीढ़ी हिन्दी के साथ नहीं है। केवल चलती हिन्दी बोल लेना अथवा लिख लेना हिन्दी नहीं है। व्याकरण कहीं खो गया है। शब्द अनर्थ होने लगे हैं, वर्णमाला ध्वस्त है। वाक्य संरचना का कोई अर्थ नहीं रह गया है।
ये आँखें
ये आँखें भी बहुत बड़ी चीज़ हैं। ये तो सब ही जानते हैं कि देखने के काम आती हैं किन्तु दिखाने के भी बहुत काम आती हैं, बस आपको दिखानी आनी चाहिए। आज सब सोचने लगी, आँखों के मुहावरों पर तो न जाने कितने मुहावरे सामने आ गये।
आँखों ही आँखों में हँसना, आँख मारना, आँखों में धूल झोंकना, आँखें बिछाना, आँख का कांटा, आँख का तारा, आँख लगना, आँख लड़ना, आँखें चुराना और न जाने कितने ही।
किन्तु कुछ मुहावरे तो बिल्कुल मेरे काम के निकले। जैसे
आँख धुंधलाना, आँख दिखाना, आँखों पर चरबी चढ़ना, आँख पर पर्दा पड़ना, आँखें बन्द होना, सीधी आँख न देखना और अन्त में आँख खुलना।
नववर्ष का उपहार लेकर आईं हमारी आँखें हमारे लिए। आँख धुंधलाने लगी। आँख देखने वाले को आँख दिखाई। किन्तु वे कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने हमें ही आँख दिखा दी। बोले, आँखों पर चरबी चढ़ गई है, आँखों पर पर्दा पड़ गया है।
और नववर्ष में उन्होंने हमारी एक आँख बन्द कर दी। अब न सीधी आँख देखना, न आँख मारना, न आँख लड़ना न लड़ाना। वाह! आँख के भीतर एक लैंस, एक चश्मा भी उपहार में मिला। मोबाईल, टी. वी., पी. सी. सब बन्द। और अन्त में जब ठीक से आँख खुली तब भी ठीक से अनुभव करने में दो-तीन दिन तो लग ही गये।
इसे कहते हैं cataract
अब एक आँख तो सुधर गई, दूसरी भी पीछे नहीं। तो चलिए उसके लिए भी ये सारे मुहावरे याद रखते हैं, अगले सप्ताह के लिए।