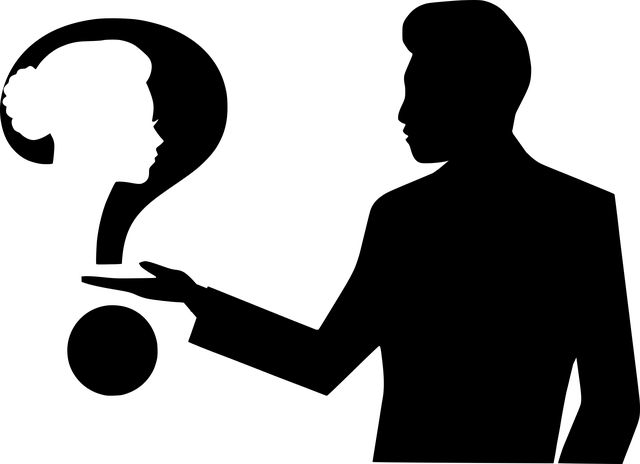इच्छाओं का कोई अन्त नहीं
हमारी इच्छाओं का
कोई अन्त नहीं।
बालपन में
चिन्ताओं से दूर
मस्ती में जीते थे
किन्तु बड़ों को देखकर
आहें भरते थे।
कब बड़े होंगे हम।
बड़ों के स्वांग भर
खूब आनन्द लेते थे हम।
बड़े हुए
तो बालपन में
मन भटकने लगा
अक्सर कहते फ़िरते
आह! काश!
हम फिर बच्चे बन जायें।
और वृ़द्धावस्था क्या आई
सब कहने लगे
वृद्ध और बाल
तो समान ही होते हैं।
ऐसा नहीं होता रे
कोई मेरे मन से पूछे
इच्छाएँ कभी नहीं मरतीं
बालपन हो
युवावस्था अथवा वृद्धावस्था
चक्रव्यूह की भांति
जीवन भर उलझाये रखती हैं
जो मिला है,
वह भाता नहीं
जो नहीं मिला
वह जीवन-भर आता नहीं।
मन करता करूँ बात चाँद तारों से
मन करता करूँ बात चाँद तारों से।
न जाने कितने भाव
कितनी बातें
अनकही, सुलझी-अनसुलझी
भीतर-ही-भीतर
कचोटती हैं
बिलखती हैं
बहुत कुछ बोलती हैं।
किसी से कहते हुए
मन डरता है
कहीं कोई पूछ न ले
कोई बात की बात न हो जाये
कहीं पुराने ज़ख्म न खुल जायें
कहीं कोई अपनापन दिखाए
और हम शत्रुता का भाव पायें
न जाने किस बात का
कौन-सा अर्थ निकल आये
खुले गगन के नीचे
चाँद -तारों से बतियाती हूँ
मन की हर बात बताती हूँ ।
और गहरी नींद सो जाती हूँ ।
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचनाकार
यह विधाता,
जगत-नियन्ता
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचनाकार।
इसकी कुछ बातें मुझे
समझ ही नहीं आतीं।
इतने बड़े ब्रह्माण्ड का निर्माण किया
करोड़ों जीव-जन्तु बनाये
कितना श्रम किया होगा
कितना तो समय लगा होगा
शायद अरबों-खरबों वर्ष।
फिर उनकी देख-भाल
नवीनीकरण, और पता नहीं क्या-क्या।
किन्तु इतनी बड़़ी भूल
कैसे हो सकती है।
विज्ञान कहता है
जब बच्चा जन्म लेता है
तो उसके शरीर में
300 हड्डियाँ होती हैं
जो कालान्तर में 206 में
बदल जाती हैं।
और 300 हड्डियों को
लगाते-लगाते
जिह्वा में हड्डी लगाना ही भूल गये।
.
शायद, इसीलिए
अकेली जिह्वा ही
ज़रा-सा हिलकर
206 हड्डियों वाले
किसी भी ढांचे की
चूर-चूर, चकनाचूर
करने की क्षमता रखती है।
भ्रम-जाल
पता नहीं किस
भ्रम में रहते हैं हम
कि बदल रहा है
बहुत कुछ,
या आने वाला कल
बदलकर आयेगा
और अब
बहुत कुछ
अच्छा ही अच्छा लायेगा।
लेकिन कुछ नहीं बदलता।
बस तरीके बदलते हैं
ढर्रे बदलते हैं
रास्ते अलग-से लगते हैं
लेकिन
आज का दौर
हो या कल का
सब एक-सा ही होता है,
शेष तो भ्रम-जाल होता है।
नया-पुराना
कुछ अलग-सा ही होता है
दिसम्बर।
पहले तो
बहुत प्रतीक्षा करवाता है
और आते ही
चलने की बात
करने लगता है।
कहता है
पुराना जायेगा तभी तो
कुछ नया आयेगा।
और जब नया आयेगा
तो कुछ पुराना जायेगा।
लेकिन
नये और पुराने के
बीच की दूरियॉं
पाटने में ही
ज़िन्दगी निकल जाती है
और हम नासमझ
बस हिसाब लगाते रह जाते हैं।
चलिए, आज
नये-पुराने को छोड़
बस आज की ही बात करते हैं
और आनन्द मनाते हैं।
नया- पुराना
कुछ अलग-सा ही होता है
दिसम्बर।
पहले तो
बहुत प्रतीक्षा करवाता है
और आते ही
चलने की बात
करने लगता है।
कहता है
पुराना जायेगा तभी तो
कुछ नया आयेगा।
और जब नया आयेगा
तो कुछ पुराना जायेगा।
लेकिन
नये और पुराने के
बीच की दूरियां
पाटने में ही
ज़िन्दगी निकल जाती है
और हम नासमझ
बस हिसाब लगाते रह जाते हैं।
स्वर्ण मृग नहीं होते
काश! स्वर्ण मृग नहीं होते।
न होती सीता की कथाएॅं
न होती रावण की चर्चा।
काश! स्वर्ण मृग नहीं होते।
तुम शायद कहोगे
आज तो नहीं हैं स्वर्ण मृग।
हैं न,
मृग मरीचिकाएॅं तो हैं,
मृग तृष्णाएॅं तो हैं।
न कोई राम है, न रावण।
स्वयॅं ही वन-कानन हैं,
स्वयं ही राम-रावण
और लक्ष्मण रेखा से जूझती
सीता भी स्वयं ही हैं।
वनवास
केवल तब नहीं होता
जब वन में रहते हैं।
मन में भी वन होते हैं सघन,
अग्नि परीक्षा
केवल अग्नि में
समा जाने से नहीं होती,
अपने भीतर भी होती रहती है।
अपनी ही परीक्षाएॅं लेते हैं
अपनी ही खींची हुई लक्ष्मण रेखा
लांघते हैं
और अपने भीतर ही
अपहृत हो जाते हैं।
इस व्यथा को
मैं स्वयं नहीं समझ सकी
तो आपको क्या समझाउॅं।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कुछ समस्याओं पर
बात करने से कतराते हैं हम
समझ नहीं पाते
कहाॅं से शुरु करें
और कहाॅं खतम।
जिन्हें बात करनी चाहिए
वे पूल में ठण्डक ले रहे हैं
सुबह-शाम
तरह-तरह के पेय से
गला तर कर रहे हैं।
वादों की, बातों की
उड़ाने भर रहे हैं।
सुरक्षा कवच इतना बड़ा है
कि इन बाल्टियों की खनक
उनके कानों तक पहुंचती नहीं।
बूॅंद-बूॅंद पानी की कमी
उन्हें खलती नहीं।
उनकी योजनाओं में
बड़े-बड़े बांध हैं,
पर्यटन के लिए
लबालब झीलें हैं।
वे नहीं जानते
प्यास क्या होती है
पानी कैसे भरा जाता है
बाल्टियाॅं, पतीले, बर्तन
क्या होते हैं।
भीड़ का अर्थ नहीं जानते वे।
घूॅंट-घूॅंट पानी की कीमत
नहीं समझते वे।
वैसे भी
हर साल आती हैं ये समस्याएॅं
कभी आगे, कभी पीछे
चलती हैं ये समस्याएॅं
मौसम बदलता है
लोग भूल जाते हैं।
फिर कोई नई समस्या आती है
और लोग
फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं।
सिलसिला चला रहता है
कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कौन जीता है
कौन मरता है।
कहीं सच न बोल बैठे
रहने दो मत छेड़ो दर्द को
कहीं सच न बोल बैठे।
राहों में फूल थे
न जाने कांटे कैसे चुभे।
चांद-सितारों से सजा था आंगन
न जाने कैसे शूल बन बैठे।
हरी-भरी थी सारी दुनिया
न जाने कैसे सूखे पल्लव बन बैठे।
सदानीरा थी नदियां
न जाने कैसे हृदय के भाव रीत गये।
रिश्तों की भीड़ थी मेरे आस-पास
न जाने कैसे सब मुझसे दूर हो गये।
स्मृतियों का अथाह सागर उमड़ता था
न जाने कैसे सब पन्ने सूख गये।
सूरज-चंदा की रोशनी से
आंखें चुंधिया जाती थीं
न जाने कैसे सब अंधेरे में खो गये।
बंद आंखों में हज़ारों सपने सजाये बैठी थी
न जाने कैसे आंख खुली, सब ओझल हो गये।
नहीं चाहा था कभी बहुत कुछ
पर जो चाहा वह भी सपने बनकर रह गये।
दर्द सच न बोल बैठे
रहने दो मत छेड़ो दर्द को
कहीं सच न बोल बैठे।
राहों में फूल थे
न जाने कांटे कैसे चुभे।
चांद-सितारों से सजा था आंगन
न जाने कैसे शूल बन बैठे।
हरी-भरी थी सारी दुनिया
न जाने कैसे सूखे पल्लव बन बैठे।
सदानीरा थी नदियां
न जाने कैसे हृदय के भाव रीत गये।
रिश्तों की भीड़ थी मेरे आस-पास
न जाने कैसे सब मुझसे दूर हो गये।
स्मृतियों का अथाह सागर उमड़ता था
न जाने कैसे सब पन्ने सूख गये।
सूरज-चंदा की रोशनी से
आंखें चुंधिया जाती थीं
न जाने कैसे सब अंधेरे में खो गये।
बंद आंखों में हज़ारों सपने सजाये बैठी थी
न जाने कैसे आंख खुली, सब ओझल हो गये।
नहीं चाहा था कभी बहुत कुछ
पर जो चाहा वह भी आप लेकर चले गये।
ये कैसा सावन ये कैसा पानी
सावन की बरसे बदरिया
सोच-सोच मन घबराये।
बूंदें कब
जल-प्लावन बन जायेंगी
कब बहेगी धारा
सोच-सोच मन डर जाये।
-
नदिया का पानी
तट-बन्धों से जब टकराए
कब टूटेंगी सीमाएं
रात-रात नींद न आये।
-
बिजली चमके
देख रहे, लाखों घर डूबे
कितनी गई जानें
मन सहम-सहम जाये।
-
कब आसमान से आयेगी विपदा
कौन रहेगा, कौन जायेगा
हाथों से हाथ छूट रहे
न जाने ये कैसे दिन आये।
.
पुल टूटू, राहें बिखर गईं
खेतों में सागर लहराया
सूनी आंखों से ताक रहा किसान
देख-देख मन भर आये।
.
न सिर पर छत रही
न पैरों के नीचे धरा रही
कहां जा रहे, कहां आ रहे
कंधों पर लादे ज़िन्दगी
न जाने हम किस राह निकल आये।
-
कैसी विपदा ये आई
हाथ बांध हम खड़े रह गये
लूट ले गया घर-घर को
जल का तांडव,
कब निकलेगा पानी
कब लौटेंगे जीवन में
नहीं, नहीं, नहीं, हम समझ पाये।
सृजनकर्ता का आभार
उस सृजनकर्ता का
आभार व्यक्त नहीं कर पाती मैं
जिसने इतने सुन्दर,
मोहक संसार की रचना की।
उस आनन्द को
व्यक्त नहीं कर सकती मैं
जो इस सृष्टिकर्ता ने
हमें दिया।
उससे ही मिले
आकाश को विस्तार देकर
गर्वोन्नत होने लगते हैं हम।
उससे मिली अमूल्य धरोहर को
अपना कहकर
अधिकार जमाने लगते हैं हम।
भूल जाते हैं उसे।
-
किन्तु नहीं जानते
कब जीवन में सब
उलट-पुलट हो जायेगा,
खाली हो जायेंगे हाथ।
और ये खाली हाथ
जुड़ जायेंगे
उसकी सत्ता स्वीकार करते हुए।
पानी के बुलबुलों सी ज़िन्दगी
जल के चिन्ह
कभी ठहरते नहीं
पलभर में
अपना रूप बदलकर
भाग जाते हैं
बिखर जाते हैं
तो कभी कुछ
नया बना जाते हैं।
छलक-छलक कर
बहुत कुछ कह जाते हैं
हाथों से छूने पर
बुलबुलों से
भाग जाते हैं।
लेकिन कभी-कभी
जल की बूंदें भी
बहुत गहरे
निशान बना जाती हैं
जीवन में,
बस हम अर्थ
ढूंढते रह जाते हैं।
और ज़िन्दगी
जब
कदम-ताल करती है,
तब हमारी समझ भी
पानी के बुलबुलों-सी
बिखर-बिखर जाती है।
मेरी प्रार्थनाएं
मैं नहीं जानती
प्रार्थनाएं कैसे करते हैं
क्यों करते हैं,
और किसके सामने करते हैं।
मैं तो यह भी नहीं जानती
कि प्रार्थनाएं करने से
क्या मिल पाता है
और क्या मांगना चाहिए।
सूरज को देखती हूं।
चांद को निरखती हूं।
बाहर निकलती हूं
तो प्रकृति से मिलती हूं।
पत्तों-फूलों को छूकर
कुछ एहसास
जोड़ती हूं।
गगन को आंखों में
बसाती हूं
धरा से नेह पाती हूं।
लौटकर बच्चों के माथे पर
स्नेह-भाव अंकित करती हूं,
वे मुझे गले से लगा लेते हैं
इस तरह मैं
ज़िन्दगी से जुड़ जाती हूं।
मेरी प्रार्थनाएं
पूरी हो जाती हैं।
आज मौसम मिला
आज मौसम मिला।
मैंने पूछा
आजकल
ये क्या रंग दिखा रहे हो।
कौन से कैलेण्डर पर
अपना रूप बना रहे हो।
अप्रैल में अक्तूबर,
और मई में
अगस्त के दर्शन
करवा रहे हो।
मौसम
मासूमियत से बोला
आजकल
इंसानों की बस्ती में
ज़्यादा रहने लगा था।
माह और तारीखों पर
ध्यान नहीं लगा था।
उनके मन को पढ़ता था
और वैसे ही मौसम रचने लगा था।
अपने और परायों में
भेद समझने में लगा था।
कौन किसका कब हुआ
यह परखने में लगा था।
कब कैसे पल्टी मारी जाती है,
किसे क्यों
साथ लेकर चलना है
और किसे पटखनी मारी जानी है
बस यही समझने में लगा था।
गर्मी, सर्दी, बरसात
तो आते-जाते रहते हैं
मैं तो तुम्हारे भीतर के
पल-पल बदलते मौसम को
समझने में लगा था।
.
इतनी जल्दी घबरा गये।
तुमसे ही तो सीख रहा हूँ।
पल में तोला,पल में माशा
इधर पंसेरी उधर तमाशा।
अभी तो शुरुआत है प्यारे
आगे-आगे देखिए होता है क्या!!!
और जब टूटती है तन्द्रा
चलती हुई घड़ी
जब अचानक ठहर-जी जाती है,
लगता है
जीवन ही ठहर गया।
सूईयाँ अटकी-सी,
सहमी-सी,
कण-कण
खिसकने का प्रयास करती हैं,
अनमनी-सी,
किन्तु फिर वहीं आकर रुक जाती हैं।
हमारी लापरवाही, आलस्य
और काल के महत्व की उपेक्षा,
कभी-कभी भारी पड़ने लगती है
जब हम भूल जाते हैं
कि घड़ी ठहरी हुई,
चुपचाप, उपेक्षित,
हमें निरन्तर देख रही है।
और हम उनींदे-से,
उसकी चुप्पी से प्रभावित
उसके ठहरे समय को ही
सच मान लेते हैं।
और जब टूटती है तन्द्रा
तब तक न जाने कितना कुछ
छूट जाता है
बहुत कुछ बोलती है घड़ी
बस हम सुनना ही नहीं चाहते
इतना बोलने लगे हैं
कि किसी की क्या
अपनी ही आवाज़ से
उकता गये हैं ।
हे सागर, रास्ता दो मुझे
हे सागर, रास्ता दो मुझे
कहा था सतयुग में राम ने।
सागर की राह से
एक युद्ध की भूमिका थी।
कारण कोई भी रहा हो
युद्ध सुनिश्चित था।
किन्तु फिर भी
सागर का
एक प्रयास
शायद
युद्ध को रोकने का,
और इसी कारण
मना कर दिया था
राम को राह देने के लिए,
राम की शक्ति को
जानते हुए भी।
शायद वह भी चाहता था
कि युद्ध न हो।
युद्ध राम-रावण का हो
अथवा कौरवों-पाण्डवों का
विनाश तो होता ही है
जिसे युगों-युगों तक
भोगती हैं
अगली पीढ़ियां।
युद्ध कोई भी हो,
अपनों से
या परायों से
एक बार तो
रोकने की कोशिश
करनी ही चाहिए।
सपने
अजीब सी होती हैं
ये रातें भी।
कभी जागते बीतती हैं
तो कभी सोते।
कभी सपने आते हैं
तो कभी
सपने डराकर
जगा जाते हैं।
कहते हैं
सिरहाने पानी ढककर
रख दें
तो बुरे सपने नहीं आते।
पर सपनों को
पानी नहीं दिखता।
उन्हें
आना है
तो आ ही जाते हैं।
कभी सोते-सोते
जगा जाते हैं
कभी पूरी-पूरी रात जगाकर
प्रात होते ही
सुला जाते हैं।
एक और अलग-सी बात
दिन हो या रात
अंधेरे में आंखें
बन्द हो ही जाती हैं।
और मुश्किल यह
कि जो देखना होता है
फिर भी देख ही लिया जाता है
क्योंकि
देखते तो हम
मन की आंखों से हैं
अंधेरे और रोशनी
दिन और रात को इससे क्या।
प्रतिबन्धित स्मृतियाँ
जब-जब
प्रतिबन्धित स्मृतियों ने
द्वार उन्मुक्त किये हैं
मन हुलस-हुलस जाता है।
कुछ नया, कुछ पुराना
अदल-बदलकर
सामने आ जाता है।
जाने-अनजाने प्रश्न
सर उठाने लगते हैं
शान्त जीवन में
एक उबाल आ जाता है।
जान पाती हूँ
समझ जाती हूँ
सच्चाईयों से
मुँह मोड़कर
ज़िन्दगी नहीं निकलती।
अच्छा-बुरा
खरा-खोटा,
सुन्दर-असुन्दर
सब मेरा ही है
कुछ भोग चुकी
कुछ भोगना है
मुँह चुराने से
पीछा छुड़ाने से
ज़िन्दगी नहीं चलती
कभी-न-कभी
सच सामने आ ही जाता है
इसलिए
प्रतीक्षा करती हूँ
प्रतिबन्धित स्मृतियों का
कब द्वार उन्मुक्त करेंगी
और आ मिलेंगी मुझसे
जीवन को
नये अंदाज़ में
जीने का
सबक देने के लिए।
ज़िन्दगी निकल जाती है
कहाँ जान पाये हम
किसका ध्वंस उचित है
और किसका पालन।
कौन सा कर्म सार्थक होगा
और कौन-सा देगा विद्वेष।
जीवन-भर समझ नहीं पाते
कौन अपना, कौन पराया
किसके हित में
कौन है
और किससे होगा अहित।
कौन अपना ही अरि
और कौन है मित्र।
जब बुद्धि पलटती है
तब कहाँ स्मरण रहते हैं
किसी के
उपदेश और निर्देश।
धर्म और अधर्म की
गाँठे बन जाती हैं
उन्हें ही
बांधते और सुलझाते
ज़िन्दगी निकल जाती है
और एक नये
युद्धघोष की सम्भावना
बन जाती है।
अपने-आपसे करते हैं हम फ़रेब
अपने-आपसे करते हैं
हम फ़रेब
जब झूठ का
पर्दाफ़ाश नहीं करते।
किसी के धोखे को
सहन कर जाते हैं,
जब हँसकर
सह लेते हैं
किसी के अपशब्द।
हमारी सच्चाई
ईमानदारी का
जब कोई अपमान करता है
और हम
मन मसोसकर
रह जाते हैं
कोई प्रतिवाद नहीं करते।
हमारी राहों में
जब कोई कंकड़ बिछाता है
हम
अपनी ही भूल समझकर
चले रहते हैं
रक्त-रंजित।
औरों के फ़रेब पर
तालियाँ पीटते हैं
और अपने नाम पर
शर्मिंदा होते हैं।
मैं उपवास नहीं करती
मैं उपवास नहीं करती।
वह वाला
उपवास नहीं करती
जिसमें बन्धन हो।
मैंने देखा है
जो उपवास करते हैं
सारा दिन
ध्यान रहता है
अरे कुछ नहीं खाना
कुछ नहीं पीना।
अथवा
यह खाना और
यह पीना।
विशेष प्रकार का भोजन
स्वाद
कभी नमक रहित
कभी मिष्ठान्न सहित।
किस समय, किस रूप में,
यही चर्चा रहती है
दो दिन।
फिर
विशेष पूजा-पाठ,
सामग्री,
चाहे-अनचाहे
सबको उलझाना।
मैं बस मस्ती में जीती हूँ,
अपने कर्मों का
ध्यान करती हूँ,
अपनी ही
भूल-चूक पर
स्वयँ प्रायश्चित कर लेती हूँ
और अपने-आपको
स्वयँ क्षमा करती हूँ।
विचारों का झंझावात
अजब है
विचारों का झंझावात भी
पलट-पलट कर कहता है
हर बार नई बात जी।
राहें, चौराहे कट रहे हैं
कदम भटक रहे हैं
कहाँ से लाऊँ
पत्थरों से अडिग भाव जी।
जब धार आती है तीखी
तब कट जाते हैं
पत्थरों के अविचल भराव भी,
नदियों के किनारों में भी
आते हैं कटाव जी।
और ये भाव तो हवाएँ हैं
कब कहाँ रुख बदल जायेगा
नहीं पता हमें
मूड बदल जाये
तो दुनिया तहस-नहस कर दें
हमारी क्या बात जी।
तो कुछ
आप ही समझाएँ जनाब जी।
दिन सभी मुट्ठियों से फ़िसल जायेंगे
किसी ने मुझे कह दिया
दिन
सभी मुट्ठियों से
फ़िसल जायेंगे,
इस डर से
न जाने कब से मैंने
हाथों को समेटना
बन्द कर दिया है
मुट्ठियों को
बांधने से डरने लगी हूँ।
रेखाएँ पढ़ती हूँ
चिन्ह परखती हूँ
अंगुलियों की लम्बाई
जांचती हूँ,
हाथों को
पलट-पलटकर देखती हूँ
पर मुट्ठियाँ बांधने से
डरने लगी हूँ।
इन छोटी -छोटी
दो मुट्ठियों में
कितने समेट लूँगी
जिन्दगी के बेहिसाब पल।
अब डर नहीं लगता
खुली मुट्ठियों में
जीवन को
शुद्ध आचमन-सा
अनुभव करने लगी हूँ,
जीवन जीने लगी हूँ।
इक आग बनती है
तीली से तीली जलती है
यूँ ही इक आग बनती है।
छोटी-छोटी चिंगारियों से
दिल जलता है
कभी बुझता है
कभी भड़कता है।
राख के ढेर नहीं बनते
इतनी-सी आग से
किन्तु जले दिल में
कितने पत्थर
और पहाड़ बनते हैं
कुछ सरकते हैं
कुछ खड़े रहते हैं।
और हम, यूँ ही, बात-बेबात
मुस्कुराते रहते हैं।
दरकते पहाड़ों के बीच से
भरभराती मिट्टी
बहुत कुछ ले डूबती है
किन्तु कौन समझता है
हमारी इस बेमतलब मुस्कान को।
पाप की हो या पुण्य की गठरी
पाप की हो या
पुण्य की गठरी
तो भारी होती है।
कौन करेगा निर्णय
पाप क्या
या पुण्य क्या!
तू मेरे गिनता
मैं तेरे गिनती,
कल के डर से
काल के डर से
सहम-सहम
चलते जीवन में।
इहलोक यहीं
परलोक यहीं
सब लोक यहीं
यहीं फ़ैसला कर लें।
कल किसने देखा
चल आज यहीं
सब भूल-भुलाकर
जीवन
जी भर जी लें।
शुष्कता को जीवन में रोपते हैं
भावहीन मन,
उजड़े-बिखरे रिश्ते,
नेह के अभाव में
अर्थहीन जीवन,
किसी निर्जन वन-कानन में
अन्तिम सांसे गिन रहे
किसी सूखे वृक्ष-सा
टूटता है, बिखरता है।
बस
वृक्ष नहीं काटने,
वृक्ष नहीं काटने,
सोच-सोचकर हम
शुष्कता को जीवन में
रोपते रहते हैं।
रसहीन ठूंठ को पकड़े,
अपनी जड़ें छोड़ चुके,
दीमक लगी जड़ों को
न जाने किस आस में
सींचते रहते हैं।
समय कहता है,
पहचान कर
मृत और जीवन्त में।
नवजीवन के लिए
नवसंचार करना ही होगा।
रोपने होंगे नये वृ़क्ष,
जैसे सूखे वृक्षों पर फल नहीं आते
पक्षी बसेरा नहीं बनाते
वैसे ही मृत आकांक्षाओं पर
जीवन नहीं चलता।
भावुक न बन।
जब मन में कांटे उगते हैं
हमारी आदतें भी अजीब सी हैं
बस एक बार तय कर लेते हैं
तो कर लेते हैं।
नज़रिया बदलना ही नहीं चाहते।
वैसे मुद्दे तो बहुत से हैं
किन्तु इस समय मेरी दृष्टि
इन कांटों पर है।
फूलों के रूप, रस, गंध, सौन्दर्य
की तो हम बहुत चर्चा करते हैं
किन्तु जब भी कांटों की बात उठती है
तो उन्हें बस फूलों के
परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं।
पता नहीं फूलों के संग कांटे होते हैं
अथवा कांटों के संग फूल।
लेकिन बात दाेनों की अक्सर
साथ साथ होती है।
बस इतना ही याद रखते हैं हम
कि कांटों से चुभन होती है।
हां, होती है कांटों से चुभन।
लेकिन कांटा भी तो
कांटे से ही निकलता है।
आैर कभी छीलकर देखा है कांटे को
भीतर से होता है रसपूर्ण।
यह कांटे की प्रवृत्ति है
कि बाहर से तीक्ष्ण है,
पर भीतर ही भीतर खिलते हैं फूल।
संजोकर देखना इन्हें,
जीवन भर अक्षुण्ण साथ देते है।
और
जब मन में कांटे उगते हैं
तो यह पलभर का उद्वेलन नहीं होता।
जीवन रस
सूख सूख कर कांटों में बदल जाता है।
कोई जान न पाये इसे
इसलिए कांटों की प्रवृत्ति के विपरीत
हम चेहरों पर फूल उगा लेते हैं
और मन में कांटे संजोये रहते हैं ।
पुल अपनों और सपनों के बीच
सारा जीवन बीत गया
इसी उहापोह में
क्या पाया, क्या गंवाया।
बस आकाश ही आकाश
दिखाई देता था
पैर ज़मीन पर न टिकते थे।
मिट्टी को मिट्टी समझ
पैरों तले रौंदते थे।
लेकिन, एक समय आया
जब मिट्टी में हाथ डाला
तो, मिट्टी ने चूल्हा दिया,
घर दिया,
और दिया भरपेट भोजन।
मिट्टी से सने हाथों से ही
साकार हुए वे सारे स्वर्णिम सपने
जो आकाश में टंगे
दिखाई देते थे,
और बन गया एक पुल
ज़मीन और आकाश के बीच।
अपनों और सपनों के बीच।
कांटों की बुआई में
तीर की जगह तुक्का चलाना आ गया।
झूठ को सच, सच को झूठ बनाना आ गया।
कांटों की बुआई में हाथ बहुत साफ़ है,
किसी की चुभन देख मुस्कुराना आ गया।