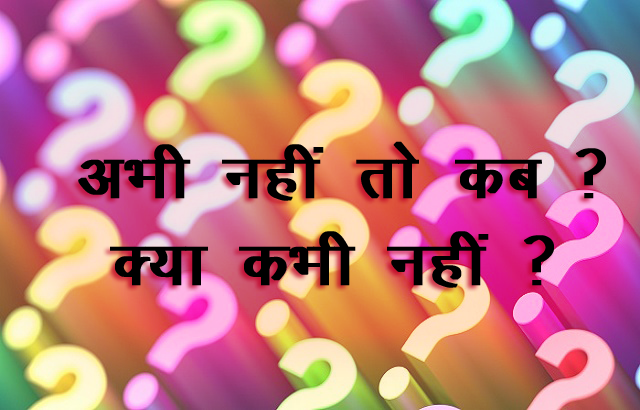दोनों अपने-अपने पथ चलें
तुम अपनी राह चलो,
मैं अपनी राह चलूंगी।
.
दोनों अपने-अपने पथ चलें
दोनों अपने-अपने कर्म करें।
होनी-अनहोनी जीवन है,
कल क्या होगा, कौन कहे।
चिन्ता मैं करती हूं,
चिन्ता तुम करते हो।
पीछे मुड़कर न देखो,
अपनी राह बढ़ो।
मैं भी चलती हूं
अपने जीवन-पथ पर,
एक नवजीवन की आस में।
तुम भी जाओ
कर्तव्य निभाने अपने कर्म-पथ पर।
डर कर क्या जीना,
मर कर क्या जीना।
आशाओं में जीते हैं।
आशाओं में रहते हैं।
कल आयेगा ऐसा
साथ चलेगें]
हाथों में हाथ थाम साथ बढ़ेगें।
मेरा भारत महान
ऐसे चित्र देखकर
मन द्रवित, भावुक होता है,
या क्रोधित,
अपनी ही समझ नहीं आता।
.
कुछ कर नहीं सकते,
या करना नहीं चाहते,
किंतु बनावट की कहानियां,
इस तरह की बानियां,
गले नहीं उतरतीं।
मेरा भारत महान है।
महान ही रहेगा।
पर रोटी, कपड़ा, मकान
की बात कौन करेगा?
सोचती हूं
बच्चे के हाथ में
किसने दी
स्लेट और चाॅक,
और कौन सिखा रहा
इसे लिखना
मेरा भारत महान?
स्लेट की जगह दो रोटी दे देते,
और देते पिता को कोई काम।
बच्चे के तन पर कपड़े होते,
तब शायद मुझे लगता,
मेरा भारत और भी ज़्यादा महान।
मन में बसन्त खिलता है
जीवन में कुछ खुशियां
बसन्त-सी लगती हैं।
और कुछ बरसात के बाद
मिट्टी से उठती
भीनी-भीनी खुशबू-सी।
बसन्त के आगमन की
सूचना देतीं,
आती-जाती सर्द हवाएं,
झरते पत्तों संग खेलती हैं,
और नव-पल्ल्वों को
सहलाकर दुलारती हैं।
पत्तों पर झूमते हैं
तुषार-कण,
धरती भीगी-भीगी-सी
महकने लगती है।
फूलों का खिलना
मुरझाना और झड़ जाना,
और पुनः कलियों का लौट आना,
तितलियों, भंवरों का गुनगुनाना,
मन में यूं ही
बसन्त खिलता है।
सागर की गहराईयों सा मन
सागर की गहराईयों सा मन।
सागर के सीने में
अनगिन मणि-रत्नम्
कौन ढूंढ पाया है आज तलक।
.
मन में रहते भाव-संगम
उलझे-उलझे, बिखरे-बिखरे,
कौन समझ पाया है
आज तलक।
.
लहरें आती हैं जाती हैं,
हिचकोले लेती नाव।
जग-जगत् में
मन भागम-भाग किया करता है,
कहां मिलता आराम।
.
खुले नयनों पर वश है अपना,
देखें या न देखें।
पर बन्द नयन
न जाने क्या-क्या दिखला जाते हैं,
अनजाने-अनचाहे भाव सुना जाते हैं,
जिनसे बचना चाहें,
वे सब रूप दिखा जाते हैं।
अगला-पिछला, अच्छा-बुरा
सब हाल बता जाते हैं,
अनचाहे मोड़ों पर खड़ा कर
कभी हंसी देकर,
तो कभी रूलाकर चले जाते हैं।
बुरा लगा शायद आपको
यह कहना
आजकल एक फ़ैशन-सा हो गया है,
कि इंसान विश्वास के लायक नहीं रहा।
.
लेकिन इतना बुरा भी नहीं है इंसान,
वास्तव में,
हम परखने-समझने का
प्रयास ही नहीं करते।
तो कैसे जानेंगे
कि सामने वाला
इंसान है या कुत्ता।
.
बुरा लगा शायद आपको
कि मैं इंसान की
तुलना कुत्ते से कर बैठी।
लेकिन जब सब कहते हैं,
कुत्ता बड़ा वफ़ादार होता है,
इंसान से ज्यादा भरोसेमंद होता है,
तब आपको क्यों बुरा नहीं लगता।
.
आदमी की
अक्सर यह विशेषता है
कह देता है मुंह खोल कर
अच्छा लगे या बुरा।
.
कुत्ता कितना भी पालतू हो,
काटने का डर तो रहता ही है
उससे भी।
और कुत्ता जब-तब
भौंकता रहता है,
हम बुरा नहीं मानते ज़रा भी,
-
इंसान की बोली
अक्सर बहुत कड़वी लगती है,
जब वह
हमारे मन की नहीं बोलता।
मन उदास क्यों है
कभी-कभी
हम जान ही नहीं पाते
कि मन उदास क्यों है।
और जब
उदास होती हूं,
तो चुप हो जाती हूं अक्सर।
अपने-आप से
भीतर ही भीतर
तर्क-वितर्क करने लगती हूं।
तुम इसे, मेरी
बेबात की नाराज़गी
समझ बैठते हो।
न जाने कब के रूके आंसू
आंखों की कोरों पर आ बैठते हैं।
मन चाहता है
किसी का हाथ
सहला जाये इस अनजाने दर्द को।
लेकिन तुम इसे
मेरा नाराज़गी जताने का
एहसास कराने का
नारीनुमा तरीका मान लेते हो।
.
पढ़ लेती हूं
तुम्हारी आंखों में
तुम्हारा नज़रिया,
तुम्हारे चेहरे पर खिंचती रेखाएं,
और तुम्हारी नाराज़गी।
और मैं तुम्हें मनाने लगती हूं।
अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति
हिन्दी को वे नाम दे गये, हिन्दी को पहचान दे गये ।
अटल वाणी से वे जग में अपनी अलग पहचान दे गये।
शत्रु से हाथ मिलाकर भी ताकत अपनी दिखलाई थी ,
विश्व-पटल पर अपनी वाणी से भारत को पहचान दे गये।
कहलाने को ये सन्त हैं
साठ करोड़ का आसन, सात करोड़ के जूते,
भोली जनता मूरख बनती, बांधे इनके फीते,
कहलाने को ये सन्त हैं, करते हैं व्यापार,
हमें सिखायें सादगी आप जीवन का रस पीते।
झूठी-सच्ची ख़बरें बुनते
नाम नहीं, पहचान नहीं, करने दो मुझको काम।
क्यों मेरी फ़ोटो खींच रहे, मिलते हैं कितने दाम।
कहीं की बात कहीं करें और झूठी-सच्ची ख़बरें बुनते
समझो तुम, मिल-जुलकर चलता है घर का काम।
सफ़लता की कुंजी
कुछ घोटाले कर गये होते, हम भी अमर हो गये होते ।
संसद में बैठे, गाड़ी-बंगला-पैंशन ले, विदेश बस गये होते।
फिसड्डी बनकर रह गये, इस ईमानदारी से जीते जीते,
बुद्धिमानी की होती, जीते-जी मूर्ति पर हार चढ़ गये होते।
मन की बातें न बताएं
पन्नों पर लिखी हैं मन की वे सारी गाथाएं
जो दुनिया तो जाने थी पर मन था छुपाए
पर इन फूलों के अन्तस में हैं वे सारी बातें
न कभी हम उन्हें बताएं न वो हमें जताएं
सम्बन्धों की डोर
विशाल वृक्षों की जड़ों से जब मिट्टी दरकने लगती है।
जिन्दगी की सांसें भी तब कुछ यूं ही रिसने लगती हैं।
विशाल वृक्षों की छाया तले ही पनपने हैं छोटे पेड़ पौधे,
बड़ों की छत्रछाया के बिना सम्बन्धों की डोर टूटने लगती है।
हम सजग प्रहरी
द्वार के दोनों ओर खड़े हैं हम सजग प्रहरी
परस्पर हमारी न शत्रुता, न कोई भागीदारी
मध्य में एक रेखा खींचकर हमें किया विलग
इसी विभाजन के समक्ष हमारी मित्रता हारी
काम की कर लें अदला-बदली
धरने पर बैठे हैं हम, रोटी आज बनाओ तुम।
छुट्टी हमको चाहिए, रसोई आज सम्हालो तुम।
झाड़ू, पोचा, बर्तन, कपड़े, सब करना होगा,
हम अखबार पढ़ेंगें, धूप में मटर छीलना तुम।
प्रेम-प्यार के मधुर गीत
मौसम बदला, फूल खिले, भंवरे गुनगुनाते हैं।
सूरज ने धूप बिखेरी, पंछी मधुर राग सुनाते हैं।
जी चाहता है भूल जायें दुनियादारी के किस्से,
चलो मिलकर प्रेम-प्यार के मधुर गीत गाते हैं।
प्रेम-प्यार की बात न करना
प्रेम-प्यार की बात न करना,
घृणा के बीज हम बो रहे हैं।
.
सम्बन्धों का मान नहीं अब,
दीवारें हम अब चिन रहे हैं।
.
काले-गोरे की बात चल रही,
चेहरों को रंगों से पोत रहे हैं ।
.
अमीर-गरीब की बात कर रहे,
पैसे से दुनिया को तोल रहे हैं ।अ
.
कौन है सच्चा, कौन है झूठा,
बिन जाने हम कोस रहे हैं।
.
पढ़ना-लिखना बात पुरानी
सुनी-सुनाई पर चल रहे हैं।
.
सर्वधर्म समभाव भूल गये,
भेद-भाव हम ढो रहे हैं।
.
अपने-अपने रूप चुन लिए,
किस्से रोज़ नये बुन रहे हैं।
-
राजनीति का ज्ञान नहीं है
चर्चा में हम लगे हुए हैं।
जब लहराता है तिरंगा
एक भाव है ध्वजा,
देश के प्रति साख है ध्वजा।
प्रतीक है,
आन का, बान का, शान का।
.
तीन रंगों से सजा,
नारंगी, श्वेत, हरा
देते हमें जीवन के शुद्ध भाव,
शक्ति, साहस की प्रेरणा,
सत्य-शांति का प्रतीक,
धर्म चक्र से चिन्हित,
प्रकृति, वृद्धि एवं शुभता
की प्रेरणा।
भाव है अपनत्व का।
शीश सदा झुकता है
शीष सदा मान से उठता है,
जब लहराता है तिरंगा।
जीवन चक्र तो चलता रहता है
जीवन चक्र तो चलता रहता है
अच्छा लगा
तुम्हारा अभियान।
पहले
वंशी की मधुर धुन पर
नेह दिया,
सबको मोहित किया,
प्रेम का संदेश दिया।
.
उपरान्त
शंखनाद किया,
एक उद्घोष, आह्वान,
सत्य पर चलने का,
अन्याय का विरोध,
अपने अधिकारों के लिए
मर मिटने का,
चक्र थाम।
.
और एक संदेश,
जीवन-चक्र तो चलता रहता है,
तू अपना कर्म किये जा
फल तो मिलेगा ही।
मेरी असमर्थ अभिव्यक्ति
जब भी
कुछ कहने का
प्रयास करती हूं कविता में,
तभी पाती हूं
कि उसे ही
एक अनजानी सी भाषा में,
अनजाने अव्यक्त शब्दों में,
जिनसे मैं जुड़ नहीं पाती
पूरी कोशिश के बावजूद भी,
किसी और ने
पहले ही कह रखी है वह बात।
.
या फिर
अनुभव मैं यह करती हूं,
कि जो मैं कहना चाहती हूं,
वह किसी और ने
मेरी ही भावनाएं चुराकर,
मानों मुझसे ही पूछकर,
मेरे ही विचार
मेरी ही इच्छानुसार,
लेकिन मुझसे पहले ही
अभिव्यक्त कर दिये हैं,
सही शब्दों में
सही लोगों के सामने
और सही रूप में।
शब्दों की तलाश में
भटकती थी मैं
जिनकी अभिव्यक्ति के लिए।
सारे शब्द
निर्थरक हो जाते थे
जिसे कहने के लिए मेरे सामने
वही बातें
कविता में व्यक्त कर दी हैं
किसी ने मानों
मेरी ही इच्छानुसार।
या फिर
तुम्हारा, उसका, इसका
सबका लिखा
गलत लगता है।
झूठ और छल।
मानों सब मिलकर
मेरे विरूद्ध
एक षड्यन्त्र के भागीदार हों।
मैं,
विरोध में कलम उठाती हूं
लिखना चाहती हूं
तुम्हारे, उसके, इसके लिखे के विरोध में।
बार बार लिखती हूं
पर फिर भी
अनलिखी रह जाती हूं
अनुभव बस एक अधूरेपन का।
आक्रोश, गुस्सा, झुंझलाहट,
विरोध, विद्रोह,
कुछ नहीं ठहरता।
इससे पहले कि लिखना पूरा करूं
चाय बनानी है, रोटी पकानी है
कपड़े धोने हैं
बीच में बच्चा रोने लगेगा
इसी बीच
स्याही चुक जाती है।
रोज़ नया आक्रोश जन्म लेता है
और चाय के साथ उफ़नकर
ठण्डा हो जाता है।
कभी लिख भी लेती हूं
तो बड़ा नाम नहीं है मेरे पास।
सम्पर्क साधन भी नहीं।
किसी गुट में भी नहीं।
फिर, किसी प्राध्यापक की
चरण रज भी नहीं ली मैंने।
किसी के बच्चे को टाफ़ियां भी नहीं खिलाईं
और न ही किसी की पत्नी को
भाभीजी बनाकर उसे तोहफ़े दिये।
मेरे पिता के पास भी
इतनी सामर्थ्य न थी
कि वे उनका कोई काम कर देते।
फिर वे मेरी रचनाओं में रूचि कैसे लेते।
और
इस सबके बाद भी लगता है
मैं ही गलत हूं कहीं
खामोश हो जीती हूं तब
अनकही, यह सोचकर
कि चलो
मेरे विचारों की अभिव्यक्ति हुई तो सही
मेरे द्वारा नहीं
तो किसी और के माध्यम से ही सही
पूर्णतया अस्पष्ट तो रही नहीं
प्रकट तो हुई
स्वयं नहीं कर पाई
तो किसी और की कृपा से
लोगों तक बात पहुंची तो सही
शायद यही कारण है
कि लोगों की लिखी कविताओं का
इतना बड़ा संग्रह मेरे पास है
जो कहीं मेरा अपना है।
पर सचमुच
आश्चर्य तो होता ही है
कि मेरे विचार
मेरी ही इच्छानुसार
मैं नहीं कोई और
कैसे अभिव्यक्त कर लेते हैं
इतने समर्थ होकर
.
जो मैं चाहती हूं
वही तुम भी चाहते हो
ऐसा कैसे।
तो क्या
इस दुनिया में
मेरे अतिरिक्त भी इंसान बसते हैं
या फिर
इस दुनिया में रहकर भी
मेरे भीतर इंसानियत बची है !
चिड़िया ने कहानी सुनाई
अरे,
एक–एक कर बोलो।
थक-हार कर आई हूं,
दाना-पानी लाई हूं,
कहां-कहां से आई हूं।
तुमको रोज़ कहानी चाहिए।
दुनिया की रवानी चाहिए।
अब तुमको क्या बतलाउं मैं
सुन्दर है यह दुनिया
बस लोग बहुत हैं।
रहने को हैं घर बनाते
जैसे हम अपना नीड़ सजाते।
उनके भी बच्चे हैं
छोटे-छोटे
वे भी यूं ही चिन्ता करते,
जब भी घर से बाहर जाते।
प्रेम, नेह , ममता लुटाते।
वे भी अपना कर्त्तव्य निभाते।
रूको, रूको, बतलाती हूं
अन्तर क्या है।
आशाओं, अभिलाषाओं का अन्त नहीं है।
जीने का कोई ढंग नहीं है।
भागम-भाग पड़ी है।
और चाहिए, और चाहिए।
बस यूं ही मार-काट पड़ी है।
घर-संसार भरा-पूरा है,
तो भी लूट-खसोट पड़ी है।
उड़ते हैं, चलते हैं, गिरते हैं,
मरते हैं
पता नहीं क्या क्या करते है।
चाहतें हैं कि बढ़ती जातीं।
बच्चों पर भी डाली जातीं।
बचपन मानों बोझ बना
मां-पिता की इच्छाओं का संसार घना।
अब क्या –क्या बतलाउं मैं।
आज बस इतना ही,
दाना लो और पिओ
जी भरकर विश्राम करो।
बस इतना ही जानो कि
इन तिनकों, पत्तों में,
रूखे-सूखे चुग्गे में,
बूंद-बूंद पानी में,
अपनी इस छोटी सी कहानी में,
जीवन में आनन्द भरा है।
उड़ना तुमको सिखलाती हूं।
बस इतना ही बतलाती हूं।
पंख पसारे
उड़ जाना तुम,
अपनी दुनिया में रहना तुम।
अपना कर्त्तव्य निभाना तुम।
अगली पीढ़ी को
अपने पंखों पर उड़ना सिखलाना तुम।
वृक्षों की लहराती शाखाएं
पुष्प पल्लवविहीन
एक छत्रछाया सी दिखती हैं।
दुलारती, आंचल फैलाकर।
समझाती हैं
न डर
थोड़ा सब्र कर।
पतझड़, सूखा, ग्रीष्म
और यह सूनापन
तो आने जाने हैं।
बस ठहर ज़रा
मौसम बदलेगा
फूल खिलेंगे
सूरज चमकेगा
सागर लहरायेगा
बस फिर
तुम ज़रा सा मुस्कुरा देना।
स्वाधीनता हमारे लिए स्वच्छन्दता बन गई
एक स्वाधीनता हमने
अंग्रेज़ो से पाई थी,
उसका रंग लाल था।
पढ़ते हैं कहानियों में,
सुनते हैं गीतों में,
वीरों की कथाएं, शौर्य की गाथाएं।
किसी समूह,
जाति, धर्म से नहीं जुड़े थे,
बेनाम थे वे सब।
बस एक नाम जानते थे
एक आस पालते थे,
आज़ादी आज़ादी और आज़ादी।
तिरंगे के मान के साथ
स्वाधीनता पाई हमने
गौरवशाली हुआ यह देश।
मुक्ति मिली हमें वर्षों की
पराधीनता से।
हम इतने अधीर थे
मानों किसी अबोध बालक के हाथ
जिन्न लग गया हो।
समझ ही नहीं पाये,
कब स्वाधीनता हमारे लिए
स्वच्छन्दता बन गई।
पहले देश टूटा था,
अब सोच बिखरने लगी।
स्वतन्त्रता, आज़ादी और
स्वाधीनता के अर्थ बदल गये।
मुक्ति और स्वायत्तता की कामना लिए
कुछ शब्दों के चक्रव्यूह में फ़ंसे हम,
नवीन अर्थ मढ़ रहे हैं।
भेड़-चाल चल रहे हैं।
आधी-अधूरी जानकारियों के साथ
रोज़ मर रहे हैं और मार रहे हैं।
-
वे, जो हर युग में आते थे
वेश और भेष बदल कर,
लगता है वे भी
हार मान बैठ हैं।
कैसे मना रहे हम अपने राष्ट्रीय दिवस
हमें स्वतन्त्र हुए
इतने
या कितने वर्ष हो गये,
इस बार हम
कौन सा
गणतन्त्र दिवस
या स्वाधीनता दिवस
मनाने जा रहे हैं,
गणना करने लगे हैं हम।
उत्सवधर्मी तो हम हैं ही।
सजने-संवरने में लगे हैं हम।
गली-गली नेता खड़े हैं,
अपने-अपने मोर्चे पर अड़े हैं,
इस बार कौन ध्वज फ़हरायेगा
चर्चा चल रही है।
स्वाधीनता सेनानियों को
आज हम इसलिए
स्मरण नहीं कर रहे
कि उन्हें नमन करें,
हम उन्हें जाति, राज्य और
धर्म पर बांध कर नाप रहे।
सड़कों पर चीखें बिखरी हैं,
सुनाई नहीं देती हमें।
सैंकड़ों जाति, धर्म वर्ग बताकर
कहते हैं
हम एक हैं, हम एक हैं।
किसको सम्मान मिला,
किसे नहीं
इस बात पर लड़-मर रहे।
मूर्तियों में
इनके बलिदानों को बांध रहे।
पर उनसे मिली
अमूल्य धरोहर को कौन सम्हाले
बस यही नहीं जान रहे।
जब नर या कुंजर कहा गया
महाभारत का युद्ध पलट गया जब नर या कुंजर कहा गया।
गज-गामिनी, मदमस्त चाल कहने वाला कवि आज कहां गया।
नहीं भाते इसे मानव-निर्मित वन-अभयारण्य, जल-स्त्रोत यहां।
मुक्त जीव, जब मूड बना, तब मनमौजी हर की पौड़ी नहा गया।
छोटे-छोटे घर हैं छोटे-छोटे सपने
छोटे-छोटे घर हैं, छोटे-छोटे सपने
घर के भीतर रहते हैं यहां सब अपने
न ताला-चाबी, न द्वार, न चोर यहां
फूलों से सज्जित, ये घर सुन्दर कितने
मौसम के रूप समझ न आयें
कोहरा है या बादलों का घेरा, हम बनते पागल।
कब रिमझिम, कब खिलती धूप, हम बनते पागल।
मौसम हरदम नये-नये रंग दिखाता, हमें भरमाता,
मौसम के रूप समझ न आयें, हम बनते पागल।
सच्चाई से भाग रहे
मुख देखें बात करें।
सुख देखें बात करें।
सच्चाई से भाग रहे,
धन देखें बात करें।
किसे अपना समझें किसे पराया
किसे अपना समझें किसे पराया
मन के द्वार पर पहरे लगाकर बैठे हैं आज।
कोई भाव पढ़ न ले, गांठ बांध कर बैठे हैं आज।
किसे अपना समझें, किसे पराया, समझ नहीं,
अपनों को ही पराया समझ कर बैठे हैं आज।
कहानी टूटे-बिखरे रिश्तों की
कुछ यादें,
कुछ बातें चुभती हैं
शीशे की किरचों-सी।
रिसता है रक्त, धीरे-धीरे।
दाग छोड़ जाता है।
सुना है मैंने
खुरच कर नमक डालने से
खुल जाते हैं ऐसे घाव।
किरचें छिटक जाती हैं।
अलग-से दिखाई देने लगती हैं।
घाव की मरहम-पट्टी को भूलकर,
हम अक्सर उन किरचों को
समेटने की कोशिश करते हैं।
कि अरे !
इस छोटे-से टुकड़े ने
इतने गहरे घाव कर दिये थे,
इतना बहा था रक्त।
इतना सहा था दर्द।
और फिर अनजाने में
फिर चुभ जाती हैं वे किरचें।
और यह कहानी
जीवन भर दोहराते रहते हैं हम।
शायद यह कहानी
किरचों की नहीं,
टूटे-बिखरे रिश्तों की है ,
या फिर किरचों की
या फिर टूटे-बिखरे रिश्तों की ।।।।
मज़बूरी से बड़ी होती है जिद्द
सुना है मैंने,
रेत पर घरौंदे नहीं बनते।
धंसते हैं पैर,
कदम नहीं उठते।
.
वैसे ऐसा भी नहीं
कि नामुमकिन हो यह।
सीखते-सीखते
सब सीख जाता है इंसान,
‘गर मज़बूरी हो
या जिद्द।
.
मज़बूरी से बड़ी होती है जिद्द,
और जब जिद्द हो,
तो रेत क्या
और पानी क्या,
घरौंदे भी बनते हैं ,
पैर भी चलते हैं,
और ऐसे ही कारवां भी बनते हैं।