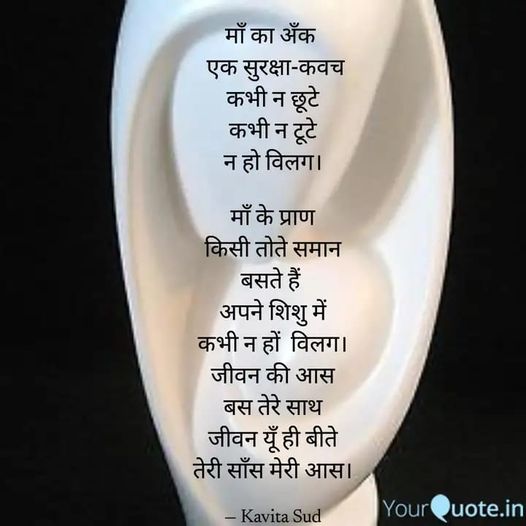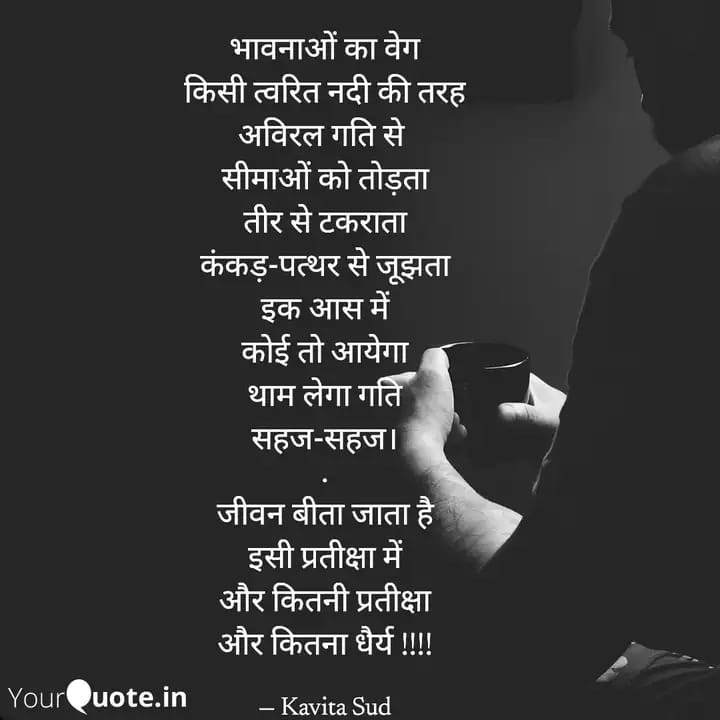जीवन और परिवर्तन
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिस पर मनुष्य का नियन्त्रण नहीं। मानव कितना ही शक्तिशाली हो जाये, प्रकृति में नित्य प्रति आने वाले परिवर्तन पर नियन्त्रण नहीं कर सकता। शीत को ग्रीष्म में और ग्रीष्म को शिशिर में नहीं बदल सकता।
वास्तव में परिवर्तन विकास, चेतना, चिन्तन का प्रतीक है। परिवर्तन हमारी इच्छाओं, कामनाओं, लालसाओं का दूसरा नाम है। जिस दिन परिवर्तन रुक जायेगा, उस दिन मानवता भी ठहर जायेगी। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन विकास का ही दूसरा नाम है।
एक परिवर्तन सहज-स्वाभाविक है और दूसरा परिवर्तन सप्रयास। परिवर्तन प्रायः आवश्यकता आधारित होता है और अब आवश्यकताएँ लगभग पूर्ण होने लगती हैं तब लालसा एवं प्रदर्शन के कारण भी हम जीवन में परिवर्तन करने लगते हैं।
मनुष्य की चेतना उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि तथा अन्य सभी गुणों का आधार है। यह व्यक्ति मानस की प्रमुख विषेशता होने के साथ.साथ निरन्तर परिवर्तनशील हैए अतः विकासोन्मुख हैए स्थिर या जड़ नहीं। यही उसे पाशव स्तर से उठाकर मानव स्तर तक ले आती है।
इसी कारण सृष्टि के आरम्भ होते ही परिवर्तन, विकास और चिन्तन की प्रक्रिया आरम्भ हुई, इसी कारण आज मानव आधुनिकता के इस द्वार पर खड़ा है। जंगल में रहते हुए मानव ने अपने हित में, अपनी सुरक्षा और जीवन-यापन के लिए प्रकृति के साथ मिलकर परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की होगी। गुफ़ाओं को घर बनाया होगा, उन्हें सुरक्षित किया होगा, जीवन-यापन के लिए, भोज्य सामग्री की तलाश की होगी। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षा साधनों का विकास किया होगा। परिवर्तन और विकास की यह प्रक्रिया इतनी लम्बी रही होगी कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। एकल मानव संगठित हुआ, समूह बने होंगें, और अन्ततः परिवर्तन और विकास की आँधी ने उसे आज आधुनिकता के चरम तक पहुँचा दिया है।
जीवन के इस परिवर्तन को यदि हम सहज-स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। क्योंकि जब भौतिक परिवर्तन होता है तब विचारों, भावों, रीति-परम्पराओं, रहन-सहन, शिक्षा, संस्कारों, व्यवहार, सामाजिकता, पारिवारिक संगठन, परिवेश, वेश-भूषा सबमें परिवर्तन अवश्यम् भावी है। भौतिक परिवर्तन एवं विकास के साथ बहुत कुछ पुराना छूटना स्वाभाविक है और नये को स्वीकार करना जीवनगत आवश्यकता।
इस वास्तविकता को, इस परिवर्तन को, हम जितनी सहजता से स्वीकार कर लें, जीवन की प्रक्रिया भी उतनी ही सरल-सहज होने लगती है।
किन्तु समस्या यह कि हम भौतिक परिवर्तन को तो स्वीकार कर रहे हैं किन्तु कहीं-कहीं पुरातनता का लबादा ओढ़ने में, प्रदर्शन करने में हमें आनन्द मिलता है। हम भौतिक परिवर्तन एवं वैचारिक परिवर्तन में तालमेल नहीं बिठाना चाहते।
हमारे आधुनिक समाज की यही समस्या है कि हम आधुनिक तो होना चाहते हैं, सब सुविधाएँ भी चाहिए किन्तु न जाने कहाँ-कहाँ पुरातनता ढूँढते हैं और अपने सुखमय वर्तमान को कोसते रहते हैं। आवश्यकता है, भौतिक परिर्वतन अर्थात भौतिक विकास एवं वैचारिक परिवर्तन अर्थात विचारधारा में एक परिपक्व समझ की।
परिवर्तन सकारात्मक भी होते हैं और विरोधाभासी भी। नकारात्मक परिवर्तन हमारे विचारों में होते हैं जिस कारण अनेक बार विकासात्मक परिवर्तन बाधित होता है।
वर्तमान में परिवर्तन में जिस विषय पर सर्वाधिक चर्चा की जाती है वह है हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति-रिवाज़ों, व्यवहार आदि में परिवर्तन की। निःसंदेह हमारी प्राचीन संस्कृति, रीति, परम्पराएँ, व्रतोपवास, पूजा-विधि, उपचार-पद्धति आदि उत्कृष्ट रहे हैं किन्तु वर्तमान जीवन पद्धति में प्राचीन काल की भाँति इनका अनुपालन सम्भव ही नहीं है। विशेषकर नई पीढ़ी आधुनिकता की सीढ़ियाँ चढ़ती प्राचीनता के प्रति आग्रही नहीं हो पा रही है। हम बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकतम् सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन देना चाहते हैं, जीवन की प्रत्येक सुख-सुविधा प्रदान करना चाहते हैं फिर वह शिक्षा हो, रहन-सहन हो, पहनावा हो अथवा अन्य कोई भी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक अथवा भौतिक आवश्यकता। किन्तु हम इस बात पर कदापि विचार नहीं करते कि जब भौतिक सुख-साधन बदलते हैं तब मानसिक विचारधाराएँ स्वयंमेव ही बदल जाती हैं। इस परिवर्तन में कुछ भी ठीक अथवा गलत नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है। परिवर्तन के इस दोहरे रूप को समझना और स्वीकार करना ही जीवन की सफ़लता है।
आत्म संतोष क्या जीवन की उपलब्धि है
प्रायः कहा जाता है कि जीवन में आत्म-संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही परम संतोष है।
किन्तु आत्म संतोष क्या है?
क्या अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं का दमन आत्म-संतोष का मार्ग है?
वास्तविक धरातल पर जीवन जीना जितना कठिन और कटु है उपदेश देना और सुनाना उतना ही सरल।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
वर्तमान उलझनों भरे जीवन, भागम-भाग की जीवन शैली, प्रतियोगिताओं, एक-दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़, प्रतिदिन कुछ नया पाने की चाहत, पुरातनता और नवीनता के बीच उलझते, परम्पराओं, संस्कृति और आधुनिकतम जीवन शैली; तब आत्म संतोष कहाँ और परम संतोष कहाँ! हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएँ और सीमाएँ केवल हमारी नहीं होती, हमारे परिवेश से जुड़ी होती हैं।
आत्म संतोष की सीमा क्या है, कौन सा द्वार है जहाँ पहुँच कर हम यह समझ लें कि अब बस। जीवन की समस्त उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली हमने। अब परम धाम चलते हैं। क्या ऐसा सम्भव है?
जी नहीं, बनी-बनाई उपदेशात्मक सूक्तियाँ सुना देना, कुछ आप्त वाक्य बोल देना, ग्रंथों से सूक्तियाँ उद्धृत करना और यह कहना कि हममें आत्म संतोष होना चाहिए और वह ही परम संतोष है, किसी के भी जीवन का सबसे बड़ा झूठ और छल है।
हम यह नहीं कह सकते कि आत्म-संतोष मिल गया और हम परम संतोष की अवस्था में पहुँच गये।
मेरे विचार में आत्म संतोष क्षणिक है, सीमित है, इसका विस्तार जीवनगत नहीं है। जैसे हम कहते हैं आज मेरे बच्चे को मेरा बनाया भोजन बहुत पसन्द आया, मुझे आत्म संतोष मिला। अथवा आज मैंने किसी की सहायता की, मन आत्म-संतोष से भर गया, और मैं परम संतोष की अवस्था में पहुँच गई। अथवा मेरे व्यवहार से वे प्रसन्न हुए, मुझे आत्म-संतोष मिला अथवा परम संतोष मिला।
संतोष की अन्तिम स्थिति हमारे जीवन में सम्भव ही नहीं क्योंकि हम सामाजिक, पारिवारिक प्राणी हैं और आत्म संतोष एवं परम संतोष के लिए प्रतिदिन हम प्रयासरत रहते हैं।
सामाजिक जीवन में, समाज में रहते हुए, अपनी इच्छाओं का दमन करना आत्म संतोष नहीं है, आत्म-संतोष है जीवन में उपलब्धि, लक्ष्य की प्राप्ति, सफ़लता। जीवन में आत्म संतोष किसी एक कार्य से नहीं मिलता, प्रति दिन और बार-बार किये जाने वाले कार्यों से मिलता रहता है, यह एक आजीवन प्रक्रिया है।
अतः आत्म संतोष अथवा परम संतोष जीवन की चरम प्राप्ति अथवा उपलब्धि नहीं है, हमारे कार्यों, व्यवहार से उपजा भाव है जिसकी प्राप्ति के लिए हम हर समय प्रयासरत रहते हैं।
बुद्धम् शरणम गच्छामि
कथाओं के अनुसार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कथा है। 563 ईसा पूर्व। एक राजकुमार अपनी सोती हुई पत्नी एवं नवजाव शिशु को आधी रात में त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चला गया। उस युवक ने घोर तपस्या की, साधना की और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सम्पूर्ण जगत को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, सत्य एवं दिव्य ज्ञान की खोज के लिए जगत के हित के लिए वर्षों कठोर साधना की और अन्त में बिहार बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ओर वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गये।
जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अपने परिवार का परित्याग किया, जो कि उनका दायित्व था क्या उस ज्ञान का उपयोग आज यह संसार कर रहा है? क्या जगत के लिए उनका ज्ञान और उपदेश चरम उपलब्धि था?
यदि था तो उनके उपरान्त क्यों आवश्यकता पड़ी कि एक-अनेक युग-पुरुष आये जिन्होंने संसार को पुनः उपदेश दिये, अपने ज्ञान की धारा बहाई, ग्रंथ लिखे गये, आप्त वाक्य बने और यह क्रम आज भी चल रहा है। एक समय बाद ज्ञान की धारा धर्म का रूप ले लेती है। उपदेश की पुनरावृत्ति होती है हर युग में, केवल नाम बदलते हैं, स्थापनाएँ नहीं बदलतीं।
जब भी गौतम बुद्ध के त्याग, ज्ञान, बौद्धित्व, साधना की बात की जाती है मुझे केवल नवजात शिशु और यशोधरा की याद आती है, उनके प्रति कर्तव्य, विश्वास की डोर टूटी तो सम्पूर्ण जगत के साथ कैसे जोड़ी?
निडर भाव रख
राही अपनी राहों पर चलते जाते
मंज़िल की आस लिए बढ़ते जाते
बाधाएँ तो आती हैं, आनी ही हैं
निडर भाव रख मन की करते जाते।
स्त्री की बात
जब कोई यूं ही
स्त्री की बात करता है
मैं समझ नहीं पाती
कि यह राहत की बात है
अथवा चिन्ता की
बहुत आनन्द आता है मुझे
बहुत आनन्द आता है मुझे
जब लोग कहते हैं
सब ऊपर वाले की मर्ज़ी।
बहुत आनन्द आता है मुझे
जब लोग कहते हैं
कर्म कर, फल की चिन्ता मत कर।
बहुत आनन्द आता है मुझे
जब लोग कहते हैं
यह तो मेरे परिश्रम का फल है।
बहुत आनन्द आता है मुझे
जब लोग कर्मों का हिसाब करते हैं
और कहते हैं कि मुझे
कर्मानुसार मान नहीं मिला।
कहते हैं यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई।
कर्मों का लेखा-जोखा
अच्छा-बुरा सब लिखकर भेजा है।
.
आपको नहीं लगता
हम अपनी ही बात में बात
बात में बात कर-करके
और अपनी ही बात
काट-काटकर
अकारण ही
परेशान होते रहते हैं।
-
लेकिन मुझे
बहुत आनन्द आता है।
चतुर सुजान
चतुर सुजान पिछले युग के
सुजान
कहीं पीछे छूटे
चतुर-चतुर यहां बचे
मेरी वीणा के तारों में ऐसी झंकार
काल की रेखाओं में
सुप्त होकर रह गये थे
मेरे मन के भाव।
दूरियों ने
मन रिक्त कर दिया था
सिक्त कर दिया था
आहत भावनाओं ने।
बसन्त की गुलाबी हवाएँ
उन्मादित नहीं करतीं थीं
न सावन की घटाएँ
पुकारती थीं
न सुनाती थीं प्रेम कथाएँ।
कोई भाव
नहीं आता था मन में
मधुर-मधुर रिमझिम से।
अपने एकान्त में
नहीं सुनना चाहती थी मैं
कोई भी पुकार।
.
किन्तु अनायास
मन में कुछ राग बजे
आँखों में झिलमिल भाव खिले
हुई अंगुलियों में सरसराहट
हृदय प्रकम्पित हुआ,
सुर-साज सजे।
तो क्या
वह लौट आया मेरे जीवन में
जिसे भूल चुकी थी मैं
और कौन देता
मेरी वीणा के तारों में
ऐसी झंकार।
जरा सी रोशनी के लिए
जरा सी रोशनी के लिए
सूरज धरा पर उतारने में लगे हैं
जरा सी रोशनी के लिए
दीप से घर जलाने में लगे हैं
ज़रा-सी रोशनी के लिए
हाथ पर लौ रखकर घुमाने में लगे हैं
ज़रा-सी रोशनी के लिए
चांद-तारों को बहकाने में लगे हैं
ज़रा-सी रोशनी के लिए
आज की नहीं
कल की बात करने में लगे हैं
ज़रा -सी रोशनी के लिए
यूं ही शोर मचाने में लगे हैं।
.
यार ! छोड़ न !!
ट्यूब लाईट जला ले,
या फिर
सी एफ़ एल लगवा ले।।।
पावस की पहली बूंद
पावस की पहली बूंद
धरा तक पहुंचते-पहुंचते ही
सूख जाती है।
तपती धरा
और तपती हवाएं
नमी सोख ले जाती हैं।
अब पावस की पहली बूंद
कहां नम करती है मन।
कहां उमड़ती हैं
मन में प्रेम-प्यार,
मनुहार की बातें।
समाचार डराते हैं,
पावस की पहली बूंद
आने से पहले ही
चेतावनियां जारी करते हैं।
सम्हल कर रहना,
सामान बांधकर रख लो,
राशन समेट लो।
कभी भी उड़ा ले जायेंगी हवाएँ।
अब पावस की बूंद,
बूंद नहीं आती,
महावृष्टि बनकर आती है।
कहीं बिजली गिरी
कहीं जल-प्लावन।
क्या जायेगा
क्या रह जायेगा
बस इसी सोच में
रह जाते हैं हम।
क्या उजड़ा, क्या बह गया
क्या बचा
बस यही देखते रह जाते हैं हम
और अगली पावस की प्रतीक्षा
करते हैं हम
इस बार देखें क्या होगा!!!
मुस्कान सरस सी
हाईकू
देखा तुमने
मुस्कान सरस सी
जीवन रेखा
हे विधाता ! किस नाम से पुकारूं तुम्हें
शायद तुम्हें अच्छा न लगे सुनकर,
किन्तु, आज
तुम्हारे नामों से डरने लगी हूं।
हे विधाता !
कहते हैं, यथानाम तथा गुण।
कितनी देर से
निर्णय नहीं कर पा रही हूं
किस नाम से पुकारूं तुम्हें।
जितने नाम, उतने ही काम।
और मेरे काम के लिए
तुम्हारा कौन-सा नाम
मेरे काम आयेगा,
समझ नहीं पा रही हूं।
तुम सृष्टि के रचयिता,
स्वयंभू,
प्रकृति के नियामक
चतुरानन, पितामह, विधाता,
और न जाने कितने नाम।
और सुना है
तुम्हारे संगी-साथी भी बहुत हैं,
जो तुम्हारे साथ चलाते हैं,
अनगिनत शस्त्र-अस्त्रों से सुसज्जित।
हे विश्व-रचयिता !
क्या भूल गये
जब युग बदलते हैं,
तब विचार भी बदलते हैं,
सत्ता बदलती है,
संरचनाएं बदलती हैं।
तो
हे विश्व रचयिता!
सामयिक परिस्थितियों में
गुण कितने भी धारण कर लो
बस नाम एक कर लो।
अब तो कुछ बोलना सीख
आग दिल में जलाकर रख
अच्छे बुरे का भाव परख कर रख।
न सुन किसी की बात को
अपने मन से जाँच-परख कर रख।
कब समझ पायेंगें हम!!
किसी और के घर में लगी
आग की चिंगारी
जब हवा लेती है
तो हमारे घर भी जलाकर जाती है।
तब
दिलों के भाव जलते हैं
अपनों के अरमान झुलसते हैं
पहचान मिटती है,
जिन्दगियां बिखरती हैं
धरा बिलखती है।
गगन सवाल पूछता है।
इसीलिए कहती हूँ
न मौन रह
अब तो कुछ बोलना सीख।
अपने हाथ आग में डालना सीख
आग परख। हाथ जला।
कुछ साहस कर, अपने मन से चल।
आप चलेंगे साथ मेरे
हम जानते हैं न
कि रक्त लाल होता है
गाढ़ा लाल।
पर पता नहीं क्यों
इधर लोग
बहुत बात करने लगे हैं
कि फ़लां का खून तो
सफ़ेद हो गया।
और यह भी कि
किसी का खून तो
अब बस ठण्डा ही हो गया है
कुछ भी हो जाये
उबाल ही नहीं आता।
मुझे और किसी के
खून से क्या लेना-देना
अपने ही खून की
जाँच करवाने जा रही हूँ
अभी लाल ही है
या सफ़ेद हो गया
ठण्डा है
या आता है
इसमें भी कभी उबाल।
आप चलेंगे साथ मेरे
जाँच के लिए ?
माँ का प्यार
माँ का अँक
एक सुरक्षा-कवच
कभी न छूटे
कभी न टूटे
न हो विलग।
माँ के प्राण
किसी तोते समान
बसते हैं
अपने शिशु में
कभी न हों विलग।
जीवन की आस
बस तेरे साथ
जीवन यूँ ही बीते
तेरी साँस मेरी आस।
मेरा क्रोध
मेरा क्रोध
एक सरल सहज अनुभूति है
मान क्यों नहीं लेते तुम
मेरी पुस्तकों की कीमत
दीपावली, होली पर
खुलती है अब
पुस्तकों की आलमारी।
झाड़-पोंछ,
उलट-पलटकर
फिर सजा देती हूँ
पुस्तकों को
डैकोरेशन पीस की तरह ।
बस, इतने से ही
बहुत प्रसन्न हो लेती हूँ
कि मेरी
पुस्तकों की कीमत
कई सौ गुणा बढ़ गई है
दस की सौ हो गई है।
सोचती हूँ
ऐमाज़ान पर डाल दूँ।
मज़दूर दिवस मनाओ
तुम मेरे लिए
मज़दूर दिवस मनाओ
कुछ पन्ने छपवाओ
दीवारों पर लगवाओ
सभाओं का आयोजन करवाओ
मेरी निर्धनता, कर्मठता
पर बातें बनाओ।
मेरे बच्चों की
बाल-मज़दूरी के विरुद्ध
आवाज़ उठाओ।
उनकी शिक्षा पर चर्चा करवाओ।
अपराधियों की भांति
एक पंक्ति में खड़ाकर
कपड़े, रोटी और ढेर सारे
अपराध-बोध बंटवाओ।
एक दिन
बस एक दिन बच्चों को
केक, टाफ़ी, बिस्कुट खिलाओ।
.
कभी समय मिले
तो मेरी मेहनत की कीमत लगाओ
मेरे बनाये महलों के नीचे
दबी मेरी झोंपड़ी
की पन्नी हटवाओ।
मेरी हँसी और खुशी
की कीमत में कभी
अपने महलों की खुशी तुलवाओ।
अतिक्रमण के नाम पर
मेरी उजड़ी झोंपड़ी से
कभी अपने महल की सीमाएँ नपवाओ।
जल लेने जाते कुएँ-ताल
बाईसवीं सदी के
मुहाने पर खड़े हम,
चाँद पर जल ढूँढ लाये
पर इस धरा पर
अभी भी
कुएँ, बावड़ियों की बात
बड़े गुरूर से करते हैं
कितना सरल लगता है
कह देना
चली गोरी
ले गागर नीर भरन को।
रसपान करते हैं
महिलाओं के सौन्दर्य का
उनकी कमनीय चाल का
घट भरकर लातीं
प्रेमरस में भिगोती
सखियों संग मदमाती
कहीं पिया की आस
कहीं राधा की प्यास।
नहीं दिखती हमें
आकाश से बरसती आग
बीहड़ वन-कानन
समस्याओं का जंजाल
कभी पुरुषों को नहीं देखा
सुबह-दोपहर-शाम
जल लेने जाते कुएँ-ताल।
कोई तो आयेगा
भावनाओं का वेग
किसी त्वरित नदी की तरह
अविरल गति से
सीमाओं को तोड़ता
तीर से टकराता
कंकड़-पत्थर से जूझता
इक आस में
कोई तो आयेगा
थाम लेगा गति
सहज-सहज।
.
जीवन बीता जाता है
इसी प्रतीक्षा में
और कितनी प्रतीक्षा
और कितना धैर्य !!!!
आवाज़ ऊँची कर
आवाज़ ऊँची कर
चिल्ला मत।
बात साफ़ कर
शोर मचा मत।
अपनी बात कह
दूसरे की दबा मत।
कौन है गूँगा
कौन है बहरा
मुझे सुना मत।
सबकी आवाज़ें
जब साथ बोलेंगीं
तब कान फ़टेंगें
मुझे बता मत।
धरा की बातें
अकारण
आकाश पर उड़ा मत।
जीने का अंदाज़ बदल
बेवजह अकड़
दिखा मत।
मिलजुलकर बात करें
तू बीच में
अपनी टाँग अड़ा मत।
मिल-बैठकर खाते हैं
गाते हैं
ढोल बजाते हैं
तू अब नखरे दिखा मत।
तिरंगे का एहसास
जब हम दोनों
साथ खड़े होते हैं
तब
तिरंगे का
एहसास होता है।
केसरिया
सफ़ेद और हरा
मानों
साथ-साथ चलते हैं
बाहों में बाहें डाले।
चलो, यूँ ही
आगे बढ़ते हैं
अपने इस मैत्री-भाव को
अमर करते हैं।
शब्दों के घाव
दिल के
कुछ ज़ख्मों का दर्द
मानों दर्द नहीं होता,
स्मृतियों का
खजाना होता है,
उनकी टीस
आनन्द देती है
कुछ यादें
कुछ वफ़ाएँ
कुछ बेवफ़ाएँ
शब्दों के घाव
रिसते रहते हैं
चुभते हैं
पर भरने का
मन नहीं करता
आँखें बन्द कर
कुरेदने में मज़ा आता है
और जब आँख का पानी
रिसता है
उन जख़्मों पर,
तब टीस
और गहरी होती है
और आनन्द और ज़्यादा।
भीतर के भाव
हर पुस्तक के
आरम्भ और अन्त में
कुछ पृष्ठ
कोरे चिपका दिये जाते हैं
शायद
पुस्तकों को सहेजने के लिए।
किन्तु हम
बस पन्नों को ही
सहेजते रह जाते हैं
पुस्तकों के भीतर के भाव
कहाँ सहेज पाते हैं।
जीवन की आपा-धापी में
सालों बाद, बस यूँ ही
पुस्तकों की आलमारी
खोल बैठी।
पन्ना-पन्ना मेरे हाथ आया,
घबराकर मैंने हाथ बढ़ाया,
बहुत प्रयास किया मैंने
पर बिखरे पन्नों को
नहीं समेट पाई,
देखा,
पुस्तकों के नाम बदल गये
आकार बदल गये
भाव बदल गये।
जीवन की आपा-धापी में
संवाद बदल गये।
प्रारम्भ और अन्त
उलझ गये।
इन्द्रधनुष-सी ज़िन्दगी
प्रतिदिन निरखती हूँ
आकाश को
भावों से सराबोर
कभी मुस्कुराता
कभी खिल-खिल हँसता
कभी रूठता-मनाता
सूरज, चंदा, तारों संग खेलता
कभी मुट्ठी में बाँधता कभी छोड़ता।
बादलों को अपने ऊपर ओढ़ता
फिर बादलों की ओट से
झाँक-झाँक देखता।
.
आकाश में बिखरे रंगों से
कभी मुलाकात की है आपने?
मेरे मन में अक्सर उतर आते हैं।
गिन नहीं पाती, परख नहीं पाती
बस हाथों में लिए
निरखती रह जाती हूँ।
आकाश से धरा तक बरसते
चाँद-तारों संग गीत गाते
बादलों में उलझते
दिन-रात, सांझ-सवेरे
नवीन आकारों में ढलते
पल-पल, हर पल रूप बदलते
वर्षा की रिमझिम बूँदों से झांकते।
पत्तों पर लहराती
ओस की बूँदों के भीतर
छुपन-छुपाई खेलते।
.
और फिर
सूरज की किरणों से झांकती
रिमझिम बारिश के बीच से
रंगों के बनते हैं भंवर
जिनमें डूबता-उतरता है मन
आकाश में लहराते हैं
लहरिए सात रँग।
.
इन रँगों को अपनी आँखों से
मन के भीतर तक ले जाती हूँ
और इस तरह
इन्द्रधनुष-सी रंगीन
हो जाती है ज़िन्दगी।
कड़वा सच
हिम्मत से मेरे घर आना
चाय-पानी भूलकर
कड़वा सच पिलवाऊँगी
कवियों की पंगत लगी
कवियों की पंगत लगी, बैठे करें विचार
तू मेरी वाह कर, मैं तेरी, ऐसे करें प्रचार
भीड़ मैं कर लूंगा, तू अनुदान जुटा प्यारे
रचना कैसी भी हो, सब चलती है यार
सुन्दर इंद्रधनुष लाये बादल
शरारती से न जाने कहां -कहां जायें पगलाये बादल
कही धूप, कहीं छांव कहीं यूं ही समय बितायें बादल
कभी-कभी बड़ी अकड़ दिखाते, यहां-वहां छुप जाते
डांट पड़ी तब जलधार संग सुन्दर इंद्रधनुष लाये बादल
अपने कर्मों पर रख पकड़
चाहे न याद कर किसी को
पर अपने कर्मों से डर
न कर पूजा किसी की
पर अपने कर्मों पर रख पकड़ ।
न आराधना के गीत गा किसी के
बस मन में शुद्ध भाव ला ।
हाथ जोड़ प्रणाम कर
सद्भाव दे,
मन में एक विश्वास
और आस दे।