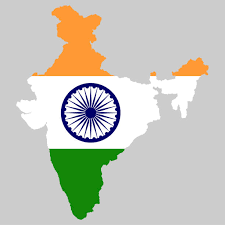अंगदान के लिए आमजन कैसे हो जागरूक
अभी तक लोग रक्तदान के लिए तो जागरूक नहीं हैं तो अंगदान के लिए कहाँ हो सकते हैं।
अँगदान के लिए आमजन को जागरूक करने के दो ही तरीके हैं। पहला अंधाधंुध प्रचार, जैसे कभी परिवार-नियोजन, पोलियो, बै्रस्ट कैंसर, एच. आई. वी. एड्स, काॅपर टी का किया जाता था। देश में हर जगह, हर कोने पर। किन्तु सकारात्मक, मनोवैज्ञानिक, सार्थक, बृहद् जानकारी युक्त एवं भावपूर्ण। केवल प्रेरणा से यह काम नहीं हो सकता। सोच में परिवर्तन लाना होगा।
दूसरा प्रयास जो इससे पहले आवश्यक है वह है क्या हमारा चिकित्सा-तंत्र इतना व्यवस्थित, जागरूक एवं आमजन के लिए उपलब्ध है कि यदि मैं अंगदान अथवा देहदान करना चाहूँ तो वह मेरी सहायता करेगा? क्या देश के किसी भी अस्पताल में किसी भी चिकित्सक से इससे सम्बन्धित जानकारी मिल जायेगी? जी नहीं।
यदि मुझे अंगदान अथवा देहदान करना है तो कहाँ जाना होगा, कौन-सा अस्पताल, कौन-सी संस्था? क्या संस्थाएं पंजीकृत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जनहित में दान करुं और उसका व्यापार हो। देश के कितने चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध है? हम किसी एन. जी. ओ. पर कैसे भरोसा करें। कौन-सा फ़ार्म भरा जायेगा? यदि किसी अनजान स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाती है तो कौन उत्तरदायित्व लेगा कि मेरे अंग ले लिए जायें। गूगल पर मुझे केवल 228 अस्पतालों की सूची मिली जो देहदान लेते हैं, 137 करोड़ जनसंख्या के लिए। यह हास्यास्पद है। छोटी-से-छोटी चिकित्सा के हम निजी अस्पतालों के पीछे भाग रहे हैं। सरकारी तंत्र पर हमें विश्वास नहीं है। निजी अस्पताल हमें लूटते दिखते हैं।
अतः पहले संसाधन विकसित कीजिए, चिकित्सा-तंत्र का विकास कीजिए, सुविधाएं उपलब्ध करवाईये, विश्वास बनाईये, उपरान्त जागरूकता अभियान चलाईये, फिर आशा कीजिए।
महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रश्न
यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए नियुक्त उच्च अधिकारी ही किसी संदेहास्पद स्थितियों में मारे जायें तो इससे बढ़कर किसी देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यह सम्पूर्ण देश के लिए चिन्ता का विषय है।
आज हमारे देश में सुरक्षा लेना एवं सुरक्षाकर्मी लेकर चलना एक स्टेटस सिम्बल बन गया है। छोटे-से-छोटे पदाधिकारी के साथ भी आप बन्दूकधारी देख सकते हैं। इस दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था एक उपहास बनकर रह गई है। एक हीरोईन को 21 कमांडोज़ की सुरक्षा दे दी जाती है और उसका मीडिया धारावाहिक प्रसारण करता है। कितना हास्यास्पद प्रतीत होता है यह सब।
इस रूप में सुरक्षा किसे दी जाये, किस स्तर की दी जाये और कब तक दी जाये, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।
फुलप्रूफ़ सुरक्षा व्यव्स्था के मेरी दृष्टि में तीन ही उपाय हैं: पहला गुप्तचर संस्थाओं को अत्याधिक आधुनिक, मज़बूत एवं व्यवस्थित करना। देश में अनेक सुरक्षा ऐजंसियाँ हैं, सबके बीच तालमेल की आवश्यकता एवं निजी सुरक्षा ऐजंसियों को भी खड़ा करना। दूसरा किसी भी अपराधी को तत्काल दण्डित करना, जो कि हमारे देश में अत्यन्त धीमी गति से चलता है।
और अन्तिम व सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा किसे प्रदान की जाये, किस स्तर की और कब तक।
लड़कियों के विवाह की आयु सम्बन्धी कानून
अभी-अभी लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने का कानून पारित हुआ। क्या इससे लड़कियों के जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? क्या हर परिवार सरकार की बात मानकर 21 वर्ष से पूर्व अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगा?
भारत में बाल विवाह अधिनियम 1929 में बना था, जो 1947 में संशोधित हुआ। 1949 में लड़कियों की विवाह की आयु 15 वर्ष और पुनः 1978 में 18 वर्ष नियत की गई। इस तरह के कानून केवल पुस्तकों में रह जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं किन्तु गहराई से लागू नहीं होते। तो इस अधिनियम को लागू कैसे करवाया जाये, इस पर भी क्या विचार हो रहा है, शायद नहीं।
देश में क्या कोई ऐसी संस्थाएँ हैं जो 137 करोड़ जनसंख्या वाले देश में होने वाले प्रत्येक विवाह की जांच कर सके? नहीं। मात्र विवाह की आयु बढ़ाने से महिलाओं के जीवन में कोई अन्तर नहीं आने वाला,
क्या हम जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में लड़के-लड़कियों का औसत प्रायः 55-45 होता है जो महाविद्यालय में आकर 40-60 अथवा 30-70 हो जाता है और उच्च शिक्षा में शायद 10-90। यह विकसित शहरों की स्थिति है जहाँ विवाह देर से ही होते हैं।
इतने वर्ष बीत जाने पर अभी तक बाल-विवाह पर रोक नहीं लगाई जा सकी है तो मात्र कानूनन आयु बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। देश में आज भी कितने विवाह पंजीकृत होते हैं?
विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने पर भी आज भी केवल शहरों में ही किसी सीमा तक विवाह पंजीकृत करवाये जाते हैं जहाँ आयु सीमा की जांच हो सकती है किन्तु विवाहोपरान्त ही पंजीकरण करवाया जाता है, पहले नहीं। अर्थात् यदि कहीं किसी ने कम आयु में विवाह किया तो वे पंजीकरण करवायेंगे ही नहीं। तो यह अधिनियम इतने बड़े देश में कार्यान्वित कैसे होगा? हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिदिन औसतन 30,000 विवाह होते हैं। बेघरबार, बंजारों आदि की गणना इनमें नहीं है। मात्र विवाह की आयु बढ़ाने से महिलाओं के जीवन में कोई अन्तर नहीं आ सकता। हाँ, शहरों में जहाँ शिक्षा के अवसर हैं, वहाँ लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और उनके विवाह की आयु भी अधिक है। कानून क्या कहता है, इस पर कोई विचार नहीं करता। किन्तु यह बात पूरे देश पर लागू नहीं होती।
और यदि लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त भी कर लेती हैं तो वे उसका कितना लाभ उठाती हैं यह भी हम जानते हैं।
इतने वर्ष बीत जाने पर अभी तक बाल.विवाह पर रोक नहीं लग पाई है तो मात्र कानूनन आयु बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। देश में आज भी कितने विवाह पंजीकृत होते हैं?
लड़कियों को कुपोषण से बचाने, पढ़ाई व स्वाबलम्बन के उचित अवसर देने हेतु मात्र विवाह कानून में संशोधन से कोई लाभ नहीं होने वालाए जब तक कि हमारी सोच नहीं बदलती, शिक्षा, स्वाबलम्बन के प्रति दिशाएं सकारात्मक नहीं होतीं। इस परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं हम स्वयं आगे बढ़ें, अपने आस-पास के लोगों को जाग्रत करें और इन कानूनों के प्रचार-प्रसार में सहयोग दें।
यह हास्यास्पद है कि बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक संसदीय समिति के 31 सदस्यों में केवल एक महिला है।
इंसान के भीतर वृक्ष भाव
एक वृक्ष को बनने में कुछ वर्ष नहीं, दशाब्दियाँ लग जाती हैं। प्रत्येक मौसम झेलता है वह।
प्रकृति स्वयं ही उसे उसकी आवश्यकताएँ पूरी करने देती है यदि मानव उसमें व्यवधान न डाले। अपने मूल रूप में वृक्ष की कोमल-कांत छवि आकर्षित करती है। हरी-भरी लहलहाती डालियाँ मन आकर्षित करती है। रंग-बिरंगे फूल मन मोहते हैं। धरा से उपज कर धीरे-धीरे कोमल से कठोर होने लगता है। जैसे-जैसे उसकी कठोरता बढ़ती है उसकी उपयोगिता भी बढ़ने लगती है। छाया, आक्सीजन, फल-फूल, लकड़ी, पर्यावरण की रक्षा, सब प्राप्त होता है एक वृक्ष से। किन्तु वृक्ष जितना ही उपयोगी होता जाता है बाहर से उतना ही कठोर भी।
किन्तु क्या वह सच में ही कठोर होता है ? नहीं ! उसके भीतर एक तरलता रहती है जिसे वह अपनी कठोरता के माध्यम से हमें देता है। वही तरलता हमें उपयोगी वस्तुएँ प्रदान करती है। और ठोस पदार्थों के अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा देते हैं यह कठोर वृक्ष जो हमें न तो दिखाई देता है और न ही समझ है बस हमें वरदान मिलता है। यदि इस बात को हम भली-भांति समझ लें तो वृक्ष की भांति हमारा जीवन भी हो सकता है।
और यही मानव जीवन कहानी है।
हर मनुष्य के भीतर कटुता और कठोरता भी है और तरलता एवं कोमलता अर्थात भाव भी। यह हमारी समझ है कि हम किसे कितना समझ पाते हैं और कितनी प्राप्तियाँ हो पाती हैं।
मानव अपने जीवन में विविध मधुर-कटु अनुभवों से गुज़रता है। सामाजिक जीवन में उलझा कभी विनम्र तो कभी कटु हो जाता है उसका स्वभाव। जीवन के कटु-मधुर अनुभव मानव को बाहर से कठोर बना देते है। किन्तु उसके मन की तरलता कभी भी समाप्त नहीं होती, चाहे हम अनुभव कर पायें अथवा नहीं। जिस प्रकार वृक्ष की छाल उतारे बिना उसके भीतर की तरलता का अनुभव नहीं होता वैसे ही मानव के भीतर भी सभी भाव हैं, कोई भी केवल अच्छा या बुरा, कटु अथवा मधुर नहीं होता। बस परख की बात है।
गलती से मिस्टेक हो गई
जब फ़ेसबुक पर नया-नया खाता खोला तब बड़ा शौक था तरह तरह की फ़ोटो पोस्ट करने का। गूगल से उठाये गये सूक्ति वाक्य, कोई चित्र आदि। बड़ा आनन्द आता था। जब भी कोई मैत्री संदेश मिलता, मन यूं खिल उठता जैसे पता नहीं कौन-सी निधि मिल गई। निधि की वास्तविकता का तो तब पता लगता जब महोदय अथवा महोदया संदेश बाक्स में आकर अपने मन की बातें कहने लगते और हम ब्लाॅक की ओर भागते। किन्तु एक बार की लत कहां छूटती है। लग गई तो लग गई।
फिर मिले कुछ साहित्यिक मंच। और हम लगे कविताएं लिखने। यहां तक तो ठीक था किन्तु जब कविताएं लिख रहे हैं तो सराहनात्मक प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं और हम भी औरों की रचनाओं पर प्रतिक्रियाएं लिखने लगे।
आप कहेंगे इसमें नया क्या, सबके साथ ही ऐसा ही तो हुआ होगा।
किन्तु हमारे साथ कुछ अलग और नया हुआ।
हमें अपने हिन्दी टंकण बड़ा गुरूर था। 1970 से रैमिंगटन टाईपराईटर पर सीखी हिन्दी टाईपिंग अब तक जीवन्त थी अंगुलियों में, और कम्प्यूटर के अंग्रेज़ी के की बोर्ड पर आराम से हिन्दी टाईपिंग कर लेते थे।
किन्तु हुआ यूं कि हमारे हिन्दी फॅ़ांट ने हमें दे दिया धोखा। सीधे टंकण हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम आ गये काॅपी-पेस्ट पर। अब काॅपी-पेस्ट तो आप सब जानते ही हैं। इधर से उठाया, उधर लगा दिया, उधर से उठाया इधर लगा दिया। वल्र्ड की फ़ाईल में लिखा, कन्वर्टर में पेस्ट किया, और फिर उठा कर फ़ेसबुक पर पेस्ट। किन्तु पेस्ट करते समय बहुत बार धोखा भी होता है और देखिए ऐसे ही धोखे जो मेरे साथ हुए।
बस, यहीं हम उलझे।
मैंने लिखा ‘‘मेरी रचना की आत्मीय सराहना के लिए आपका आभार। ’’
किन्तु काॅपी-पेस्ट में रह गया ‘‘मरी रचना के लिए’’
एक बार लिखा ‘‘रचना पर आपकी प्रतिक्रिया’’
बाद में देखा तो पेस्ट था ‘‘ चना पर आपकी प्रतिक्रिया’’
एक बार प्रतिक्रिया की ‘‘ आपकी रचना से मन आनन्दित हुआ’’
और काॅपी -पेस्ट हो गया ‘‘ पकी रचना से मन आनन्दित हुआ ’’
लिखा मैंने ‘‘ आभार , नमन’’, पेस्ट हुआ: ‘‘ भार, नमन’’
मैंने लिखा ‘‘ आपका हार्दिक आभार’’ पेस्ट हुआ ‘‘ पका हार्दिक आभार’’
स्वभाव में तो हडबडी है एक बार लिखना था Hello Sir लिख दिया Hell Sir
यदि कभी आप सभी मित्रों को मेरी ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलें तो कृपया पहला अक्षर जोड़ लीजिएगा।
अंगूठा-छाप
एक समय की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे। उस समय अशिक्षित का यह कह कर उपहास किया जाता था कि रहा तू अंगूठा-छाप का अंगूठा-छाप ही। जो बच्चे अच्छे-से पढ़ते नहीं थे उन्हें भी यह कर डराया जाता था कि पढ़-लिख ले, नहीं तो फ़लां की तरह अंगूठा-छाप ही रह जायेगा, फिर ढोना खेतों में मिट्टी और करना खेतों में मज़दूरी। इन अंगूठा-छापों के लिए एक नीले रंग की रंगीन टीन की छोटी-सी डिब्बी-सी रखी रहती थी जिस पर अंगूठा लगवाने वाला अंगूठा ठोक कर उठवाता था और किसी भी कागज़ पर लगवा लेता था। अंगूठा-छाप होना बड़ा अपमानजनक माना जाता था।
किन्तु यह उस समय की बात है जब लोग अंगूठे का महत्व नहीं समझते थे। जब से आधार कार्ड आया, हमें भी अंगूठे का महत्व समझ आया। आज आधार-कार्ड का अंगूठा ही आपकी पहचान है। अब याद कीजिए आपने आधार कार्ड बनाने वाले को कौन-सा अंगूठा दिखाया था।
आप जानना चाहेंगे मुझे आज अंगूठे की याद क्यों आई और कहां से चलकर आई। यह तो आप जानते ही हैं कि एक विद्यालय में कार्यरत हूं। विद्यालयों में विभिन्न परीक्षाओं के केन्द्र संचालित होते हैं। यहां पिछले सप्ताह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अन्तर्गत ग्रुप डी के कर्मचारियों के चयन हेतु परीक्षा केन्द्र स्थापित था। अब आप सोच रहे होंगे यह ग्रुप डी क्या है, अंग्रेज़ी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट लगती है किन्तु हिन्दी में इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं।
अन्य विवरणों के अतिरिक्त इस पद हेतु भरे जाने वाले फ़ार्म में आवेदक का अंगूठा चाहिए] यहां भी भेद-भाव की नीति रही। लड़कियों का दायां और लड़कों का बायां। किन्तु चाहिए वही जो आधार कार्ड पर है नहीं तो दो सौ रूपये गये पानी में । हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बहुत खुले दिल का है। आयु सीमा कर दी 25&42 और $ 5 वर्ष। इससे भी अधिक कि इस बहाने आप हरियाणा घूम सकें अधिकांश आवेदकों का परीक्षा केन्द्र उनके अपने शहर का नहीं बनाया गया, इस प्रकार उन्होंने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया।
अब आईये परीक्षा केन्द्र के द्वार पर चलते हैं। बड़े-बड़े बैग उठाये अम्यर्थी पंक्तियों में लगे हैं। किन्तु परीक्षा केन्द्र के भीतर घड़ी, मोबाईल तो क्या गले, कान, नाक में भी कुछ नहीं ले जा सकते। पैन भी हम ही देंगे, बस आप परीक्षा दीजिए। साढ़े दस बजे परीक्षा के लिए साढ़े आठ बजे आपको अपने सम्पूर्ण चैकअप के लिए उपस्थित होना होगा। सबसे पहले आपके अंगूठे-छाप वाले प्रवेश-पत्र का निरीक्षण और उसके बाद निकालिए अपना अंगूठा। भौंचक से हरियाणे के छोरे-छोरे छोरियां देख रहे उस रंगीन-सी रोशन हरी डब्बी को, जिसमें बाउ ने कहा अंगूठा दिखा। अब छोरे-छोरियां तो उस डब्बी को देखें जायें। छोरे ने दायां हाथ आगे बढ़ाया, बाउ बोलया, अरे दायां नहीं उल्टा अंगूठा जो आधार कार्ड पर लगाया था, छोरे ने बाउ की शकल देखी और अंगूठा उल्टा कर दिया, नाखून वाला हिस्सा नीचे और बाकी हाथ उपर। सिर पर हाथ मारयो, चलो जैसे तैसे वहां तीन-तीन बार अंगूठे लेकर पहुंच गये अपणी -अपणी सीटां ते।
अब आगे की कहाणी सुनो।
पेपर ऐसे सील बन्द कि रिजर्व बैंक के नोट भी न रखे जाते होंगे। कई तहों के बीच से निकले परीक्षा पत्र अन्ततः अभ्यथिर्यों के सामने रख दिये गये। अब फिर निकालो अपना वही अंगूठा। एक-दो नहीं पांच बार और लगवाया अंगूठा, तब जाकर चैन पड़ा।
अब आई परीक्षा देने की बारी। किसी-किसी ने तो वो दानेदान पेपर देखया ही पहली बार। देखें जाये उसे उलट-पलट कर। कोई बात नहीं उनको भी रास्ता दिखा दियो।
आपको स्मरण होगा कि मैंने बताया था कि परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है। चलिए आप सबके लिए प्रश्न-पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संक्षेप में अवलोकन करते हैं -
----बाईक पर थियेटर योजना किसने शुरू की।
-उच्च क्रियाशील धातु कौन-सी है- सीसा, लोहा, तांबा, जस्ता
-नाभिकीय खनिज और नाभिकीय उर्जा संयत्र
-लाला लाजपतराय, होम रूल आंदोलन हषवर्धन, दोड्डबेट्टा, बू अली शाह कलंदर आदि पर प्रश्न।
---चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाईन किसने बनाया।
---जूही चावला हरियाणा के किस ज़िले की है।
--इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन- सा वायसराय जुड़ा था।
--बहू शब्द का बहुवचन रूप क्या है।
उच्च क्रियाशील धातु कौन-सी है- सीसा, लोहा, तांबा, जस्ता
-नाभिकीय खनिज और नाभिकीय उर्जा संयत्र
-लाला लाजपतराय, होम रूल आंदोलन, हषवर्धन, दोड्डबेट्टा, बू अली शाह कलंदर आदि पर प्रश्न।
-चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाईन किसने बनाया।
-जूही चावला हरियाणा के किस ज़िले की है।
इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन- सा वायसराय जुड़ा था।
एक बहुत पुराना हास-परिहास है। एक डाकिये का साक्षात्कार चल रहा था। डाकिये से पूछा गया कि बताओ धरती से सूरज की दूरी कितनी है। प्रत्याशी बोला , महोदय यदि डाक इस रूट पर बांटनी है तो मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए।
नौकरियों का झूठा झांसा देकर क्यों बरबाद किया जा रहा है इस पीढ़ी को।
न घटना न दुर्घटना
लगभग 15-16 वर्ष औटो में खूब धक्के खाये हैं। 1992 में किराया मात्र दो-तीन रूपये होता था और आज इतने वर्षों बाद दस रूपये। मात्र तीन गुणा, जबकि सरकारी बसों के किराया जो उस समय दस रूपये था आज एक सौ रूपये है फिर भी हम कहते हैं औटो वाले हमें लूटते हैं। आज भी अधिकांश सवारियां मोल-भाव करती हैं। तरह-तरह के अनुभव रहे। सबसे सुविधाजनक यह रहता है कि औटो से कहीं भी उतर जाओ और कहीं भी हाथ हिलाकर रोक लो। कोई नियम नहीं, कोई रोक नहीं। अपनी सुविधानुसार हम औटो वाले से जहां-तहां रूकवा लेंगे, भरे औटो में भी जगह बनाकर सरक-सरक कर बैठ जायेंगे और फिर औटो वाले को भला-बुरा कहेंगे कि लालच करते हैं नियमों का पालन नहीं करते।
औटो वालों से अधिक मुझे औटो में यात्रा करने वाली सवारियों से शिकायत रहती थी। जहां उतरना है, वहां उतरकर पर्स निकालेंगे उसमें से दूसरा पर्स निकालेंगे, दो जेबों में हाथ डालकर पैसे ढूंढेगे और फिर पांच या दस रूपये देने के लिए सौ-पचास का नोट पकड़ा देंगे, फिर बहस करेंगे कि तुम पैसे खुले क्यों नहीं रखते, सवारियों को लूटना चाहते हो।
मुझे प्रतिदिन औटो लेना होता था, मैं घर से हाथ में खुले पैसे लेकर चलती थी और औटो के स्टाप पर रूकने से पहले ही पैसे दे देती थी। चाहे बस में यात्रा करूं या औटो में यह मेरा नियम था। इतने वर्षों तक औटो में एक ही राह पर जाने से कितने औटो वालों से तो मानों एक आत्मीय व्यवहार हो गया जोकि एक ही रूट पर चलते रहे मेरी तरह। हाल-चाल पूछना, परिवार की जानकारी, सुख-दुख की बातें, 15&20 मिनट की यात्रा में कई बातें हो जाती थीं।
बस एक ही बार कटु अनुभव हुआ। स्कूल में कोई कार्यक्रम होने के कारण अंधेरा घिरने के बाद मैंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से लगभग सात बजे एक औटो लिया जिसमें दो सवारियां पहले से बैठी थीं। मेरे हाथ में बड़ा-सा पर्स था। औटो वाला लड़का-सा था। जैसे ही मैंने औटो के पायदान पर एक पैर रखा, औटो वाले ने औटो चला दिया और मुख्य सड़क से हटकर सुनसान अंधेरे रास्ते, जो श्मशान घाट से होकर जाता था वहां डाल दिया। मैं आधी लटकी रह गई। लगभग चिल्लाने लगी, भैया औटो रोको, औटो रोको, वह फिर भी भगाता रहा। पहले बैठी सवारियां भी कुछ नहीं बोल रही थीं, पल-भर में ही दिमाग घूम गया कि लूट का मामला तो नहीं। मैंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और चालक की कालर खींचनी शुरू कर दी, कान-नाक जो हाथ आया, मारना शुरू कर दिया। और लगभग छलांग लगा दी। औटो रूका और मैंने लड़के को दो-चार थप्पड़ लगा दिये, रोने-सk लगा वह कि पीछे पुलिस वाले थे और उसने गलत जगह रोका था, उनके डर से भगा रहा था। मौका पाते ही औटो वाला भाग गया और मैं पीछे मुड़कर पुलिस वालों से बहस पड़ी कि वे गप्पें मार रहे थे और मेरी चीखें नहीं सुनीं। उन्होंने एक और औटो मेरे लिए कर दिया, मानों मुझसे पीछा छुड़ाया।
घर आकर अपने पति को किस्सा सुनाया, आदतन चुपचाप सुना और बस। किन्तु अगले दिन भी स्कूल से निकलने का वही समय था।
स्कूल से बाहर निकली तो पतिदेव स्कूटर लेकर खड़े थे मुझे लेने के लिए। मैं चकित आज यह कैसी अनहोनी।
बोले, मैंने सोचा कल की तरह किसी को मारपीट न आये, या थाने ही न चली जाये पुलिस वालों से लड़ने के लिए , मैं ही लेने आ जाता हूं। वाह ! आज तो अनहोनी हो गई। पहले जब मैं कहती थी मुझे लेने आ जाना, तो कहते थे आ जाना औटो लेकर, पैट्रोल भी तो उतने ही रूपये का लगेगा।
बालपन की स्मृतियाँ
५०-५५ वर्ष पुरानी स्म़ृतियां मानस-पटल पर उभर कर आ गईं।
उसे चोरी कहते ही नहीं जो पकड़ी जाये। हम तो इतने होशियार थे कि कभी चोरी पकड़ी ही नहीं गई।
सस्ते का युग था। बाज़ार से छोटा-मोटा सामान हम बहनें ही लाया करती थीं। एक से पांच रूपये तक में न जाने कितना सामान आ जाता था। दस-बीस पैसे तो अक्सर मैं छुपा ही लिया करती थी। अब छुपायें तो छुपायें कहां। प्रवेश द्वार के बाद बरामदा था और उसमें पुस्तकों की अलमारियां थीं, वहां मैंने एक पुस्तक उपर के खाने में निर्धारित कर ली थी जिसके उपर मैं वह पैसे रख देती थी, और स्कूल जाते समय चुपके निकाल लेती थी। आप सोचेंगे, उन पांच-दस पैसों का क्या करते होंगे, दस पैसे के बीस गोलगप्पे आते थे और पांच पैसे का चूरण, गोलियां, अथवा दो-तीन नाशपाती, खट्टा (गलगल) आदि।
स्कूल तो पैदल ही आते-जाते थे, एक घंटे का रास्ता था। अब घर से स्कूल तो कोई पहुंचने से रहा। वह युग पी.टी.एम. वाला युग भी नहीं था कि कोई सच-झूठ का पता लगा पाता। स्कूल से फूलों के पौधे बहुत चुराया करती थी। घर के बाहर बड़ा सा मैदान था, उसमें क्यारियां बनाकर लगाते थे। मां पूछती थी कहां से लाये, कह देते थे स्कूल से माली से ले लिए। और राह-भर में पेड़ों से तोड़-तोड़कर अलूचे, पलम, कैंथ खुरमानी तो बहुत खाये हैं, उस खट्टे-मीठे स्वाद का तो कहना ही क्या।
आज नहीं सोच पाते कि उस समय जो किया वह सही था अथवा गलत, किन्तु जो था यही सत्य था, आज प्रकट कर अच्छा लगा।
ग्रह तो ग्रह ही होते हैं
यह घटना वर्ष 2009 की है।
यह आलेख एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरे अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।
========================
ठीक-ठाक थे मेरे पति। वायु सेना में। मंगल, शनि, संक्रांति, श्राद्ध, नवरात्रि सब एक समान। न मंदिर, न पूजा-पाठ, न कोई पंडित-पुजारियों के चक्कर, मुझे और क्या चाहिए था। मैं तो वैसे ही जन्म से पूरी नास्तिक । मन निश्चिंत हुआ।
किन्तु समय बदलते या कहूं ग्रहों के बिगड़ते देर नहीं लगती। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। पन्द्रह वर्ष के कार्यकाल के बाद वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए और व्यवसाय में आ गये। अब जब वातावरण, पर्यावरण परिवर्तित हुआ तो कुछ और भी बदल जायेगा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। किन्तु ऐसा ही हुआ।
हादसा
समय ठीक नहीं है, तब चलता है। किन्तु कोई कहे ग्रह ठीक नहीं हैं, तब डर लगता है। ग्रह कैसे भी हों मुझे पंडित-पुजारी, ज्योतिषियों, पूजा-पाठ, मन्दिर, दान वगैरह की याद नहीं सताती। एक तो वैसे ही समस्याएं होती हैं, दूसरी ओर पंडित-ज्योतिषियों का परामर्श शुल्क, उनके अपने-अपने विभाग के भगवानों के लिए विशेष प्रावधान, उनके विभागीय उपायों की विशेष सामग्री, और न जाने क्या-क्या। इससे आगे इनकी सांठ-गांठ नग-मोती बेचने वालों के साथ भी रहती है। और जब इस तरह का सिलसिला एक बार चल निकलता है तो उसे रोकना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जब कोई कहता है कि आपके ग्रह आजकल ठीक नहीं हैं, कुछ उपाय कीजिए, तो मैं मुंह ढककर सो जाती हूं। (इसे बस एक मुहावरा ही मानकर चलिए)
किन्तु तात्कालिक चिन्ता का विषय यह था कि मेरे पति अनायास ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने लगे और मैं आतंकित। ग्रहों की चिन्ता में वे प्रायः पंडित-ज्योतिषियों के पास जाने लगे। अब जब घर में एक आतंकवादी हो तो प्रभावित और दण्डित तो सारा परिवार होगा ही। कुछ ऐसा ही हमारे परिवार में होने जा रहा था।
अब पति महोदय एक ज्योतिषि से ग्रहों की दुर्दशा के उपाय पूछकर आये। अधिकांश पूजा-पाठ, दान आदि तो उनके अपने कर्म-क्षेत्र में आये, कुछ पुत्र के हिस्से, किन्तु एक ऐसा कार्य था जिसके लिए पण्डित महोदय का सख्त निर्देश था कि यह कार्य पत्नी द्वारा करने पर ही सुफल मिलेगा।
अब परिवार की भलाई के लिए कभी न कभी और कहीं न कहीं तो परिवार-पति के समक्ष आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है, हमने भी कर दिया। उपाय था कुल 108 दिन तक प्रतिदिन बिना नागा सुन्दर काण्ड का पाठ। पाठ में आदरणीय पण्डित जी ने यह सुविधा दी थी कि चाहे दोहे-चौपाईयां पढे़ं अथवा हिन्दी अनुवाद, फल समान मात्रा में मिलेगा । किन्तु व्यवधान नहीं आना चाहिए, अथवा पुनः एक से गिनती करनी होगी।
अब मैं दुविधा-ग्रस्त थी। सुन्दरकाण्ड का ऐसा क्या प्रभाव है कि जो समस्याएं पिछले पच्चीस वर्षों में हमारे कठोर परिश्रम, कर्त्तव्य-निष्ठा, सत्य-कर्म और अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ उचित करने पर भी दूर नहीं हुईं, इस सुन्दर-काण्ड का 108 बार जाप करने पर दूर हो जायेंगी। किन्तु मुझे तर्क का अधिकार नहीं था अब। बस करना था। इस काण्ड का अध्ययन एम. ए. में अंकों के लिए किया था अब ग्रहों को ठीक करने के लिए करना होगा। तब दोहे, चौपाईयां , भाषा-शैली, अलंकार, आदि की ओर ही ध्यान जाता था, इसका एक रूप यह भी है, ज्ञात ही नहीं था। कोई तर्क-बुद्धि नहीं थी कि कथानक में क्यों, कैसे, किसलिए, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस अंक मिलें, इतनी-सी ही छोटी सोच थी। किन्तु अब जब बुद्धि आतंकवादी हो चुकी है तब कुछ भी पढ़ते समय साहित्यिक अथवा धार्मिक विचार उपजते ही नहीं, बम और बारूद ही दिखाई देने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
कोई बात नहीं, मैंने सोचा, 108 दिन तक सास-बहू के धारावाहिक नहीं देखेंगे, कर लेते हैं पाठ।
संक्षेप में मुझे जो कथा समझ आई वह इस प्रकार हैः
जब पहली बार सुन्दरकांड का पाठ आरम्भ किया तो ज्ञात हुआ कि तुलसीदास ने ‘काण्ड’ शब्द का प्रयोग बिल्कुल ठीक किया है। यह कांड हनुमान की लंका यात्रा की कथा पर आधारित है। हनुमान राम के दूत बनकर लंका की ओर सीता को ढूंढने के लिए निकले। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं किन्तु क्योंकि वे राम के दूत थे इसलिए सब बाधाओं से पार पा लिया। कभी चार सौ योजन के बन गये तो कभी मच्छर के समान। लंका में प्रवेश किया। विभीषण से मुलाकात हुई। सीता का एड्ेर्स लिया। सीता को राम के आई-डी प्रूफ़ के रूप में अंगूठी दी। बगीचा उजाड़ा। ब्रम्हास्त्र से बंधकर रावण के दरबार में पहुंचे। राम का गुणगान किया। रावण ने दंडस्वरूप उनकी पंूछ में घी, तेल और कपड़ा बंधवाकर आग लगवाई जिसमें लंका का संपूर्ण घी, तेल और कपड़ा समाप्त हो गया। ;पढ़ते-पढ़ते मेरा ध्यान भटक गया कि इसके बाद बेचारे लंकावासियों ने इन वस्तुओं को कैसे और कहां से प्राप्त किया होगा क्योंकि बीच में तो समुद्र था और आगे राम की सेना खड़ी थी, मैंने इस विषय को भविष्य में कभी शोध कार्य करने के लिए छोड़ दिया। विभीषण का घर छोड़कर हनुमान ने सम्पूर्ण लंका जला डाली। फिर समुद्र में पूंछ बुझाई, सीता से उनके आई डी प्रूफ के रूप में उनकी चूड़ामणि ली और राम के पास लौट आये।
कथा के दूसरे हिस्से में लंका में प्रवेश की योजनाएं, राम की सेना के बल और संख्या का वर्णन आदि, रावण के छद्म दूतों को पकड़ना, उनके हाथ लक्ष्मण द्वारा पत्र भेजना, रावण का उसे पढ़ना, समुद्र पर बांध की तैयारी आदि कथाएं हैं।
इन दो कथाओं के बीच एक तीसरी व मेरी दृष्टि में मुख्य कथा है जिससे मेैं विचलित हूं और जिसका समाधान ढूंढ रही हूं ओैर वह हैै: लंका का राजा कौन? मेरे प्रश्न करते ही तीनों लोकों, चारों दिशाओं से एक ही उत्तर आयाः ‘रावण’। मैंने पुनः पूछा, तो विभीषण कौन? तीनों लोकों और चारों दिशाओं से पुनः उत्तर आया, अरे, मूर्ख बालिके, इतना भी नहीं जानती ! विभीषण अर्थात ‘घर का भेदी लंका ढाए’। इतना सुनते ही मैं भगवान रामजी की आस्था के प्रति चिन्तित हो उठी।
विभीषण बड़े सदाचारी थे और सदैव राम का ही ध्यान करते थे। तुलसीदास ने लिखा है कि विभीषण ने रावण को समझाने का बड़ा प्रयास किया किन्तु उसके द्वारा अनादृत होने पर वे अपने साथियों के साथ लंका छोड़कर राम की शरण में आ गए। तुलसीदास ने लिखा है कि विभीषण हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ लेकर राम के पास चले। अब वे मनोरथ क्या थे तुलसी जानें या विभीषण स्वयं।
तुलसी ने बार-बार यह भी लिखा है कि राम सब की दीनता से बहुत प्रसन्न होते थे। वैसे ही राम विभीषण के दीन वचनों और दण्डवत् से बहुत प्रसन्न हुए। सो राम ने विभीषण को लंकापति और लंकेश कहकर संबोधित किया। अब दोनों एक-दूसरे का स्तुति गान करके परस्पर न्योछावर होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि राम ने समुद्र के जल द्वारा विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक किया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दस सिरों की बलि देने पर दी थी, राम ने वह सब सम्पत्ति विभीषण को दी। मेरे मन में आशंका यह कि राम ने रावण के जीवित रहते हुए किस अधिकार से विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और यह सम्पत्ति राम के पास कहां से और कैसे आई। क्योंकि राम तो अयोध्या से सर्वस्व त्याग कर आये थे, कंद-मूल खा रहे थे, कुशा पर सोते थे, वानरों के संग रहते थे, सीता को ढूंढने के लिए वन-वन की ठोकरें खा रहे थे, वानरों-भालुओं की सहायता ले रहे थे। फिर मान लीजिए उन्होंने दे भी दी तो विभीषण ने रखी कहां - इस बात की चर्चा इस ‘काण्ड’ में कहीं नहीं हैं। किन्तु मेरे मन में इससे भी बड़ी व्यथा उपजी है जो मुझे निरन्तर कचोट रही है, वह यह कि जिस विभीषण को भगवान श्रीरामजी ने लंका का राजा बनाया, उन्हें अखंड राज्य सौंपा, रामजी के इस प्रताप की चर्चा कभी भी कहीं भी नहीं होती। उसके बाद लंका पर विजय प्राप्त करके राम ने पुनः विभीषण को लंका का राजा बनाया, उसके बाद विभीषण का क्या हुआ किसी को भी पता नहीं। जो भी कहता है वह यही कहता है कि लंका का राजा रावण। और विभीषण घर का भेदी लंका ढाए। इस काण्ड के अध्ययन के उपरान्त मैं सबसे कहती हूं कि लंका का राजा विभीषण तो सब मेरा उपहास करते हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। किन्तु मुझे अपनी चिन्ता नहीं है। चिन्ता है तो रामजी की। उनकी ख्याति एवं प्रतिष्ठा की कि जिसे उन्होंने लंका का राजा बनाया उसका सब उपहास करते हैं और जिसका उन्होने वध किया उसे सब सोने की लंका का राजा कहते हैं । हे रामजी ! आपकी प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित करने के लिए मैं क्या करुं ? सोचती हूं एक सौ आठ बार सुन्दर कांड ही पढ़ डालूं। शायद इससे ही आपका कुछ भला हो जाए !और इसी कांड में ‘ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी’ पंक्तियां भी हैं इन्हें भी मैं 108 बार पढ़ूंगी। अभी तो पाठ करते मात्र 13 ही दिन बीते हैं। श्रीरामजी ही जानें कि मेरा क्या होगा ?
हमारी हिन्दी तुम्हारी हिन्दी
आज हम सब हिन्दी-हिन्दी की बात कर रहे हैं। किन्तु वास्तव में हिन्दी की स्थिति क्या है ?
आज हम कहने लगे हैं कि हिन्दी की स्थिति सुधरने लगी है। अधिकाधिक लोग आज हिन्दी में लिखने एवं बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हिन्दी छाई हुई है। संचार माध्यमों पर हिन्दी भाषा का साम्राज्य है। किन्तु क्या मात्र इतने से ही हिन्दी की स्थिति अच्छी मान लेनी चाहिए ?
मेरी दृष्टि में आज हिन्दी भाषा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। वास्तविकता यह कि हिन्दी की दुर्दशा के लिए हिन्दी भाषी ही उत्तरदायी हैं। हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य से सीधे जुड़े लोग ही हिन्दी की उपेक्षा कर रहे हैं। हम हर बात के लिए सरकार को दोष देते हैं। सरकारी स्तर पर हिन्दी विभाग, हिन्दी समितियां, संस्थान आदि बनाये गये हैं। यहां कार्यरत लोग हिन्दी के नाम से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किन्तु क्या कभी, हमने इन समितियों की कार्यविधि पर कोई आवाज उठाई है? ये समितियां हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कोई कार्य नहीं करतीं। इनका हिन्दी के प्रति क्या दायित्व है? हिन्दी के विकास-प्रचार के नाम पर वर्ष भर में कुछ कवि सम्मेलन, एक लघु पत्रिका का प्रकाशन जिसमें अपनी अथवा अपनों की ही रचनाएं प्रकाशित होती हैं, ढेर सारा मानदेय, कुछ विमोचन समारोह, अनुदान, छात्रवृत्तियां, शोध वृत्तियां आदि। इस सब पर लाखों रूपये व्यय किये जाते हैं। इन संस्थानों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी कुछ ही वर्षों में एक प्रतिष्ठित साहित्यकार बन जाता है और यहां तक कि उनकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में भी दिखाई देने लगती हैं।
हिन्दी भाषी एवं हिन्दी साहित्यकार हिन्दी प्रचार प्रसार से नहीं जुड़ते। हिन्दी के भ्रष्ट उच्चारण, प्रयोग का विरोध नहीं करते। शब्द, प्रयोग, व्याकरण की चिन्ता नहीं करते।
किसी भी हिन्दी समाचार-पत्र को उठा लीजिए, पचास प्रतिशत से भी अधिक देवनागरी में अंग्रेज़ी शब्द लिखे मिलेंगे। ये समाचार पत्र वास्तव में हिन्दी के माध्यम से अंग्रेज़ी के ही प्रचार-प्रसार में लगे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात:
शिक्षा से हिन्दी गायब हो रही है। हिन्दी का साहित्येतिहास कहीं खो रहा है। जो थोड़ी-बहुत हिन्दी पढ़ाई भी जा रही है वहां मानक हिन्दी का स्वरूप समाप्त होता जा रहा है। आज विद्यालयों में कौन सी हिन्दी पढ़ाई जा रही है इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। निजी प्रकाशक अपनी-अपनी हिन्दी परोस रहे हैं। भाषा, विषय-वस्तु , शब्द प्रयोग, व्याकरण की जांच करने वाला कोई नहीं है। आप प्राथमिक शिक्षा से लेकर दसवी शिक्षा तक की किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर लें भाषिक, व्याकरणिक एवं शाब्दिक त्रुटियों की कोई सीमा नहीं। वर्णमाला का एक नया ही रूप यहां मिलता है। वर्णानुसार अनुस्वरों का प्रयोग अब कोई नहीं जानता। वर्णानुसार अनुस्वरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और न ही उनके बारे में आज के विद्यार्थियों को कोई भी ज्ञान है। केवल बिन्दी का प्रयोग किया जाता है। लेखन और उच्चारण का सम्बन्ध टूट गया है। संयुक्ताक्षर भी वर्णमाला में नहीं पढ़ाए जाते। इनके स्थान पर हलन्त का प्रयाेग ही किया जा रहा है, द्व, द्य, द्ध आदि संयुक्ताक्षर रूप अब गायब हो चुके हैं। द्ध के स्थान पर ध का ही प्रयोग होने लगा है। विद्यालयों में हिन्दी और संस्कृत के शिक्षकों में अन्तर नहीं किया जाता। जो संस्कृत जानते हैं वे हिन्दी तो पढ़ा ही लेंगे। निजी विद्यालयों में हिन्दी बोलने पर दण्डित किया जाता है। दसवीं के बाद हिन्दी का विकल्प प्राय: समाप्त हो चुका है।
हिन्दी भाषा को ठेस पहुंचाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है हिन्दी के साथ “कठिन” की उपाधि। सरल, बोलचाल की हिन्दी के नाम पर हिन्दी के सार्थक शब्दों को हम भूलते जा रहे हैं। अर्थवान शाब्दिक सौन्दर्य, व्याकरणिक महत्व का ह्रास हो रहा है। प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा देने के नाम पर भी हिन्दी का ह्रास हो रहा है।
विश्व की किसी भी भाषा में सरलता के नाम पर अन्य भाषाओं की घुसपैठ नहीं होती। इसमें हमारे संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वाभाविक रूप से कोई भी भाषा स्वयंमेव ही नवीन शब्दों, प्रयोग को ग्रहण करती है। किन्तु आरोपण भाषा की शक्ति का ह्रास करता है। हम शुद्ध हिन्दी बोलते डरते हैं कि ये तो बहुत हिन्दी वाले हैं। एक पिछड़ेपन का एहसास कराता है ।
आज तक कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए हिन्दी को एक मानक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है। फेसबुक पर लिखने के लिए अलग तरह से टंकण करना पड़ता है और जब हम सीधे कम्प्यूटर में वर्ड फाईल में फांट में लिखते हैं तो मात्राओं आदि को अलग प्रकार से लिखना पड़ता है।
शुभकामना संदेश
आज मन उदास है। उदास नहीं, कहते हैं न कि आज मन बहुत खराब है।
क्या किसी को शुभकामना संदेश भेजने से मन खराब हो सकता है ? हाँ , हो सकता है। मेरा हुआ। एक नहीं दो-दो बार।
और शुभकामना संदेश भी साधारण नहीं, जन्मदिन की शुभकामनाएँ। जन्मदिवस का एक सुन्दर-सा संदेश भेजने पर मेरा मन दो बार बहुत खराब हुआ और मुझे शर्मिन्दगी महसूस हुई। है न एक बहुत ही अजीब बात। किन्तु मेरे साथ ऐसा ही हुआ।
मेरे फ़ेसबुक की सूची के अनुसार मेरे 2600 से अधिक मित्र हैं और 644 विचाराधीन सूची में हैं। अब फ़ेसबुक कहती है कि मेरे इतने मित्र हैं तो अपना अहोभाग्य। किन्तु मेरे परिचय में और निकट कितने हैं यह तो मैं भी नहीं जानती। लगभग 100 तो मेरे पुराने सहकर्मी, कुछ कवि-लेखक और अन्य, जिन्होंने मुझे मित्र के रूप में चुना और कुछ को मैंने उन्हें मित्र के रूप में चुना।
किन्तु आज सोचने के लिए विवश हुई कि वास्वत में मित्र कितने हैं। व्यक्तिगत सम्पर्क किसी से नहीं, वार्तालाप, बातचीत शायद किसी से नहीं। लेखक-कवियों से केवल प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान। वैसे भी मुझे मित्र बनाना और निभाना आता ही नहीं। जीवन में मित्रों का अभाव मैंने सदैव अनुभव किया है, एक टीस रही है मेरे भीतर।
विषयान्तर हो गया।
मैंने अपने इन परिचित-अपरिचित फ़ेसबुक मित्रों के प्रति एक नियम बनाया है, वही नियम आज मेरा मन खराब कर गया। फ़ेसबुक प्रतिदिन एक सूची देता है मित्रों के शुभ जन्मदिन की। मैंने नियम बनाया है कि इन अपरिचित मित्रों को अवश्य ही जन्मदिवस की शुभकामना संदेश प्रेषित करूँ।पूरे वर्ष में एक बार ही सही, दो अच्छे वाक्यों का आदान-प्रदान। मैं यह मानकर चलती रही कि मेरा शुभकामना संदेश मेरे फ़ेसबुक मित्र को अच्छा ही लगेगा और उनकी ओर से मिलने वाले धन्यवाद से मेरा मन भी आह्लादित होता है।
किन्तु पिछले सप्ताह जब मैंने ऐसे ही एक मित्र को जन्मदिन की शुभकामना संदेश भेजा तब उनके पुत्र का उत्तर में विनम्र संदेश मिला कि इनका निधन हुए एक वर्ष बीत चुका है। मुझे बेहद बुरा लगा, न तो अफ़सोस करने लायक न उत्तर देने लायक रही मैं। फिर भी मैंने क्षमा माँगी और खेद जताया।
दो दिन पहले फिर ऐसा ही हुआ। किन्तु इस बार संदेश में थोड़ी-सी कटुता थी कि इनका तो निधन हो चुका है और आप जन्मदिन का संदेश भेज रही हैं। मैंने यहाँ भी क्षमा माँगी और खेद व्यक्त किया।
किन्तु मैंने पाया कि दोनों के ही फ़ेसबुक खाते चल रहे हैं।
अब जिनका निधन हो चुका है उनके खाते परिवार ने बन्द क्यों नहीं किये?
अब असमंजस में हूँ कि जन्मदिन के संदेश भेजना जारी रखूँ अथवा बन्द कर देने चाहिए, आप क्या परामर्श देते हैं,?
आज कुछ नया लिखा जाये
मन किया आज कुछ नया लिखा जाये। किन्तु रोज़-रोज़ नया कहाँ से लायें? तो क्या करें ? मंच-मंच घूमें, रचनाएँ पढ़ें और कुछ नया निकाल लायें और तब लिखें। और नया कैसे लिखें कि नकल का आरोप भी न लगे, ऐसा लिखें आगे बताते हैं आपको।
पहले कुछ और बात।
पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से फ़ेसबुकिया साहित्य के क्षेत्र में मुझे अपना-आप महत्वपूर्ण लगने लगा है। आप पूछेंगे क्यों? इधर कुछ दिनों से अत्याधिक निमन्त्रण मिलने लगे हैं समूहों से जुड़ने के लिए। जब समूह की जांच करती तो बड़े-बड़े कवि-साहित्यकार वहाँ दिखते, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से नीचे की तो बात ही नहीं रही अब। ज़ूम पर कवि-सम्मेलन, विदेशी कवि-कवियत्रियाँ, मुँह में पानी आ जाता था लालच से। आह! इतने बड़े प्रतिष्ठित कवि अपने मंच से मुझे जोड़ रहे हैं, अवसर के नये द्वार खुल रहे हैं और कुछ तो मेरे लेखन में भी बात होगी, तभी तो उन्होंने मुझे चुना।
हमने भी झट से ऐसे कितने ही मंचों को अपनी स्वीकृति दे दी। और उसके बाद? मैसेंजर में झड़ी लग गई संदेशों की। बड़े-बड़े पोस्टर, महान-महान कवि-कवियत्रियाँ, वीडियो, फ़ोटो और न जाने कितनी तरह के संदेश। यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भी समूह बनाकर जोड़ लिया जाता है और दस-बीस नहीं सैंकड़ों संदेश यानी कविताएं, विचार पढ़ने के लिए परोस दिये जाते हैं कि मोबाईल टंगने लगता है। किन्तु अपनी इतनी पाचन-शक्ति कहाँ! और हम! मुँह बाये खड़े। कौन पूछता है हमें। मंच पर रचना पोस्ट करो तो महीना-महीना अप्रूव नहीं होती। हमारी वाॅल पर तो क्या आना, रचनाओं पर कभी एक लाईक तक के लिए तरसते हैं नैन। और दूसरी ओर दस-बीस टैगिंग की मार झेलती हमारी वाॅल। मैं तो चकित हूँ कि लोग इतनी टैगिंग कर कैसे लेते हैं। मैंने एक बार अपनी वैबसाईट के लिए टैंगिंग का प्रयास किया था मात्र 49 की अनुमति दी फ़ेसबुक ने और मुझे तीन घंटे लग गये। किन्तु इन कवियों को तो महारत है दिन की दस-दस रचनाएँ और 99 टैगिंग और मैसेंजर, व्हाट्सएप में भी संदेश। सत्य में ही ये महानुभाव चरण-रज के योग्य हैं किन्तु अपनी तो वह भी औकात नहीं।
एक बार तो मन किया कि इस आलेख में उन सबको टैग करूं जिनके कारण मेरा मोबाईल टंगने लगता है, फिर सोचा छोड़ो रे, जी लें अपनी ज़िन्दगी।
अब आईये नयी रचनाओं के सृजन पर। रचनाओं की चोरी की बात तो बहुत पुरानी हो गई, आपको एक नया ढंग बताते हैं। इस हेतु एक नवीन अनुसंधान आपके समक्ष रखती हूँ, बस आपमें थोड़ी योग्यता होनी चाहिए।
किसी की रचना से विषय उठाईये, कविता को गज़ल बनाईये, गज़ल को गीत, गीत को मुक्तछन्द, मुक्तछन्द को छन्दबद्ध, आलेख को कथा, कथा को लघु कथा और सृजन के जितने प्रकार हैं, किसी में भी अपनी ‘‘नवीन’’ रचनाओं का सृजन कीजिए। मज़ाल है कि कोई आप पर चोरी का आरोप लगा सके। पात्रों के नाम, स्थान तो आप बदल ही लेंगे बस बन गई नई रचना। एक और तरीका है पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग का। जैसे आकाश को व्योम, धरा को भूमि, पवन को हवा, सूरज को रवि, आप समझ गये न मेरा मंतव्य।
क्यों कैसा लगा आपको मेरा परामर्श?
मुझे धन्यवाद अवश्य दें।
जैसे ऐसे और कैसे रिश्ते
हमारे पारिवारिक-सामाजिक सम्बन्धों में एक शब्द बहुत महत्व रखता है –“जैसा”,जैसे”,“समान” क्या आपका किन्हीं सम्बन्धों के बीच इन शब्दों का सामना हुआ है।
सीधे-सीधे अपने मन की बात कहती हूं।
किसी ने मुझसे पूछा “क्या यह आपकी बेटी है?”
मैंने कहा “जी नहीं, मेरी बहू है।“
उन्होंने मुझे कुछ तिरस्कार, कुछ उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा और बोले, बहू भी तो बेटी-समान ही होती है। क्या आप अपनी बहू को “बेटी-जैसी” नहीं मानते
मैंने कहा ,नहीं, मैं अपनी बहू को, बेटी “जैसी” नहीं मानती। बहू ही मानती हूं
उनके लिए एवं समाज के लिए मेरा यह उत्तर पर्याप्त नकारात्मक है।
मेरे इस कथन पर मुझे बहुत उपदेश मिले, तिरस्कार-पूर्ण भाव मिले, और मुझे समझाया गया कि सास-बहू में आज इसीलिए इतनी खटपट होती है क्योंकि सासें बहुंओं को अपनाती ही नहीं।
मैंने अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि मैंने अपनाया है अपनी बहू को बहू के रूप में, बहू के अधिकार के रूप में , उसकी जो ‘‘पोस्ट’’ है उसी पर। इसी सम्बन्ध को बनाये रखने में हमारी गरिमा है, किन्तु प्रायः मेरा उत्तर किसी की समझ में नहीं आता। घर में कहते हैं तू क्यों सबसे पंगा लेती है, कहने दे जो कोई कहता है। मेरा प्रश्न है कि हर क्षेत्र के सम्बन्धों की अपनी गरिमा, रूप होता है, उस पर अन्य सम्बन्ध क्यों थोपे जाते हैं ? हम पारिवारिक–सामाजिक सम्बन्धों में यह “जैसा”, “समान” जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करने लगे हैं। जो सम्बन्ध हैं, उनको उसी रूप में सम्मान क्यों नहीं दे पाते।
मैं कार्यरत हूं। अनेक बार कोई सहकर्मी कह देता है “आप तो मेरी मां जैसी हैं।“ कोई कहता है आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, किसी का वाक्य होता है : “मैं तो आपके बेटे जैसा हूं।“
मैं कहती हूं “नहीं, आप केवल मेरे सहकर्मी हैं।“
मेरा यह उत्तर नकारात्मक ही नहीं हास्यास्पद भी होता है।
हम अपने बच्चों को कहते हैं: भाभी को मां समान समझना, देवर को बेटे समान मानना। सास-ससुर की माता-पिता समान सेवा करना। एक महिला अपने ढाई वर्ष के बेटे को पड़ोस की दो वर्ष की बच्ची के लिए कह रही है, बेटा यह तेरी दीदी है। लेकिन साली को बहन समान समझना यह मैंने कभी नहीं सुना।
और सबसे बड़ी बात: बेटी को बेटा जैसा मानें। जहां तक मेरी समझ कहती है इसका अभिप्राय यह कि बेटे और बेटी के अधिकार समान रहें। तो मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि बेटे को बेटी जैसा मानें, जब समानता की बात करनी है तो दोनों ओर से की जा सकती है, अर्थात हम कहीं तो भेद-भाव लेकर चल ही रहे हैं।
हम वे ही रिश्ते क्यों न मानें, जो वास्तव में हैं, उन्हीं सम्बन्धों में पूर्ण सम्मान दें, अधिकार एवं अपनत्व दें, तो क्या सम्बन्धों में ज़्यादा गहराई, ज़्यादा अपनत्व, ज़्यादा विश्वास का भाव नहीं उपजेगा।
क्या सामाजिक –पारिवारिक सम्बन्धों को लेकर हमारे मन में कोई डर, कोई खौफ़ है जो हम हर सम्बन्ध पर एक लबादा ओढ़ाने में लगे हैं, अथवा परत-दर-परत चढ़ाने में लगे हैं।
लोग कहते हैं कि हम सम्बन्धों का नाम देकर सम्मान-भाव प्रदर्शित करते हैं। मेरा प्रश्र होता है कि जो सम्बन्ध वास्तव में है, उस पर कोई और सम्बन्ध लादकर क्या हम वास्तविक सम्बन्धों का अपमान नहीं कर रहे।
अपना तो वोट देना ही बेकार चला गया
अपना तो वोट देना ही बेकार चला गया।
हमारे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा अन्याय होता है अक्सर।
अब देखिए, मैं प्रातः काल सात बजे से टी.वी. देख रही थी। हर शहर में , हर मतदान केन्द्र पर टी. वी. के संवाददाता खड़े थे। वोट देने वालों का साक्षात्कार ले रहे थे।
उनसे पूछ रहे थे
‘‘आपको कैसा लग रहा है वोट देकर’
‘‘आपने किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है’’
एक बेचारे व्हील चेयर पर आये थे। उन्हें न तो सुनाई दे रहा था न ही दिखाई। किन्तु हमारी तो ड्यूटी है उनसे पूछना। सो उनके मुंह में माईक घुसा कर हम पूछ रहे थे
‘‘ आप देखिए व्हील चेयर पर वोट देने आये हैं कैसा लग रहा है आपको’’
वे हकबकाये से कभी माईक को देखें और कभी अपने आस-पास खड़े लोगों को।
एक ‘‘बड़ा व्यक्ति’’ अपने घर से पैदल ही वोट देने आ गया। जब तक हमें अच्छे से याद नहीं हो गया कि फलां व्यक्ति अपने घर से पैदल ही वोट देने आया है, संवाददाता हमें याद कराते रहे।
वे ढूंढ-ढूंढकर वृद्ध, बैसाखी वाले लोगों को, व्हील चेयर वाले मतदाताओं को ढूंढ रहे थे , सब कवर हो गये टी. वी. पर।
अन्त में वे कुछ आम लोगों के बीच भी अपना माईक लेकर आ गये।
‘‘आप सुबह-सुबह सात बजे ही यहां आ गये हैं? ’’
जी हां
तो वोट देने आये हैं
जी हां
अच्छा तो क्या सोचकर वोट देने आये हैं
जी, वोट देनी है यही सोच कर आये हैं
पर कुछ तो मुद्दे होंगे जिनको सोचकर आप वोट दे रहे हैं
जी हां, बेरोजगारी मंहगाई वगैरह , वे आखिर में हारकर बोल दिये।
बाद में ज्ञात हुआ कि वे एक बहुत बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी में हैं किन्तु उनके लिए बेरोज़गारी कैसे मुद्दा है समझ नहीं आया।
हमारा अन्तर्मन भी प्रसन्न हुआ। जल्दी-जल्दी तैयार हुई अच्छे से। मतदान केन्द्र जा रही हूं मत देने, वहां टी. वी. वाले खड़े होंगे, हमारा साक्षात्कार लेंगे। मुद्दे तैयार किये।
पैदल ही गये। पर वहां तो कोई न था।
मत तो देना ही था, यद्यपि मतदान में ही मत शब्द है फिर भी दे दिया। अपना तो आज वोट देना ही बेकार चला गया। हमारे साथ तो पता नहीं ऐसा अन्याय क्यों होता है अक्सर।
एक और कथा बताना और भी ज्यादा जरूरी है।
हम अपने परिचितों में प्रायः बात करते हैं इस बार वोट किसे। हमारे एक मित्र बोले मैं तो मोदी को ही अपना वोट दूंगा। क्यों आप राहुल को दे रही हैं क्या या फिर केजरीवाल को।
मैंने कहा , ये दोनों ही हमारे क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किन्तु मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं वे विधान सभा के लिए आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्या?
मेरी ऐसी बातों पर सब बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मित्र बोले, फालतू में बात खींचती हो, मतलब भाजपा को वोट देगें।
मैं सिरे की ढीठ। फिर पूछ लिया चलिए अच्छी बात है भाजपा को देंगे, प्रत्याशी तो होगा कोई जिसे वोट देंगें।
अब वे उखड़ गये, इससे क्या ।
क्यों नहीं? काम तो प्रत्याशी ही करेगा, न तो भाजपा करेगी, न ही मोदी जी।
जब कुछ पता नहीं तो बोलती क्यों हो, कहकर वे चिढ़कर उठकर चले गये।
सरकार और मीडिया कहते हैं जनता जागृत हो रही है। जी हां, जनता जागृत हो रही है, जागरण करती है, दस रूपये चढ़ाती है, प्रसाद लेती है, उन दस रूपयों में पूरा परिवार खाना खाता है और घर जाकर सो जाता है। फिर सुबह उठकर कहता है , मुझे नहीं पता क्या कहता है, और यदि कुछ कहता भी है तो मुझे क्या लेना, कहता रहे, जिसे जो कहना है।
जो मुद्दे कल थे , वे ही आज हैं और कल भी वे ही रहेंगे, कुछ हेर-फ़ेर के साथ क्योंकि हम जागरण करते हैं जागृत नहीं हो रहे।
कड़वा सच पिलवाऊँगा
न मैंने पी है प्यारी
न मैंने ली है।
नई यूनिफ़ार्म
बनवाई है
चुनाव सभा के लिए आई है।
जनसभा से आया हूँ,
कुछ नये नारे
लेकर आया हूँ।
चाय नहीं पीनी है मुझको
जाकर झाड़ू ला।
झाड़ू दूँगा,
हाथ भी दिखलाऊँगा,
फूलों-सा खिल जाऊँगा,
साईकिल भी चलाऊँगा,
हाथी पर तुझको
बिठलाऊँगा,
फिर ढोलक बजवाऊँगा।
वहाँ तीर-कमान भी चलते हैं
मंजी पर बिठलाऊँगा।
आरी भी देखी मैंने
हल-बैल भी घूम रहे,
तुझको
क्या-क्या बतलाउँ मैं।
सूरज-चंदा भी चमके हैं
लालटेन-बल्ब
सब वहाँ लटके हैं।
चल ज़रा मेरे साथ
वहाँ सोने-चाँदी भी चमके है,
टाट-पैबन्द भी लटके हैं,
चल तुझको
असली दुनियाँ दिखलाऊँगा,
चाय-पानी भूलकर
कड़वा सच पिलवाऊँगा।
कुछ और नाम न रख लें
समाचार पत्र
कभी मोहल्ले की
रौनक हुआ करते थे।
एक आप लेते थे
एक पड़ोसियों से
मांगकर पढ़ा करते थे।
पूरे घर की
माँग हुआ करते थे।
दिनों-दिन
बातचीत का
आधार हुआ करते थे,
चैपाल और काॅफ़ी हाउस में
काफ़ी से ज़्यादा गर्म
चर्चा का आधार हुआ करते थे।
विश्वास का
नाम हुआ करते थे।
ज्ञान-विज्ञान की
खान हुआ करते थे।
नित नये काॅलम
पूरे परिवार के
मनोरंजन का
आधार हुआ करते थे।
-
मानों
युग बदल गया।
अब
समाचार पत्रों में
सब मिलता है
बस
समाचार नहीं मिलते।
कोई मुद्दे,
कोई भाव नहीं मिलते।
पृष्ठ घटते गये
विज्ञापन बढ़ते गये।
चार पन्नों को
उलट-पुलटकर
पलभर में रख देते हैं।
चित्र बड़े हो रहे हैं
पर कुछ बोलते नहीें।
बस
डराते हैं
धमकाते हैं
और चले जाते हैं।
कहानियाँ रह गईं
सत्य कहीं बिखर गया।
अन्त में लिखा रहता है
अनेक जगह
इन समाचारों/विचारों का
हमारा कोई दायित्व नहीं।
तो फिर
इनका
कुछ और नाम न रख लें।
ज़िन्दगी ज़िन्दगी हो उठी
प्रकृति में
बिखरे सौन्दर्य को
अपनी आँखों में
समेटकर
मैंने आँखें बन्द कर लीं।
हवाओं की
रमणीयता को
चेहरे से छूकर
बस गहरी साँस भर ली।
आकर्षक बसन्त के
सुहाने मौसम की
बासन्ती चादर
मन पर ओढ़ ली।
सुरम्य घाटियों सी गहराई
मन के भावों से जोड़ ली।
और यूँ ज़िन्दगी
सच में ज़िन्दगी हो उठी।
खून का असली रंग
हमारे यहाँ
रगों में बहते खून की
बहुत बात होती है।
किसी का खून खानदानी,
किसी का उजला,
किसी का काला
किसी का अपना
और किसी का पराया।
तब आसानी से
कह देते हैं
अपना तो खून ही
ख़राब निकला।
और
ऐसा नीच खून
तो हमारा खून
हो ही नहीं सकता।
-
लेकिन
काश! हम समझ पाते
कि रगों में बहते खून का
कोई रंग नहीं होता
खून का रंग तब होता है
जब वह किसी के काम आये।
फिर अपना हो या पराया,
खानदानी हो या काला,
खून का असली रंग
तभी पहचान में आता है।
लाल, नीला या काला
होने से कभी
कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मित्रता
कृष्ण और सुदामा की मित्रता
यह नहीं
कि एक धनी ने
निर्धन की मदद की,
बल्कि यह
कि मददगार ने
मदद करके
एहसान जताने का
अवसर नहीं दिया।
मेरा नाम श्रमिक है
कहते हैं
पैरों के नीचे
ज़मीन हो
और सिर पर छत
तो ज़िन्दगी
आसान हो जाती है।
किन्तु
जिनके पैरों के नीचे
छत हो
और सिर पर
खुला आसमान
उनका क्या !!!
कैसा दुर्भाग्य है मेरा
कैसा दुर्भाग्य है मेरा
कि जब तक
मेरे साथ दो बैल
और ग़रीबी की रेखा न हो
मुझे कोई पहचानता ही नहीं।
जब तक
मैं असहाय, शोषित न दिखूँ
मुझे कोई किसान
मानता ही नहीं।
मेरी
इस हरी-भरी दुनियाँ में
एक सुख भरा संसार भी है
लहलहाती कृषि
और भरा-पूरा
परिवार भी है।
गुरूर नहीं है मुझे
पर गर्व करता हूँ
कि अन्न उपजाता हूँ
ग्रीष्म-शिशिर सब झेलता हूँ,
आशाओं में जीता हूँ
आशाएँ बांटता हूँ।
दुख-सुख तो
आने-जाने हैं।
अरबों-खरबों के बड़े-बड़े महल
अक्सर भरभराकर गिर जाते हैं,
तो कृषि की
असामयिक आपदा के लिए
हम सदैव तैयार रहते हैं,
हमारे लिए
दान-दया की बात कौन करता है
हम नहीं जानते।
अपने बल पर जीते हैं
श्रम ही हमारा धर्म है
बस इतना ही हम मानते।
होने का एहसास
साथ-साथ होकर भी
आस-पास होकर भी
दिन-रात होकर भी
अक्सर साथ नहीं होते ।n
और मीलों दूर बैठै भी
देश-दुनिया बेखबर
दिला जाते हैं
साथ-साथ
अपने आस-पास
होने का एहसास।
भीतर तक
दीवारों में दरारें होना
ज़रूरी तो नहींए
ज़रा
मिट्टी की परत
हिलने से ही
दुनिया
भीतर तक
झांक लेती है।
अनजाने ही
दरारों से
झांकने की
यूँ आदत तो नहीं
किन्तु
कुछ सुराख
इतने महीन होते हैं
कि
अनजाने ही
दिल में
मिट्टी दरक जाती है।
आदतें ठीक नहीं मेरी
जानती हूँ
बहुत-सी आदतें
तो ठीक नहीं मेरी
पर
कोई अफ़सोस नहीं होता मुझे।
दुनिया-भर की
अच्छाईयों का ठेका
मेरा ही तो नहीं।
कुछ तुम ही
बदल जाओ
मेरे लिए।
जिन्दगी संवारती हूं
भीतर ही भीतर
न जाने कितने रंग
बिखरे पड़े हैं,
कितना अधूरापन
खंगालता है मन,
कितनी कहानियां
कही-अनकही रह जाती हैं,
कितने रंग बदरंग हो जाते हैं।
आज उतारती हूं
सबको
तूलिका से।
अपना मन भरमाती हूं,
दबी-घुटी कामनाओं को
रंग देती हूं,
भावों को पटल पर
निखारती हूं,
तूलिका से जिन्दगी संवारती हूं।
अवसान एवं उदित
यह कैसा समय है,
अंधेरे उजालों को
डराने में लगे हैं,
अपने पंख फैलाने में लगे हैं।
दूर जा रही रोशनियां,
अंधेरे निकट आने में लगे हैं।
अक्सर मैंने पाया है,
अवसान एवं उदित में
ज़्यादा अन्तर नहीं होता।
दोनों ही तम-प्रकाश से
जूझते प्रतीत होते हैं मुझे।
एक रोशनी-रंगीनियां समेटकर
निकल लेता है,
किसी पथ पर,
किसी और को
रोशनी बांटने के लिए।
और दूसरा
बिखरी रोशनी-रंगीनियों को
एक धुरी में बांधकर
फिर बिखेरता है
धरा पर।
चलो, आज एक नई कोशिश करें,
दोनों में ही रंगीनियां-रोशनी ढूंढे।
अंधेरे सिमटने लगेंगें
रोशनियां बिखरने लगेंगी।
डर-डर कर जी रहे हैं
खुले आसमान के नीचे
विघ्न-बाधाओं को लांघकर
समुद्र मापकर
आकाश और धरा को नापकर,
हवाओं को बांधकर,
मानव समझ बैठा था
स्वयं को विधाता, सर्वशक्तिमान।
और आज
अपनी ही करनी से,
अपनी ही कथनी से,
अपने ही कर्मों से,
अपने लिए, आप ही,
तैयार कर लिया है कारागार।
सीमाओं में रहना सीख रहा है,
अपनापन अपनाना सीख रहा है।
उच्च विचार पता नहीं,
पर सादा जीवन जी रहा है।
इच्छाओं पर प्रतिबन्ध लगा है।
आशाओं पर तुषारापात हुआ है।
चाबी अपने पास है
पर खोलने से डरा हुआ है।
दूरियों में जी रहा है
नज़दीकियों से भाग रहा है।
हर पल मर-मर कर जी रहा है,
हर पल डर-डर कर जी रहा है।
देश और ध्वज
देश
केवल एक देश नहीं होता
देश होता है
एक भाव, पूजा, अर्चना,
और भक्ति का आधार।
-
ध्वज
केवल एक ध्वज नहीं होता
ध्वज होता है प्रतीक
देश की आन, बान,
सम्मान और शान का।
.
और यह देश भारत है
और है आकाश में लहराता
हमारा तिरंगा
और जब वह भारत हो
और हो हमारा तिरंगा
तब शीश स्वयं झुकता है
शीश मान से उठता है
जब आकाश में लहराता है तिरंगा।
.
रंगों की आभा बिखेरता
शक्ति, साहस
सत्य और शांति का संदेश देता
हमारे मन में
गौरव का भाव जगाता है तिरंगा।
.
जब हम
निरखते हैं तिरंगे की आभा,
गीत गाते हैं
भारत के गौरव के,
शस्य-श्यामला
धरा की बात करते हैं
तल से अतल तक विस्तार से
गर्वोन्नत होते हैं
तब हमारा शीश झुकता है
उन वीरों की स्मृति में
जिनके रक्त से सिंची थी यह धरा।
.
स्वर्णिम आज़ादी का
उपहार दे गये हमें।
आत्मसम्मान, स्वाभिमान
का भान दे गये हमें
देश के लिए जिएँ
देश के लिए मरें
यह ज्ञान दे गये हमें।
-
स्वर्णिम आज़ादी का
उपहार दे गये हमें।
आत्मसम्मान, स्वाभिमान
का भान दे गये हमें
हम सब कैसे एक हैं
उलझता है बालपन
पूछता है कुछ प्रश्न
लिखा है पुस्तकों में
और पढ़ते हैं हम,
हम सब एक हैं,
हम सब एक हैं।
साथ-साथ रहते
साथ-साथ पढ़ते
एक से कपड़े पहन,
खाते-पीते , खेलते।
फिर आज
यह क्या हो गया
इसे हिन्दू बना दिया गया
मुझे मुसलमान
और इसे इसाई।
और कुछ मित्र बने हैं
सिख, जैनी, बौद्ध।
फिर कह रहे हैं
हम सब एक हैं।
बच्चे हैं हम।
समझ नहीं पा रहे हैं
कल तक भी तो
हम सब एक-से थे।
फिर आज
यूं
अलग-अलग बनाकर
क्यों कह रहे हैं
हम सब एक हैं,
हम सब एक हैं।