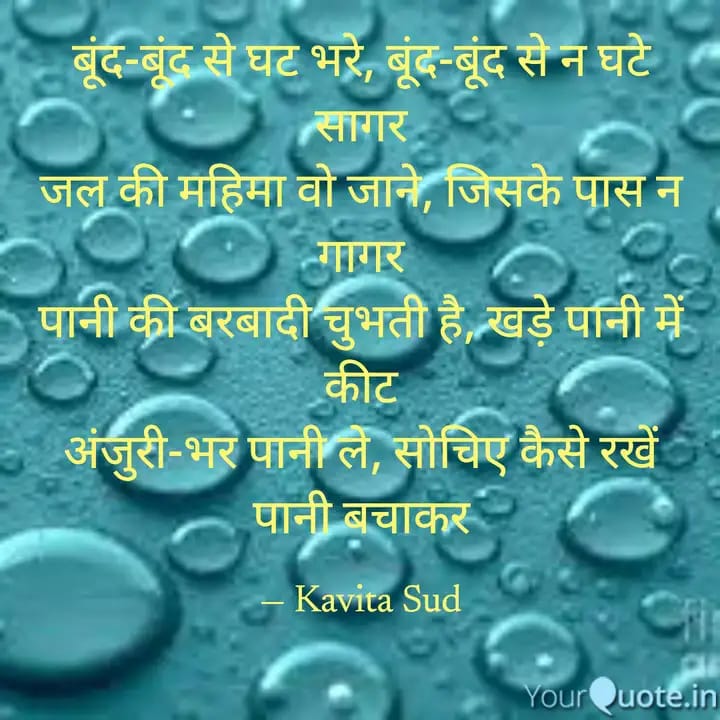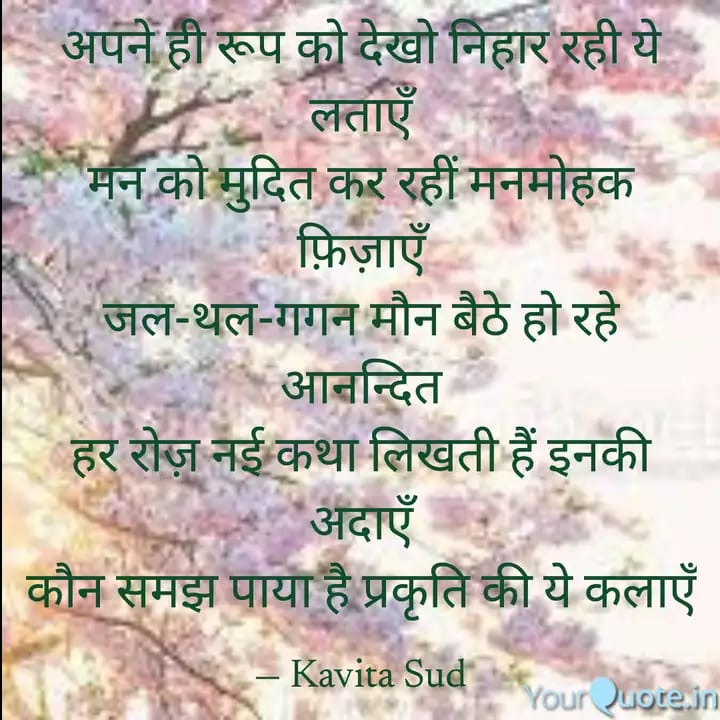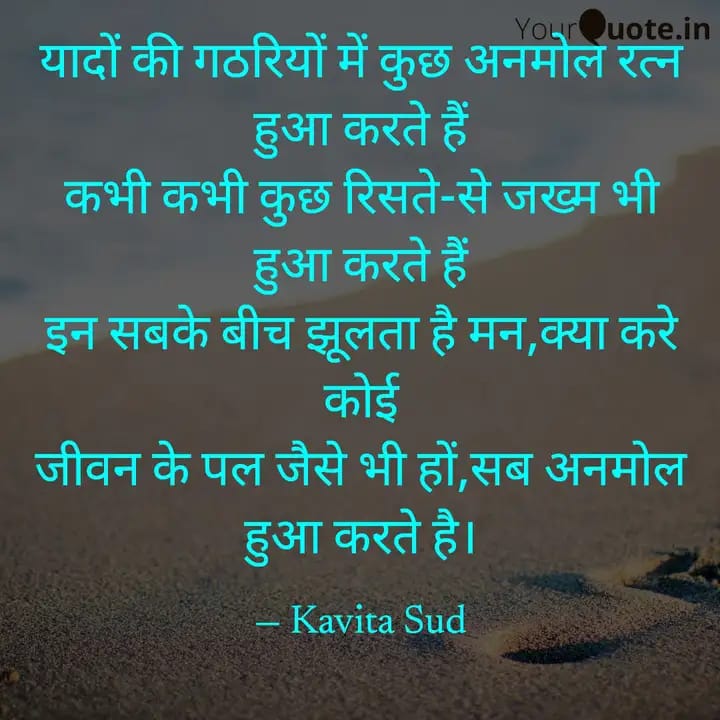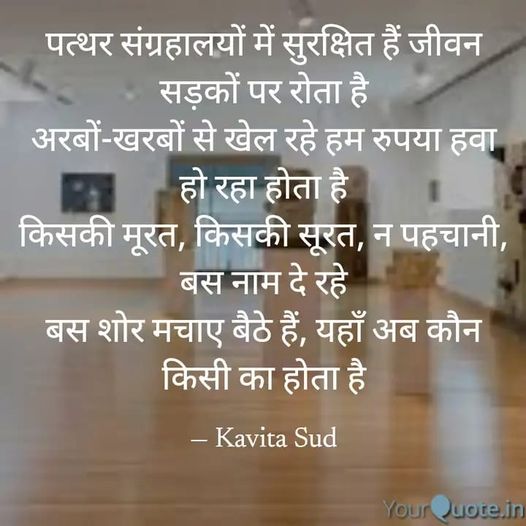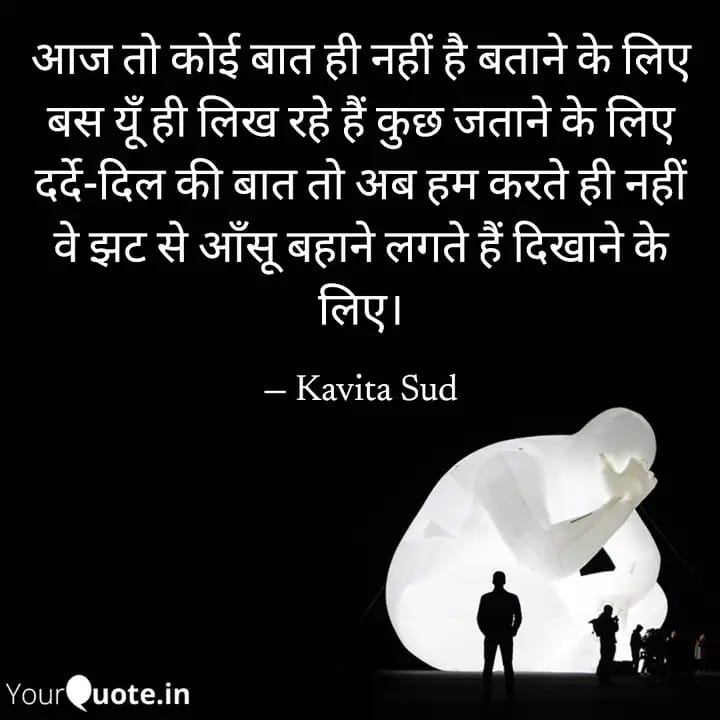कर लो नारी पर वार
जब कुछ न लिखने को मिले तो कर लो नारी पर वार।
वाह-वाही भरपूर मिलेगी, वैसे समझते उसको लाचार।
कल तक माँ-माँ लिख नहीं अघाते थे सारे साहित्यकार
आज उसी में खोट दिखे, समझती देखो पति को दास
पत्नी भी माँ है क्यों कभी नहीं देख पाते हो तुम
यदि माता-पिता को वृद्धाश्रम भेजा, किसका है यह दोष
परिवारों में निर्णय पर हावी होते सदा पुरुष के भाव
जब मन में आता है कर लेते नारी के चरित्र पर प्रहार।
लिखने से पहले मुड़ अपनी पत्नी पर दृष्टि डालें एक बार ।
अपने बच्चों की माँ के मान की भी सोच लिया करो कभी कभार
शुभकामना संदेश
एक समय था
जब हम
हाथों से कार्ड बनाया करते थे
रंगों और मन की
रंगीनियों से सजाया करते थे।
अच्छी-अच्छी शब्दावली चुनकर
मन के भाव बनाया करते थे।
लिफ़ाफ़ों पर
सुन्दर लिखावट से
पता लिखवाया करते थे।
और प्रतीक्षा भी रहती थी
ऐसे ही कार्ड की
मिलेंगे किसी के मन के भावों से
सजे शुभकामना संदेश।
फिर धन्यवाद का पत्र लिखवाया करते थे।
.
समय बदला
बना-बनाया कार्ड आया
मन के रंग
बनाये-बनाये शब्दों के संग
बाज़ार में मिलने लगे
और हम अपने भावों को
छपे कार्ड पर ही समझने लगे।
.
और अब
भाव नहीं
शब्द रह गये
बने-बनाये चित्र
और नाम रह गये।
न कलम है, न कार्ड है
न पत्र है, न तार है
न टिकट है न भार है
न व्यय है
न समय की मार है
पल भर का काम है
सैंकड़ों का आभार है
ज़रा-सी अंगुली चलाईये
एक नहीं,
बीसियों
शुभकामना संदेश पाईये
औपचारिकताएँ निभाईये
काॅपी-पेस्ट कीजिए
एक से संदेश भेजिए
और एक से संदेश पाईये
जल की महिमा
बूंद-बूंद से घट भरे, बूंद-बूंद से न घटे सागर
जल की महिमा वो जाने, जिसके पास न गागर
पानी की बरबादी चुभती है, खड़़े पानी में कीट
अंजुरी-भर पानी ले, सोचिए कैसे रखें पानी बचाकर
प्रकृति का सौन्दर्य
फूलों पर मंडराती तितली को मदमाते देखा
भंवरे को फूलों से गुपचुप पराग चुराते देखा
सूरज की गुनगुनी धूप, चंदा से चांदनी आई
हमने गिरगिट को कभी न रंग बदलते देखा
मन हर्षाए बादल
बिन मौसम आज आये बादल
कड़क-कड़क यूँ डराये बादल
पानी बरस-बरस मन भिगाये
शाम सुहानी, मन हर्षाए बादल
राजनीति अब बदल गई
राजनीति अब बदल गई, मानों दंगल हो रहे
देश-प्रेम की बात कहां, सब अपने सपने बो रहे
इसको काटो, उसको बांटों, बस सत्ता हथियानी है
धमा- चौकड़ी मची है मानों हथेली सरसों बो रहे
प्रकृति की ये कलाएँ
अपने ही रूप को देखो निहार रही ये लताएँ
मन को मुदित कर रहीं मनमोहक फ़िज़ाएँ
जल-थल-गगन मौन बैठे हो रहे आनन्दित
हर रोज़ नई कथा लिखती हैं इनकी अदाएँ
कौन समझ पाया है प्रकृति की ये कलाएँ
जीवन के अनमोल पल
यादों की गठरियों में कुछ अनमोल रत्न हुआ करते हैं
कभी कभी कुछ रिसते-से जख्म भी हुआ करते हैं
इन सबके बीच झूलता है मन,क्या करे कोई
जीवन के पल जैसे भी हों,सब अनमोल हुआ करते है।
कौन किसी का होता है
पत्थर संग्रहालयों में सुरक्षित हैं जीवन सड़कों पर रोता है
अरबों-खरबों से खेल रहे हम रुपया हवा हो रहा होता है
किसकी मूरत, किसकी सूरत, न पहचानी, बस नाम दे रहे
बस शोर मचाए बैठे हैं, यहाँ अब कौन किसी का होता है
अब मैं शर्मिंदा नहीं होता
अब मैं शर्मिंदा नहीं होता
जब कोई मेरी फ़ोटो खींचता है
मुझे ऐसे-वैसे बैठने
पोज़ बनाने के लिए कहता है।
हाँ, कार्य में व्यवधान आता है
मेरी रोज़ी-रोटी पर
सवाल आता है।
कैमरे के सामने पूछते हैं मुझसे
क्या तुम स्कूल नहीं जाते
तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें नहीं पढ़ाते
क्या बाप तुम्हारा कमाता नहीं
अपनी कमाई घर लाता नहीं
कहीं शराब तो पीता-पिलाता नहीं
तुम्हारी माँ को मारता-वारता तो नहीं
अनाथ हो या सनाथ
और कितने भाई-बहन हो
ले जायेगी तुम्हें पुलिस पकड़कर
बाल-श्रम के बारे में क्या जानते हो
किसे अपना माई-बाप मानते हो
सरकारी योजनाओं को जानते हो
उनका लाभ उठाते हो
पूछते-पूछते
उनकी फ़ोटू पूरी हो जाती है
दस रुपये पकड़ाते हैं
और चले जाते हैं
मैं उजबुक-सा बना देखता रह जाता हूँ
और काम पर लौट आता हूँ।
नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे
किसी मित्र ने मुझसे कहा कि आपकी सोच यानी मेरी यानी कविता की सोच बहुत नकारात्मक है। यदि मैं अच्छा सोचूँगी, सकारात्मक रहूँगी तो सब अच्छा ही होगा। इस बात पर उन्होंने एक मुहावरा पढ़ डाला ‘‘नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे’’ किन्तु कैसे उन्होने नहीं बताया।
तो इस मुहावरे पर मेरा एक सरल सा हास्य-व्यंग्य
*-*-*-*-*-*-*
आप अवश्य ही सोचेंगे इसकी तो बुद्धि ही उलट-पुलट है। किन्तु जैसी है, वैसी ही है, मैं क्या कर सकती हूँ। आप सब हर विषय पर गम्भीरता का ताना-बाना क्यों ओढ़ लेते हैं?
अब आप कह रहे हैं, नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे। कैसे भई, किस तरह?
अब इस आयु में मैं तो बदलने से रही। कोई भी योगी-महायोगी कहेगा, बदलने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस प्रयास करना पड़ता है। अब सारा जीवन प्रयास करते ही निकल गया, कभी किसी के लिए बदले, तो कभी किसी के लिए। बचपन में माँ-पिता, बड़े भाई-बहनों के आदेश-निर्देश बदलने के लिए, फिर ससुराल पक्ष के, उपरान्त बच्चों के और अब आप शुरु हो गये। अब तो थोड़ा मनमर्ज़ी से आराम करने दीजिए।
चलिए, कुछ गम्भीर बात कर लेते हैं। क्या मात्र नज़रिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं? पता नहीं, चलिए विचार करने का प्रयास करते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नज़ारे बदलें तो नज़रिया अवश्य बदलता है।
मन उदास है और बाहर खिली-खिली धूप है, गुंजन करते भंवरे, हवाओं से लहलहाते पुष्प, पंछियों की चहक, दूर तक फैली हरियाली, देखिए कैसे नज़रिया बदलता है। आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट खिल आती है, मन आनन्दमय होने लगता है और चाय पीने का मन हो आता है जिसे हम गुस्से में अन्दर छोड़ आये थे।
कोई यदि हमारे सामने अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हम नज़रिया कैसे बदल लें? किन्तु मन खिन्न होने पर हमें कोई सान्त्वना के दो मधुर शब्द बोल देता है, हमारे हित में बात करता है, तो नज़रिया बदल जाता है।
*
किन्तु मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बु़िद्ध उलट-पुलट है। अब आपके पक्ष से विचार करते हैं। नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे।
मैंने नज़रिया बदल लिया।
करेला कड़वा नहीं है, नीम मीठी है। मिर्च तीखी नहीं है, कौआ कितना मीठा गाता है, गोभी का फूल कितना सुन्दर है किसी को भेंट करने के लिए।
हमने करेले-नीम की सब्जी बनाई और यह कहकर सबको खिलाई कि मेरे सकारात्मक विचारों से बनी देखिए कितनी मीठी सब्ज़ी है।
अब यह नज़रिया बदलने पर हमारे क्या नज़ारे बदले न ही पूछिए, क्योंकि हम जानते हैं आप अत्यधिक सकारात्मक विचारों के हैं हमारा दर्द क्या समझेंगे।
कोई बात ही नहीं
आज तो कोई बात ही नहीं है बताने के लिए
बस यूँ ही लिख रहे हैं कुछ जताने के लिए
दर्दे-दिल की बात तो अब हम करते ही नहीं
वे झट से आँसू बहाने लगते हैं दिखाने के लिए।
स्थायी समाधान की बात मत करना
हर रोज़ नहीं करते हम
चिन्ता किसी भी समस्या की,
जब तक विकराल न हो जाये।
बात तो करते हैं
किन्तु समाधान ढूँढना
हमारा काम नहीं है।
हाँ, नौटंकी हम खूब
करना जानते हैं।
खूब चिन्ताएँ परोसते हैं
नारे बनाते हैं
बातें बनाते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में ही
हमें याद आता है
जल संरक्षण
शीत ऋतु में आप
स्वतन्त्र हैं
बर्बादी के लिए।
जल की ही क्यों,
समस्या हो पर्यावरण की
वृक्षारोपण की बात हो
अथवा वृक्षों को बचाने की।
या हो बात
पशु-पक्षियों के हित की
याद आ जाती है
कभी-कभी,
खाना डालिए, पानी रखिए,
बातें बनाईये
और कोई नई समस्या ढूँढिये
चर्चा के लिए।
बस
स्थायी समाधान की बात मत करना।
चाहतों की भूख
जीवन में आगे-पीछे, ऊपर-नीचे तो चलता रहता है
जो पाया, अनायास न जाने कभी कहाँ खो जाता है
बहुत-बहुत की चाह में धक्का-मुक्की में लगे हैं हम
चाहतों की भूख से मानव कहाँ कभी पार पा पाता है।
धन्यवाद देते रहना हमें Keep Thanking
आकाश को थाम कर खड़े हैं नहीं तो न जाने कब का गिर गया होता
पग हैं धरा पर अड़ाये, नहीं तो न जाने कब का भूकम्प आ गया होता
धन्यवाद देते रहना हमें, बहुत ध्यान रखते हैं हम आप सबका सदैव ही
पानी पीते हैं, नहा-धो लेते हैं नहीं तो न जाने कब का सुनामी आ गया होता।
ज्योति प्रज्वलित है
क्यों ढूंढते हो दीप तले अंधेरा जब ज्योति प्रज्वलित है
क्यों देखते हो मुड़कर पीछे, जब सामने प्रशस्त पथ है
जीवन में अमा और पूर्णिमा का आवागमन नियत है
अंधेरे में भी आंख खुली रखें ज़रा, प्रकाश की दमक सरस है
ऐसा अक्सर होता है
ऐसा अक्सर होता है जब हम रोते हैं जग हंसता है
ऐसा अक्सर होता है हम हंसते हैं जग ताने कसता है
न हमारी हंसी देख सकते हो न दुख में साथ होते हो
दुनिया की बातों में आकर मन यूँ ही फ़ँसता है।
धर्म-कर्म के नाम
धर्म-कर्म के नाम पर पाखण्ड आज होय
मंत्र-तंत्र के नाम पर घृणा के बीज बोयें
परम्परा के नाम पर रूढ़ियां पाल रहे हम
किसकी मानें, किसकी छोड़ें, इसी सोच में खोय
नेह के बोल
जल लाती हूँ पीकर जाना,
धूप बहुत है सांझ ढले जाना
नेह की छाँव तले बैठो तुम
सब आते होंगे, मिलकर जाना
एक पंथ दो काज
आजकल ज़िन्दगी
न जाने क्यों
मुहावरों के आस-पास
घूमने लगी है
न तो एक पंथ मिलता है
न ही दो काज हो पाते हैं।
विचारों में भटकाव है
जीवन में टकराव है
राहें चौराहे बन रही हैं
काज कितने हैं
कहाँ सूची बना पाते हैं
कब चयन कर पाते हैं
चौराहों पर खड़े ताकते हैं
काज की सूची
लम्बी होती जाती है
राहें बिखरने लगती हैं।
जो राह हम चुनते हैं
रातों-रात वहां
नई इमारतें खड़ी हो जाती हैं
दोराहे
और न जाने कितने चौराहे
खिंच जाते हैं
और हम जीवन-भर
ऊपर और नीचे
घूमते रह जाते हैं।
धुआँ- धुआँ ज़िन्दगी
कुछ चेतावनियों के साथ
बेहिचक बिकता है
कोई भी, कहीं भी
पी ले
सुट्टा ले
हवा ले और हवाओं में ज़हर घोले
पूर्ण स्वतन्त्र हैं हम।
शानौ-शौकत का प्रतीक बन जाता है।
कहीं गम भुलाने के लिए
तो कहीं सर-दर्द मिटाने के लिए
कभी दोस्ती के लिए
तो कभी
देखकर मन ललचाता है
कुछ आधुनिक दिखने की चाहत
खींच ले जाती है
एकान्त में, छिपकर
फिर दिखाकर
और बाद में अकड़कर।
और जब तक समझ आता है
तब तक
धुआँ- धुआँ हो चुकी होती है ज़िन्दगी।
ज़िन्दगी के गीत
ज़िन्दगी के कदमों की तरह
बड़ा कठिन होता है
सितार के तारों को साधना।
बड़ा कठिन होता है
इनका पेंच बांधना।
यूँ तो मोतियों के सहारे
बांधी जाती हैं तारें
किन्तु ज़रा-सा
ढिलाई या कसाव
नहीं सह पातीं
जैसे प्यार में ज़िन्दगी।
मंद्र, मध्य, तार सप्तक की तरह
अलग-अलग भावों में
बहती है ज़िन्दगी।
तबले की थाप के बिना
नहीं सजते सितार के सुर
वैसे ही अपनों के साथ
उलझती है जिन्दगी
कभी भागती, कभी रुकती
कभी तानें छेड़ती,
राग गाती,
झाले-सी दनादन बजती,
लड़ती-झगड़ती
मन को आनन्द देती है ज़िन्दगी।
ताकता रह जाता है मानव
लहरें उठ रहीं
आकाश को छूने चलीं
बादल झुक रहे
लहरों को दुलारते
धरा को पुकारते।
गगन और धरा पर
जल और अनिल
उलझ पड़े
बदरी रूठ-रूठ उमड़ रही
रंग बदरंग हो रहे
कालिमा घिर रही
बवंडर उठ रहे
ताकता रह जाता है मानव।
एक किस्सागोई
कुछ बातें बेवजह याद आती हैं लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पातीं।
वैसे तो 22 मार्च 2020 से ही घर पर हूं, जब पहला लॉक डाउन हुआ था किन्तु आधिकारिक तौर पर 20 जुलाई 2020 को त्यागपत्र देकर घर ही हूं।
तो कल तक जब यानी 20 जुलाई 2020 से पूर्व कोई मुझे पूछता था कि आप क्या करती हैं तो मैं पहले कहा करती थी, बैंक में कार्यरत हूं, उपरान्त मैं इस विद्यालय में वरिष्ठ लेखाकार हूं।
21 जुलाई 2020 से मेरी पोस्ट बदल गई। अब मेरी पोस्ट क्या है, यही विचार करने के लिए यह आलेख लिख रही हूं।
बात यह कि कुछ वर्ष पहले तक जो महिला नौकरी नहीं करती थी, उसे घरेलू महिला हाउस वाईफ़ कहा जाता था, और इसे बड़े सामान्य तौर पर लिया जाता था, चाहे वह महिला कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो। और नौकरी न करना कोई अपराध अथवा हीन भावना भी नहीं होती थी।
वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है।
विद्यालय में बच्चों के प्रवेश फ़ार्म में माता-पिता के विवरण के विस्तृत काॅलम होते हैं, जिनमें उनकी शिक्षा, नौकरी, कार्यक्षेत्र, कार्यस्थल, वेतन, अन्य अनुभवों आदि की जानकारी मांगी जाती है।
इसी काॅलम से मेरा यह आलेख निकला। मैंने देखा कि कुछ फ़ार्मों में माता के विवरण में जाॅब/बिजनैस के आगे लिखा मिलने लगा: हाउस मेकर, हाउस मैनेजर, हाउस इंचार्ज। किन्तु विभाग के आगे कोई सूचना नहीं लिखी गई थी। मैं महामूर्ख। मुझे लगा सम्भवतः किसी हास्पिटैलिटीए होटल आदि में कोई पोस्ट होगी।
मैं एक महिला से पूछ बैठी मैम आपने डिपार्टमैंट नहीं लिखा। डिपार्टमैंट मतलब? मैंने लिखा तो है हाउस मैनेजर। जी हां, पोस्ट तो लिखी है, डिपार्टमैंट, आफिॅस का पता भी तो लिखिए।
उसे बड़ा अपमानजनक लगा मेरा प्रश्न। क्रोध से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं कि जो लेडीज जाॅब नहीं करतीं, वो केवल घरेलू, अनपढ़, गंवार, निकम्मी होती हैं क्या? मैं हाउस मेकर, हाउस मैनेजर हूं, घर हम औरतें ही बनाती हैं।
मैं एकदम हकबका-सी गई, तो क्या ये पोस्ट हो गई। तो फिरघर में पति की क्या पोस्ट है, पूछ नहीं पाई।
मैं अचानक ही बोल बैठी, तो आप हाउस-वाईफ़ हैं। आपने पोस्ट के सामने हाउस मैनेजर लिखा है न, मुझे लगा किसी विभाग में पोस्ट का नाम होगा। साॅरी अगर आपको बुरा लगा।
अब नाराज़गी चरम पर थी। बोली, हाउस वाईफ़ का क्या मतलब होता है? मैं कोई अनपढ़, गंवार औरत हूं कि बस एक घरेलू औरत हूं। घर हम औरतें ही चलाती हैं। क्या वह काम नहीं है? क्या आपकी तरह बाहर नौकरी न करने वाली औरतें क्या बस घरेलू ही हैं। क्या आप ही काम करती हैं जो घर से बाहर नौकरी करती हैं। हम घर चलाती हैं, घर सम्हालती हैं तो हाउस मैनेजर, हाउस मेकर हुई या नहीं। हमारे बिना घर चल सकता है क्या? हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? घर तो हम औरतें ही बनाती हैं न।
मैं भी सिरे की ढीठ। उल्टी खोपड़ी। पीछे हटने वाली कहां। मैंने आगे से कहा, मैम वो तो सारी ही महिलाएं करती हैं, हम नौकरी वाली भी करती हैं तो क्या मुझे अपनी पोस्ट के साथ ओब्लीग करके हाउस मेकर भी लिखना चाहिए। और घर सम्हालना कोई नौकरी तो नहीं हुई न। यहां काॅलम जाॅब/बिज़नेस है।
वह महिला देर तक बड़बड़ाती रही। और उसने वर्तमान में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, विरोध, शोषण, उनके अधिकारों के हनन, सम्मान की कमी, पारिवारिक समस्याओं और न जाने कितने विषयों पर भाषण दे डाला।
मैं समझ नहीं पाई कि घर से बाहर नौकरी न करना हीन भावना क्यों बनने लगा है और घर में रहना एक जाॅब या नौकरी कैसे बना। निःसदेह महिलाओं के साथ अनेक क्षेत्रों में अन्याय, विरोधाभास है किन्तु इन बातों के अत्यधिक प्रचार-प्रसार ने महिलाओं की सोच को भी प्रभावित कर दिया है। इसका दुष्परिणाम यह कि महिलाओं की परिवार के प्रति सोच संकुचित होने लगी है और वे उन क्षेत्रों में भी अधिकारों की बातें करने लगी हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र की नहीं हैं। मुझे लगता है महिलाओं में इस तरह की सोच, प्रवृत्ति, उन्हें आत्मनिर्भर, स्वाबलम्बी, स्वतन्त्र नहीं बना रही, पुरुष समाज के विरुद्ध अकारण खड़ा कर रही है। उनमें पारिवारिक दायित्वों के प्रति एक विमुखता ला रही है। अपने पारिवारिक दायित्वों को एक जाॅब या नौकरी समझने से सोच बहुत बदली है और महिलाओं की मानसिकता में गहरी नकारात्मकता आने लगी है।
कर्तव्य श्री
दृश्य एकः
श्री जी की पत्नी का निधन हो गया। अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गई। माता-पिता बूढ़े थे, बच्चे छोटे-छोटे। बूढ़े-बुढ़िया से अपना शरीर तो संभलता न था बच्चे और घर कहां संभाल पाते। और श्री जी अपनी नौकरी देखें, बच्चे संभाले या बूढे़-बुढ़िया की सेवा करें।
बड़ी समस्या हुई। कभी भूखे पेट सोते, कभी बाहर से गुज़ारा करते। श्री जी से सबकी सहानुभूति थी। कभी सासजी आकर घर संभालती, कभी सालियांजी, कभी भाभियांजी और कभी बहनेंजी। पर आखिर ऐसे कितने दिन चलता। आदमी आप तो कहीं भी मुंह मार ले पर ये बूढ़े-बुढ़िया और बच्चे।
अन्ततः सबने समझाया और श्री जी की भी समझ में आया। रोटी बनाने वाली, बच्चों कोे सम्हालने वाली, घर की देखभाल करने वाली और बूढ़े-बुढ़िया की देखभाल करने वाली कोई तो होनी ही चाहिए। भला, आदमी के वश का कहां है ये सब। वह नौकरी करे या ये सब देखे। सो मज़बूर होकर महीने भर में ही लानी पड़ी।
और इस तरह श्री जी की जिन्दगी अपने ढर्रे पर चल निकली।
‘अथ सर्वशक्तिमान पुरुष’
दृश्य दोः
श्रीमती जी के पति का निधन हो गया। अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गये। सास-ससुर बूढ़े थे। बच्चे छोटे-छोटे। श्रीमती जी स्वयं अभी बच्चा-सी दिखतीं। दसवीं की नहीं कि माता-पिता पर भारी हो गई। शहर में लड़का मिल गया सरकारी नौकर, घर ठीक-ठाक-सा। बस झटपट शादी कर दी। अब यह पहाड़ टूट पड़ा। कभी दहलीज न लांघी थी, सिर से पल्लू न हटा था। पर अब कमाकर खिलाने वाला कोई न रहा। बूढ़े-बुढ़िया से अपना शरीर तो संभलता न था, करते-कमाते क्या ? भूखांे मरने की नौबत दिखने लगी।
अब नाते-रिश्तेदार भी क्या करें ? सबका अपना-अपना घर, बाल-बच्चे, काम और नौकरियां, आखिर कौन कितने दिन तक साथ देता। सब एक-दूसरे से पहले खिसक जाना चाहते थे। कहीं ये बूढ़े-बुढ़िया, श्रीमतीजी या बच्चे किसी का पल्लू न पकड़ लें।
अन्ततः श्रीमती जी स्वयं उठीं। पल्लू सिर से उतारकर कमर में कसा। पति के कार्यालय जाकर खड़ी हो गईं नौकरी पाने के लिए।
अभी महीना भी न बीता था कि श्रीमतीजी लगी दफ्तर में कलम चलाने। प्रातः पांच बजे उठकर घर संवारतीं, बूढ़े-बुढ़िया की आवश्यकताएं पूरी करती। बच्चों को स्कूल भेजतीं। खाना-वाना बनाकर दस बजे दफ््तर पहुंच जाती, दिन-भर वहां कलम घिसतीं। शाम को बच्चों का पढ़ातीं। घर-बाहर देखतीं, राशन-पानी जुटाती, दुनियादारी निभातीं। खाती-खिलाती औेर सो जातीं।
और इस तरह श्रीमतीजी की जिन्दगी अपने ढर्रे पर चल निकली।
‘बेचारी कमज़ोर औरत’
हास्य बाल कथा गीदड़ और ऊंट की कहानी
अध्यापक ने तीसरी कक्षा के बच्चों को यह बोध कथा सुनाई।
एक जंगल में गीदड़ और ऊंट रहते थे। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, नदी पार गन्नों का खेत है, चलो आज रात वहां गन्ने खाने चलते हैं। ऊंट ने पूछा कि तुम कैसे नदी पार करोगे, तुम्हें तो तैरना नहीं आता। गीदड़ ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें गन्ने के खेत के बारे में बताया, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा देना। हम अंधेरे में ही चुपचाप गन्ने खाकर आ जायेंगे, खेत का मालिक नहीं जागेगा।
दोनों नदी पारकर खेत में गये और पेटभर कर गन्ने खाये। ऊंट ने कहा चलो वापिस चलते हैं। लेकिन गीदड़ अचानक गर्दन ऊपर उठाकर ‘‘हुआं-हुआं’’ करने लगा। ऊंट ने उसे रोका, कि ऐसा मत करो, खेत का मालिक जाग जायेगा और हमें मारेगा। गीदड़ ने कहा कि खाना खाने के बाद अगर वह ‘‘हुआं-हुआ’’ न करे तो खाना नहीं पचता। और वह और ज़ोर से ‘‘हुंआ-हुंआ’’ करने लगा। खेत का मालिक जाग गया और डंडा लेकर दौड़ा। गीदड़ तो गन्नों में छुप गया और ऊंट को खूब मार पड़ी।
तब वे फिर नदी पार कर लौटने लगे और गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। गहरी नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट डुबकियां लेने लगा। गीदड़ चिल्लाया अरे ऊंट भाई, यह क्या कर रहे हो, मैं डूब जाउंगा। ऊंट ने कहा कि खाना खाने के बाद जब तक मैं पानी में डुबकी नहीं लगा लेता मेरा भोजन नहीं पचता। ऊंट ने एक गहरी डुबकी लगाई और गीदड़ डूब गया।
अब अध्यापक ने बच्चों से पूछा ‘‘ बच्चो, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?’’
एक बच्चे ने उठकर कहा ‘‘ इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि खाना खाने के बाद ‘‘हुंआ-हुंआ नहीं करना चाहिए।’’
आत्म संतोष क्या जीवन की उपलब्धि है 2
पिछले कुछ समय से मैं एक गम्भीर प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हूं। प्रश्न आर्थिक/वित्तीय है। अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं शहर के विभिन्न बैंकों में गई, वित्तीय संस्थानों में पूछताछ की। स्टॉक एक्सचेंज की खाक छानी, विदेशी मुद्रा विनिमय केन्द्रों में गई, बड़े-बड़े वित्तीय अधिकारियों से मिली, किन्तु मेेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
अब मैं अपना प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जब बड़ी-बड़ी संस्थाएँ और बड़े-बडे़ लोग मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाये तो मैं अपने वयोवृद्ध दादाजी के पास जा बैठी। मुझे रुंआसी देखकर दादाजी ने कारण पूछा। डूबते को क्या चाहिए एक तिनके का सहारा। मैंने अपना प्रश्न दादाजी के मामन रख दिया। दादाजी, लोग रुपये की बात करते हैं डॅालर, पौंड, यूरो और न जाने कितना विदेशी मुद्राओं की बात करते हैं किन्तु मैंने एक नये धन का नाम सुना है जिसे सन्तोष धन कहा जाता है। यह धन तो मैंने किसी के पास नहीं देख।
जिससे पूछती हूं वही मेरा उपहास करता हे कि अरे इस पगली लड़की को देखो, भला आज के ज़माने में भी कहीं संतोष धन पाया जाता है। दादाजी कोई नहीं मानता कि संतोष भी कोई धन होता है। अब आप ही बताईये दादाजी , यह संतोष धन कौन-सा धन है कहां मिलता है, कहां पाया जाता है , कौन प्रयोग करता है । किस काम आता है। यह कैसा गुप्त धन है जिसके बारे में बड़े-बड़े लोग नहीं जानते।
दादाजी मेरी बात सुनकर ठठाकर हंस दिये। बोले बेटी, संतोष धन तो मनुष्य ने सदियों पहले ही खो दिया। और तुम पुरातात्विक विभाग की वस्तु को आधुनिक विज्ञान की मशीनों में खोजोगी तो भला बताओ कैसे मिलेगी? अब आधुनिकता की दौेड़ में जुटे लोगों की रुचि भला पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी की वस्तुओं में कैसे हो सकती है।
लेकिन वे चकित भी थे कि मुझे इस संतोष धन का पता कैसे लगा। क्या मैंने इस धन को पा लिया है। मैं हंस दी नहीं दादाजी मुझे यह धन नहीं मिला। मैंने उन्हें बताया कि कोई कबीरदास हुआ करते थे वे लिख गये हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब दादाजी से तो बहुत बातें हूईं किन्तु उनसे वार्तालाप में मेरे सामने अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। उन्हीं पर चिन्तन करते हुए मैं आपके समक्ष हूं।
क्या सत्य में ही आधुनिकता के पीछे भाग रहे मनुष्य ने संतोष धन खो दिया है। कबीरदास ने कहा कि जिस मनुष्य के पास संतोष धन है उसके सामने सब धन धूल के समान हैं अर्थात उनका कोई महत्व नहीं।
किन्तु वर्तमान में इस दोहे के अर्थ बदल गये हैं। वर्तमान में इस दोहे का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास संतोष धन है उसके लिए सब धन धूल के समान हो जातेे हैं अर्थात उसे जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती।
तो क्या जीवन में सचमुच संतोष ही सबसे बड़ी उपलब्धि है? मेरी दृष्टि में नहीं। मेरी दृष्टि में संतोष का अभिप्राय है एक ठहराव, निप्क्रियता, इच्छाओं का दमन। यदि मानव ने अपनी स्थितियों पर संतोेष कर लिया होता तो वह आज भी वन में पत्थर रगड़ कर आग जला रहा होता, पत्तों के वस्त्र धारण कर वृक्षों पर सो रहा होता। मेरी दृप्टि में संतोष न करने का अभिप्राय है, आगे बढ़ने की इच्छा, प्रगति की कामना, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, नव-नवोन्मेष प्रतिभा एवं विचारो का स्तवन, अनुसंधान, स्वाबलम्बन, अच्छे से अच्छा करने की कामना।
संतोष न करने का ही परिणाम हे कि आज हम चांद पर पहुंच गये हैं, समुद्र की अतल गहराईयों को नाप रहे हैं। लाखों मीलों की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं।
विश्व के एक कोने में बैठकर सम्पूर्ण विश्व के लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं।
यदि मैं संतोष धन अपना लूं तो कभी भी अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास ही न करुं। उत्तीर्ण होकर भी क्या करता है, संतोष धन तो पा ही लिया है। माता-पिता से कहूँगी मैंने संतोष धन प्राप्त कर लिया है मुझे आगे मत पढ़ाईये।
मेरे कुछ साथी संतोष-असंतोष की तुलता कर सकते हैं कि संतोष न होने का अर्थ है असंतोष। किन्तु मेरी दृष्टि में असंतोष एक मानसिक वेदना है जो ईर्ष्या-द्वेष-भाव से उपजती है जबकि संतोष न करने की भावना प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है।
खामोशियां भी बोलती है
नई बात। अब कहते हैं मौन रहकर अपनी बात कहना सीखिए, खामोशियाँ भी बोलती हैं। यह भी भला कोई बात हुई। ईश्वर ने गज़ भर की जिह्वा दी किसलिए है, बोलने के लिए ही न, शब्दाभिव्यक्ति के लिए ही तो। आपने तो कह दिया कि खामोशियाँ बोलती हैं, मैंने तो सदैव धोखा ही खाया यह सोचकर कि मेरी खामोशियाँ समझी जायेगी। न जी न, सरासर झूठ, धोखा, छल, फ़रेब और सारे पर्यायवाची शब्द आप अपने आप देख लीजिएगा व्याकरण में।
मैंने तो खामोशियों को कभी बोलते नहीं सुना। हाँ, हम संकेत का प्रयास करते हैं अपनी खामोशी से। चेहरे के हाव-भाव से स्वीकृति-अस्वीकृति, मुस्कान से सहमति-असहमति, सिर से सहमति-असहमति। लेकिन बहुत बार सामने वाला जानबूझकर उपेक्षा कर जाता है क्योंकि उसे हमें महत्व देना ही नहीं है। वह तो कह जाता है तुम बोली नहीं तो मैंने समझा तुम्हारी मना है।
कहते हैं प्यार-व्यार में बड़ी खामोशियाँ होती हैं। यह भी सरासर झूठ है। इतने प्यार-भरे गाने हैं तो क्या वे सब झूठे हैं? जो आनन्द अच्छे, सुन्दर, मन से जुड़े शब्दों से बात करने में आता है वह चुप्पी में कहाँ, और यदि किसी ने आपकी चुप्पी न समझी तो गये काम से। अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है।
मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। खामोशी की भाषा अभिव्यक्ति करने वाले से अधिक समझने वाले पर निर्भर करती है। शायद स्पष्ट ही कहना पड़ेगा, गोलमाल अथवा शब्दों की खामोशी से काम नहीं चलने वाला।
मेरा अभिप्राय यह कि जिस व्यक्ति के साथ हम खामोशी की भाषा में अथवा खामोश अभिव्यक्ति में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वह कितना समझदार है, वह खामोशी की कितनी भाषा जानता है, उसकी कौन-सी डिग्री ली है इस खामोशी की भाषा समझने में। बस यहीं हम लोग मात खा जाते हैं।
इस भीड़ में, इस शोर में, जो जितना ऊँचा बोलता है, जितना चिल्लाता है उसकी आवाज़ उतनी ही सुनी जाती है, वही सफ़ल होता है। चुप रहने वाले को गूँगा, अज्ञानी, मूर्ख समझा जाता है।
ध्यान रहे, मैं खामोशी की भाषा न बोलना जानती हूँ और न समझती हूँ, मुझे अपने शब्दों पर, अपनी अभिव्यक्ति पर, अपने भावों पर पूरा विश्वास है और ईश प्रदत्त गज़-भर की जिह्वा पर भी।
मोबाईल: आवश्यकता अथवा व्यसन
हमारी एक प्रवृत्ति हो गई है कि हम बहुत जल्दी किसी भी बात की आलोचना अथवा सराहना करने लगते हैं। कोई एक करता है और फिर सब करने लगते हैं जैसे मानों नम्बर बनाने हों कि किसने कितनी आलोचना कर ली अथवा सराहना कर ली। जैसे हमारी विचार-शक्ति समाप्त हो जाती है और हम निर्भाव बहती धारा के साथ बहने लगते हैं।
मोबाईल!!!
आधुनिकता के इस युग में मोबाईल जीवन की आवश्यकता बन चुका है। चाहे कितनी भी आलोचना कर लें किन्तु वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में इसके महत्व और आवश्यकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको मोबाईल किस स्तर का चाहिए और किस कार्य के लिए।
एक समय था जब विद्यालयों में मोबाईल ले जाना प्रतिबन्धित था। फिर समय ऐसा आया कि यही मोबाईल शिक्षा का केन्द्र बन गया। कोराना काल ने आम आदमी के जीवन में इतने परिवर्तन कर दिये कि एक बार तो वह स्वयं ही समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। जब तक समझ आती, जीवन की धाराएँ ही बदल चुकीं थीं।
शिक्षा का यह ऐसा काल था, लगभग दो वर्ष का, जिसने शिक्षा, ज्ञान और परीक्षाओं के सारे प्रतिमान ही बदल कर रख दिये। शिक्षा की इस नवीन प्रणाली ने पारिवारिक व्यवस्थाएँ, आवश्यकताएँ, जीवन का ढाँचा ही बदल कर रख दिया। देश के मध्यमवर्गीय परिवारों में रोटी से अधिक महत्वपूर्ण मोबाईल हो उठे। फिर वह पहली कक्षा का विद्यार्थी हो अथवा किसी बड़ी कक्षा का। किसी-किसी परिवार में एक साथ दो-दो लैपटॉप और तीन-चार मोबाईल की आवश्यकता उठ खड़ी हुई अर्थात लाखों का व्यय। आय बन्द, व्यवसाय बन्द, वेतन आधा और मोबाईल ज़रूरी। ऐसे कितने ही परिवार मैंने इस समय में देखे जहाँ माता-पिता के पास एक-एक मोबाईल था और पिता के पास लैपटॉप। अब तीन बच्चे। तीनों की एक समय ऑनलाईन क्लास। माता अध्यापिका। अब एक लैपटॉप और तीन मोबाईल की अनिवार्यता उठ खड़ी हुई। चाहिए भी एंड्राएड अर्थात कम से कम 15-20 हज़ार प्रति। जहाँ मोबाईल पढ़ाई की आवश्यकता बने वहाँ आदत का हिस्सा भी। असीमित ज्ञान का भण्डार। आय-व्यय, बैंकिंग, भुगतान-प्राप्ति का सरल साधन, डिजिटल पेमंट, खेल का माध्यम। बच्चे घर में बैठकर पूरी दुनिया से जुड़ रहे थे, ज्ञान का असीमित भण्डार का पिटारा मानों उनके सामने खुल गया था और वे अचम्भित थे। माता-पिता से जल्दी बच्चे यह सब सीखने लगे। इसमें कहीं भी कुछ भी ग़लत अथवा ठीक नहीं कहा जा सकता था, यह सब समय की आवश्यकता के कारण विकसित हो रहा था, जो धीरे-धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बनता गया। यदि शिक्षा के क्षेत्र में यह मोबाईल न होता तो बच्चे दो वर्ष पीछे चले जाते और उन्होंने ऑन लाईन जो ज्ञान प्राप्त किया, आधुनिकता से जुड़े, वह एक बहुत बड़ा अभाव रह जाता।
आज का समय ऐसा नहीं है कि बच्चे विद्यालय से निकले और घर। नहीं जी, ट्यूशन, डांस क्लास, स्विमिंग, क्रिकेट और न जाने क्या-क्या। तब माता-पिता और बच्चों के बीच यही एक वार्तालाप का सहारा बनता है
ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही मोबाईल ने हमारे जीवन को प्रभावित किया। इससे पूर्व भी विद्यालयों में सीनियर कक्षाओं में प्रोजेक्ट वर्क, आर्ट वर्क और अनेक गृह कार्य ऐसे दिये जाते थे जो गूगल देवता की सहायता से ही किये जाते थे। कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड और अनेक तकनीक प्रयोग में पहले से ही चल रहे थे, बस मोबाईल की इसमें वृद्धि हुई।
किसी सीमा तक यह बात ठीक है कि जब किसी वस्तु का हम अत्याधिक प्रयोग करने लगत हैं तब आवश्यकता से बढ़कर वह हमारी आदत बन जाती है, हमें उसकी लत लग जाती है और जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है।
निश्चित रूप से बच्चे आज पक्षियों की भांति स्वतन्त्र पंछी नहीं रह गये हैं। इसका एक कारण मोबाईल हो सकता है किन्तु सारा दोष केवल मोबाईल को नहीं दिया जा सकता। आधुनिकतम जीवन शैली, शिक्षा एवं ज्ञान का माध्यम, बच्चे तो क्या हमारी पीढ़ी भी इसमें उलझी बैठी है। अब यह माता-पिता का कर्तव्य है और शिक्षा-संस्थानों का भी कि बच्चों को मोबाईल के उचित प्रयोग एवं सीमित प्रयोग के लिए प्रेरित करें न कि उन्हें आरोपित।
विश्व चाय दिवस
सुबह से भूली-भटकी अभी मंच पर आगमन हुआ तो ज्ञात हुआ कि आज तो अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस अथवा विश्व चाय दिवस है।
ऐसा कैसे सम्भव है। चाय का और केवल एक दिवस! नहीं, नहीं, यह तो चाय का और चाय के नशेड़ियों का घोर अपमान है।
शिमला में हम परिवार में आठ सदस्य थे, दिन-भर में 80-90 चाय तो बनती ही होगी और वह भी लार्ज पटियाला साईज़, पीतल के बड़े गिलास। मेरी दादी मेरी माँ से कहती थी पानी की टंकी में ही चीनी-पत्ती डाल दे, अपने-आप सब दिन-भर पीते रहेंगे।
दिन भर में पाँच-छः चाय तो अब भी पी ही लेती हूँ। कुछ वर्ष पहले तक दस-बारह हो ही जाती थी। उससे पहले 12-15। गज़ब की पाचन-क्षमता रही है मेरी। प्रातः घर से 7.30 निकल जाती थी किन्तु आम बात थी कि चार से पांच चाय पी लेती थी। काम करते-करते एक कप खाली हुआ, दूसरा तैयार। एक नाश्ते के साथ और दूसरा नाश्ते के बाद। फिर कार्यालय पहुँचकर टेबल पर सबसे पहले चाय। चाय देने वाले को भी पता था कि मैडम को कितनी चाय चाहिए होती है। वैसे भी छोटे-छोटे गिलास में आती चाय वैसे ही मूड खराब कर देती है इस कारण मुझे हर जगह अपना ही कप या गिलास रखना पड़ता था। जब मेरा स्थानान्तरण हुआ तो मज़ाक किया जाता था कि कंटीन तो अब बन्द हो जायेगी, कविता तो जा रही है।
मेरे लिए चाय का अर्थ है शुद्ध चाय। अर्थात पानी, ठीक-सा दूध, चीनी और पत्ती। कुछ लोग चाय के नाम पर काढ़ा पीना पसन्द करते हैं। हाय! अदरक नहीं डाला, छोटी इलायची के बिना तो स्वाद ही नहीं आता, दालचीनी वाली चाय बड़ी स्वाद होती है। दूध वाली गाढ़ी चाय होनी चाहिए। अरे तो दूध ही पी लीजिए, चाय के बहाने दूध क्यों पी रहे हैं, सीधे-सीधे कहिए कि दूध पीना है। कुछ लोग चाय का मसाला बनाकर रखते हैं। अरे ! ऐसी ही चाय पीनी है तो गर्म मसाला ही पी लीजिए, चाय को क्यों बदनाम कर रहे हैं।
लोग कहते हैं चाय से गैस हो जाती है, नींद नहीं आती है अथवा नींद आ जाती है। पता नहीं कैसे हैं यह लोग।
आह! किसी समय, कितनी बार, कहीं भी, बस चाय, चाय और चाय।