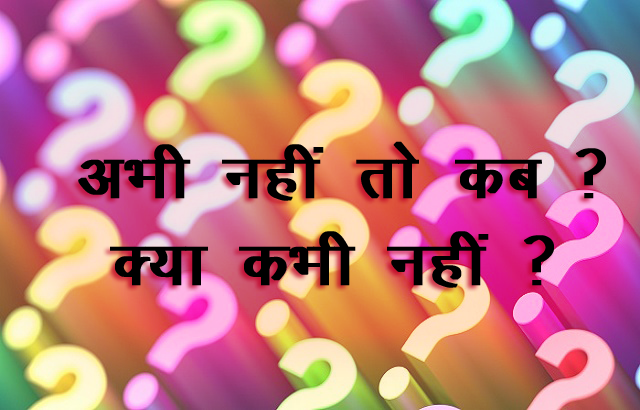अब कोई हमसफ़र नहीं होता
प्रार्थनाओं का अब कोई असर नहीं होता।
कामनाओं का अब कोई
सफ़र नहीं होता।
सबकी अपनी-अपनी मंज़िलें हैं ,
और अपने हैं रास्ते।
सरे राह चलते
अब कोई हमसफ़र नहीं होता।
देखते-परखते निकल जाती है
ज़िन्दगी सारी,
साथ-साथ रहकर भी ,
अब कोई बसर नहीं होता।
भरोसे की तो हम
अब बात ही नहीं करते,
अपने और परायों में
अब कुछ अलग महसूस नहीं होता।
रोज़ पढ़ती हूं भूल जाती हूं
जीवन के सिखाये गये पाठ
बार बार दोहराती हूं।
रोज़ याद करती हूं, पर भूल जाती हूं ।
पुस्तकें पढ़कर नहीं चलता जीवन,
यह जानकर भी
वही पाठ बार-बार दोहराती हूं ।
सब कहते हैं, पढ़ ले, पढ़ ले,
जीवन में कुछ आगे बढ़ ले ।
पर मेरी बात
कोई क्यों नहीं समझ पाता।
कुछ पन्ने, कुछ हिसाब-बेहिसाब
कभी समझ ही नहीं पाती हूं,
लिख-लिखकर दोहराती हूं ।
कभी स्याही चुक जाती है ,
कभी कलम छूट जाती है,
अपने को बार-बार समझाती हूं ।
फिर भी,
रोज़ याद करती हूं ,भूल जाती हूं ।
ज़्यादा गहराईयों से
डर लगता है मुझे
इसलिए कितने ही पन्ने
अधपढ़े छोड़ आगे बढ़ जाती हूं ।
कोई तो समझे मेरी बात ।
कहते हैं,
तकिये के नीचे रख दो किताब,
जिसे याद करना हो बेहिसाब,
पर ऐसा करके भी देख लिया मैंने
सपनों में भी पढ़कर देख लिया मैंने,
बस, इसी तरह जीती चली जाती हूं ।
.
रोज़ पढ़ती हूं भूल जाती हूं ।
सच बोलने की आदत है बुरी
सच बोलने की आदत है बुरी।
इसीलिए
सभी लोग रहने लगे हैं किनारे ।
पीठ पर वार करना मुझे भाता नहीं।
चुप रहना मुझे आता नहीं।
भाती नहीं मुझे झूठी मिठास।
मन मसोस कर मैं जीती नहीं।
खरी-खरी कहने से मैं रूकती नहीं।
इसीलिए
सभी लोग रहने लगे हैं किनारे।
-
हालात क्या बदले,
वक्त ने क्या चोट दी,
सब लोग रहने लगे हैं किनारे ।
काश !
कोई तो हमारी डूबती कश्ती में
सवार होता संग हमारे।
कहीं तो हम नाव खेते
किसी के सहारे।
-
किन्तु हालात यूं बदले
न पता लगा, कब टूटे किनारे।
सब लोग जो बैठे थे किनारे।
डूबते-उतरते वे अब ढूंढने लगे सहारे।
तैर कर निकल आये हम तो किनारे।
उसी कश्ती को थाम ,
अब वे भी ढूंढने में लगे हैं किनारे ।
आंसू और हंसी के बीच
यूं तो राहें समतल लगती हैं, अवरोध नहीं दिखते।
चलते-चलते कंकड़ चुभते हैं, घाव कहीं रिसते।
कभी तो बारिश की बूंदें भी चुभ जाया करती हैं,
आंसू और हंसी के बीच ही इन्द्रधनुष देखे खिलते।
पुष्प निःस्वार्थ भाव से
पुष्प निःस्वार्थ भाव से नित बागों को महकाते।
पंछी को देखो नित नये राग हमें मधुर सुनाते।
चंदा-सूरज दिग्-दिगन्त रोशन करते हरपल,
हम ही क्यों छल-कपट में उलझे सबको बहकाते।
कुछ पल बस अपने लिये
उदित होते सूर्य की रश्मियां
मन को आह्लादित करती हैं।
विविध रंग
मन को आह्लादमयी सांत्वना
प्रदान करते हैं।
शांत चित्त, एकान्त चिन्तन
सांसारिक विषमताओं से
मुक्त करता है।
सांसारिकता से जूझते-जूझते
जब मन उचाट होता है,
तब पल भर का ध्यान
मन-मस्तिष्क को
संतुलित करता है।
आधुनिकता की तीव्र गति
प्राय: निढाल कर जाती है।
किन्तु एक दीर्घ उच्छवास
सारी थकान लूट ले जाता है।
जब मन एकाग्र होता है
तब अधिकांश चिन्ताएं
कहीं गह्वर में चली जाती हैं
और स्वस्थ मन-मस्तिष्क
सारे हल ढूंढ लाता है।
इन व्यस्तताओं में
कुछ पल तो निकाल
बस अपने लिये।
मेरी असमर्थ अभिव्यक्ति
जब भी
कुछ कहने का
प्रयास करती हूं कविता में,
तभी पाती हूं
कि उसे ही
एक अनजानी सी भाषा में,
अनजाने अव्यक्त शब्दों में,
जिनसे मैं जुड़ नहीं पाती
पूरी कोशिश के बावजूद भी,
किसी और ने
पहले ही कह रखी है वह बात।
.
या फिर
अनुभव मैं यह करती हूं,
कि जो मैं कहना चाहती हूं,
वह किसी और ने
मेरी ही भावनाएं चुराकर,
मानों मुझसे ही पूछकर,
मेरे ही विचार
मेरी ही इच्छानुसार,
लेकिन मुझसे पहले ही
अभिव्यक्त कर दिये हैं,
सही शब्दों में
सही लोगों के सामने
और सही रूप में।
शब्दों की तलाश में
भटकती थी मैं
जिनकी अभिव्यक्ति के लिए।
सारे शब्द
निर्थरक हो जाते थे
जिसे कहने के लिए मेरे सामने
वही बातें
कविता में व्यक्त कर दी हैं
किसी ने मानों
मेरी ही इच्छानुसार।
या फिर
तुम्हारा, उसका, इसका
सबका लिखा
गलत लगता है।
झूठ और छल।
मानों सब मिलकर
मेरे विरूद्ध
एक षड्यन्त्र के भागीदार हों।
मैं,
विरोध में कलम उठाती हूं
लिखना चाहती हूं
तुम्हारे, उसके, इसके लिखे के विरोध में।
बार बार लिखती हूं
पर फिर भी
अनलिखी रह जाती हूं
अनुभव बस एक अधूरेपन का।
आक्रोश, गुस्सा, झुंझलाहट,
विरोध, विद्रोह,
कुछ नहीं ठहरता।
इससे पहले कि लिखना पूरा करूं
चाय बनानी है, रोटी पकानी है
कपड़े धोने हैं
बीच में बच्चा रोने लगेगा
इसी बीच
स्याही चुक जाती है।
रोज़ नया आक्रोश जन्म लेता है
और चाय के साथ उफ़नकर
ठण्डा हो जाता है।
कभी लिख भी लेती हूं
तो बड़ा नाम नहीं है मेरे पास।
सम्पर्क साधन भी नहीं।
किसी गुट में भी नहीं।
फिर, किसी प्राध्यापक की
चरण रज भी नहीं ली मैंने।
किसी के बच्चे को टाफ़ियां भी नहीं खिलाईं
और न ही किसी की पत्नी को
भाभीजी बनाकर उसे तोहफ़े दिये।
मेरे पिता के पास भी
इतनी सामर्थ्य न थी
कि वे उनका कोई काम कर देते।
फिर वे मेरी रचनाओं में रूचि कैसे लेते।
और
इस सबके बाद भी लगता है
मैं ही गलत हूं कहीं
खामोश हो जीती हूं तब
अनकही, यह सोचकर
कि चलो
मेरे विचारों की अभिव्यक्ति हुई तो सही
मेरे द्वारा नहीं
तो किसी और के माध्यम से ही सही
पूर्णतया अस्पष्ट तो रही नहीं
प्रकट तो हुई
स्वयं नहीं कर पाई
तो किसी और की कृपा से
लोगों तक बात पहुंची तो सही
शायद यही कारण है
कि लोगों की लिखी कविताओं का
इतना बड़ा संग्रह मेरे पास है
जो कहीं मेरा अपना है।
पर सचमुच
आश्चर्य तो होता ही है
कि मेरे विचार
मेरी ही इच्छानुसार
मैं नहीं कोई और
कैसे अभिव्यक्त कर लेते हैं
इतने समर्थ होकर
.
जो मैं चाहती हूं
वही तुम भी चाहते हो
ऐसा कैसे।
तो क्या
इस दुनिया में
मेरे अतिरिक्त भी इंसान बसते हैं
या फिर
इस दुनिया में रहकर भी
मेरे भीतर इंसानियत बची है !
कोयल और कौए दोनों की वाणी मीठी होती है
बड़ी मौसमी,
बड़ी मूडी होती है कोयल।
अपनी कूक सुनाने के लिए
एक मौसम की प्रतीक्षा में
छिपकर बैठी रहती है।
पत्तों के झुरमुट में,
डालियों के बीच।
दूर से आवाज़ देती है
आम के मौसम की प्रतीक्षा में,
बैठी रहती है, लालची सी।
कौन से गीत गाती है
मुझे आज तक समझ नहीं आये।
मुझे तो आनन्द देती है
कौए की कां कां भी।
आवाज़ लगाकर,
कितने अपनेपन से,
अधिकार से आ बैठता है
मुंडेर पर।
बिना किसी नाटक के
आराम से बैठकर
जो मिल जाये
खाकर चल देता है।
हर मौसम में
एक-सा भाव रखता है।
बस कुछ धारणाएं
बनाकर बैठ जाते हैं हम,
नहीं तो, बेचारे पंछी
तो सभी मधुर बोलते हैं,
मौसम की आहट तो
हमारे मन की है
फिर वह बसन्त हो
अथवा पतझड़।
अब घड़ी से नहीं चलती ज़िन्दगी
अक्सर लगता है,
कुछ
निठ्ठलापन आ गया है।
वे ही सारे काम
जो खेल-खेल में
हो जाया करते थे,
पल भर में,
अब, दिनों-दिन
बहकने लगे हैं।
सुबह कब आती है,
शाम कब ढल जाती है,
आभास चला गया है।
अंधेरे -उजाले
एक-से लगने लगे हैं।
घर बंधन तो नहीं लगता,
किन्तु बंधे से रहते हैं,
फिर भी वे सारे काम,
जो खेल-खेल में
हो जाया करते थे,
अब, दिनों तक
टहलने लगे हैं।
समय बहुत है,
शायद यही एहसास
समय के महत्व को
समझने से रोकता है।
घड़ी के घंटों से
नहीं बंधे हैं अब।
न विलम्ब की चिन्ता,
न लम्बित कार्यों की।
मैं नहीं तो
कोई और कर लेगा,
मुझे चिन्ता नहीं।
खेल-खेल में
क्या समय का महत्व
घटने लगा है।
कहीं एक तकलीफ़ तो है,
बस शब्द नहीं हैं।
घड़ियां बन्द पड़ी हैं,
अब घड़ी से नहीं चलती ज़िन्दगी,
पर पता नहीं
समय कैसे कटने लगा है।
मन बहक-बहक जाये
इन फूलों को देखकर
अकारण ही मन मुस्काए।
न जाने
किस की याद आये।
तब, यहां
गुनगुनाती थी चिड़ियां।
तितलियां पास आकर पूछती थीं,
क्यों मन ही मन शरमाये।
उलझी-उलझी सी डालियां,
मानों गलबहियां डाले,
फूलों की ओट में छुप जायें।
हवाओं का रूख भी
अजीब हुआ करता था,
फूलों संग लाड़ करती
शरारती-सी
महक-महक जाये।
खिली-खिली-सी धूप,
बादलों संग करती अठखेलियां,
न जाने क्या कह जाये।
झरते फूलों को
अंजुरि में समेट
मन बहक-बहक जाये।
अवसर है अकेलापन अपनी तलाश का
एक सपने में जीती हूं,
अंधेरे में रोशनी ढूंढती हूं।
बहारों की आस में,
कुछ पुष्प लिए हाथ में,
दिन-रात को भूलती हूं।
काल-चक्र घूमता है,
मुझसे कुछ पूछता है,
मैं कहां समझ पाती हूं।
कुछ पाने की आस में
बढ़ती जाती हूं।
गगन-धरा पुकारते हैं,
कहते हैं
चलते जाना, चलते जाना
जीवन-गति कभी ठहर न पाये,
चंदा-सूरज से सीख लेना
तारों-सा टिमटिमाना,
अवसर है अकेलापन
अपनी तलाश का ,
अपने को पहचानने का,
अपने-आप में
अपने लिए जीने का।
ठहरी ठहरी सी लगती है ज़िन्दगी
अब तो
ठहरी-ठहरी-सी
लगती है ज़िन्दगी।
दीवारों के भीतर
सिमटी-सिमटी-सी
लगती है ज़िन्दगी।
द्वार पर पहरे लगे हैं,
मन पर गहरे लगे हैं,
न कोई चोट है कहीं,
न घाव रिसता है,
रक्त के थक्के जमने लगे हैं।
भाव सिमटने लगे हैं,
अभिव्यक्ति के रूप
बदलने लगे हैं।
इच्छाओं पर ताले लगने लगे हैं।
सत्य से मन डरने लगा है,
झूठ के ध्वज फ़हराने लगे हैं।
न करना शिकायत किसी की
न बताना कभी मन के भेद,
लोग बस
तमाशा बनाने में लगे हैं।
न ग्रहण है न अमावस्या,
तब भी जीवन में
अंधेरे गहराने लगे हैं।
जीतने वालों को न पूछता कोई
हारने वालों के नाम
सुर्खियों में चमकने लगे हैं।
अनजाने डर और खौफ़ में जीते
अपने भी अब
पराये-से लगने लगे हैं।
मन के पिंजरे खोल रे मनवा
मन विहग!
मन के पिंजरे खोल रे मनवा,
मन के बंधन तोड़ रे मनवा।
कुछ तो टूटेगा,
कुछ तो बिखरेगा,
कुछ तो बदलेगा।
गगन विशाल,
उड़ान बड़ी है,
पंख मिले छोटे,
कुछ कतरे गये।
कुछ टूटे,
कुछ बिखर गये।
चाहत न छोड़,
मन को न मोड़,
उड़ान भर,
आज नहीं तो कल,
कल नहीं तो कभी,
या फिर अभी
चाहतों को जोड़,
मन को न मोड़।
उड़ान भर।
न डर, बस
मन के पिंजरे खोल रे मनवा,
मन के बंधन तोड़ रे मनवा।
सघन-वन-कानन ये मन है
सघन-वन-कानन ये मन है।
चिड़िया भी चहके,
कोयल भी कूके,
फूलों की डाली भी महके,
कभी उलझ-उलझकर
मन-भाव बहके।
पर डर लगता है
जब
वानर, डाल-डाल बहके।
कब जाग उठेगा नृसिंह
कब गज की गर्जन से
गूंजेगा गगन,
कौन जाने।
कभी हरीतिमा, कभी सूखा,
कभी पतझड़, कभी रूखा
कब टूटेगी डाली,
कब बिखरेंगे पल्लव
कौन जाने।
दावानल भीतर ही भीतर चलता है
इसीलिए ये
सघन-वन-कानन मन डरता है।
जो भी हुआ अच्छा हुआ
अच्छा हुआ
इधर कानों ने सुनना
कम कर दिया है।
अच्छा हुआ
आंखों पर चश्मा
चढ़ा हुआ है।
अच्छा हुआ
अब दूरियों की पहचान
होने लगी है।
अच्छा हुआ
नज़दीकियों की चाहत
घटने लगी है।
अच्छा हुआ
अब घर से निकलता
बन्द हुआ है।
अच्छा हुआ
अब कामनाओं पर
आहट होने लगी है।
अच्छा हुआ
सवालों के रूख
बदलने लगे हैं।
अच्छा हुआ
उत्तर अब बने-बनाये
मिलने लगे हैं।
अच्छा हुआ
ज़िन्दगी अब
ठहरने-सी लगी है।
सोचती हूं
जो भी हुआ।
अच्छा हुआ,
अच्छा ही हुआ।
अवसान एक प्रेम-कथा का
अपनी कामनाओं को
मुट्ठी में बांधे
चुप रहे हम
कैसे जान गये
धरा-गगन
क्यों हवाओं में
छप गया हमारा नाम
बादलों में क्यों सिहरन हुई
क्यों पंछियों ने तान छेड़ी
लहरों में एक कशमकश
कहीं भंवर उठे
कहीं सागर मचले
धूमिल-धूमिल हुआ सब
और हम
देखते रह गये
पाषाण बनते भाव
अवसान
एक प्रेम-कथा का।
आंखों में तिरते हैं सपने
आंखों में तिरते हैं सपने,
कुछ गहरे हैं कुछ अपने।
पलकों के साये में
लिखते रहे
प्यार की कहानियां,
कागज़ पर न उकेरी कभी
तेरी मेरी रूमानियां।
कुछ मोती हैं,
नयनों के भीतर
कोई देख न ले,
पलकें मूंद सकते नहीं
कोई भेद न ले।
यूं तो कजराने नयना
काजर से सजते हैं
पर जब तुम्हारी बात उठती है
तब नयनों में तारे सजते हैं।
जीना है तो बुझी राख में भी आग दबाकर रखनी पड़ती है
मन के गह्वर में एक ज्वाला जलाकर रखनी पड़ती है
आंसुओं को सोखकर विचारधारा बनाकर रखनी पड़ती है
ज़्यादा सहनशीलता, कहते हैं निर्बलता का प्रतीक होती है
जीना है तो, बुझी राख में भी आग दबाकर रखनी पड़ती है
सोचने का वक्त ही कहां मिला
ज़िन्दगी की खरीदारी में मोल-भाव कभी कर न पाई
तराजू लेकर बैठी रही खरीद-फरोख्त कभी कर न पाई
कहां लाभ, कहां हानि, सोचने का वक्त ही कहां मिला
इसी उधेड़बुन में उलझी जिन्दगी कभी सम्हल न पाई
मत विश्वास कर परछाईयों पर
कौन कहता है दर्पण सदैव सच बताता है
हम जो देखना चाहें अक्सर वही दिखाता है
मत विश्वास कर इन परछाईयों-अक्सों पर
बायें को दायां और दायें को बायां बताता है
नासूर सी चुभती हैं बातें
काश मैं वह सब बोल पाती, कुछ सीमाओं को तोड़ पाती
नासूर सी चुभती हैं कितनी ही बातें, क्यों नहीं मैं रोक पाती
न शब्द मिलें, न आज़ादी, और न नैतिकता अनुमति देती है
पर्यावरण के शाब्दिक प्रदूषण का मैं खुलकर, कर विरोध पाती
मन की बगिया महक रही देखो मैं बहक रही
फुलवारी में फूल खिले हैं मन की बगिया भी महक रही
पेड़ों पर बूर पड़े,कलियों ने करवट ली,देखो महक रहीं
तितली ने पंख पसारे,फूलों से देखो तो गुपचुप बात हुई
अन्तर्मन में चाहत की हूक उठी, देखो तो मैं बहक रही
मन से अब भी बच्चे हैं
हाव-भाव भी अच्छे हैं
मन के भी हम सच्चे हैं
सूरत पर तो जाना मत
मन से अब भी बच्चे हैं
माणिक मोती ढलते हैं
सीपी में गिरती हैं बूंदे तब माणिक मोती ढलते हैं
नयनों से बहती हैं तब भावों के सागर बनते हैं
अदा इनकी मुस्कानों के संग निराली होती है
भीतर-भीतर रिसती हैं तब गहरे घाव पनपते हैं
आशा अब नहीं रहती
औरों की क्या बात करें, अब तो अपनी खोज-खबर नहीं रहती,
इतनी उम्र बीत गई, क्या कर गई, क्या करना है सोचती रहती,
किसने साथ दिया था जीवन में, कौन छोड़ गया था मझधार में
रिश्ते बिगड़े,आघात हुए, पर लौटेंगे शायद, आशा अब नहीं रहती
पता नहीं क्या क्या मन करता है आजकल
रजाई खींच कर, देर तक सोने का बहुत मन करता है रे ! आजकल।
बना-बनाया भोजन परस जाये थाली में बहुत मन करता है आजकल।
एक मेरी जान के दुश्मन ये चिकित्सक, कह दिया रक्तचाप अधिक है
सैर के लिए जाना ज़रूरी है, संध्या समय घर से निकाल देते हैं आजकल
प्रात कोई चाय पिला दे, देर तक सोते रहें, यही मन करता है आजकल
जीवन है मेरा राहें हैं मेरी सपने हैं अपने हैं
साहस है मेरा, इच्छा है मेरी, पर क्यों लोग हस्तक्षेप करने चले आते हैं
जीवन है मेरा, राहें हैं मेरी, पर क्यों लोग “कंधा” देने चले आते हैं
अपने हैं, सपने हैं, कुछ जुड़ते हैं बनते हैं, कुछ मिटते हैं, तुमको क्या
जीती हूं अपनी शर्तों पर, पर पता नहीं क्यों लोग आग लगाने चले आते हैं
क्रोध कोई विकार नहीं
अनैतिकता, अन्याय, अनाचार पर क्या क्रोध नहीं आता, जो बोलते नहीं
केवल विनम्रता, दया, विलाप से यह दुनिया चलती नहीं, क्यों सोचते नहीं
नवरसों में क्रोध कोई विकार नहीं मन की सहज सरल अभिव्यक्ति है
एक सुखद परिवर्तन के लिए खुलकर बोलिए, अपने आप को रोकिए नहीं
कभी-कभी वजह-बेवजह क्रोध करना भी ज़रूरी है
विनम्रता से दुनिया अब नहीं चलती, असहिष्णुता भी ज़रूरी है।
समझौतों से बात अब नहीं बनती, अस्त्र उठाना भी ज़रूरी है।
ऐसा अब होता है जब हम रोते हैं जग हंसता है ताने कसता है
सरलता छोड़, कभी-कभी वजह-बेवजह क्रोध करना भी ज़रूरी है
धूप-छांव तो आनी-जानी है हर पल
सोचती कुछ और हूं, समझती कुछ और हूं, लिखती कुछ और हूं
बहकते हैं मन के उद्गार, भीगते हैं नमय, तब बोलती कुछ और हूं
जानती हूं धूप-छांव तो आनी-जानी है हर पल, हर दिन जीवन में
देखती कुछ और हूं, दिखाती कुछ और हूं, अनुभव करती कुछ और हूं